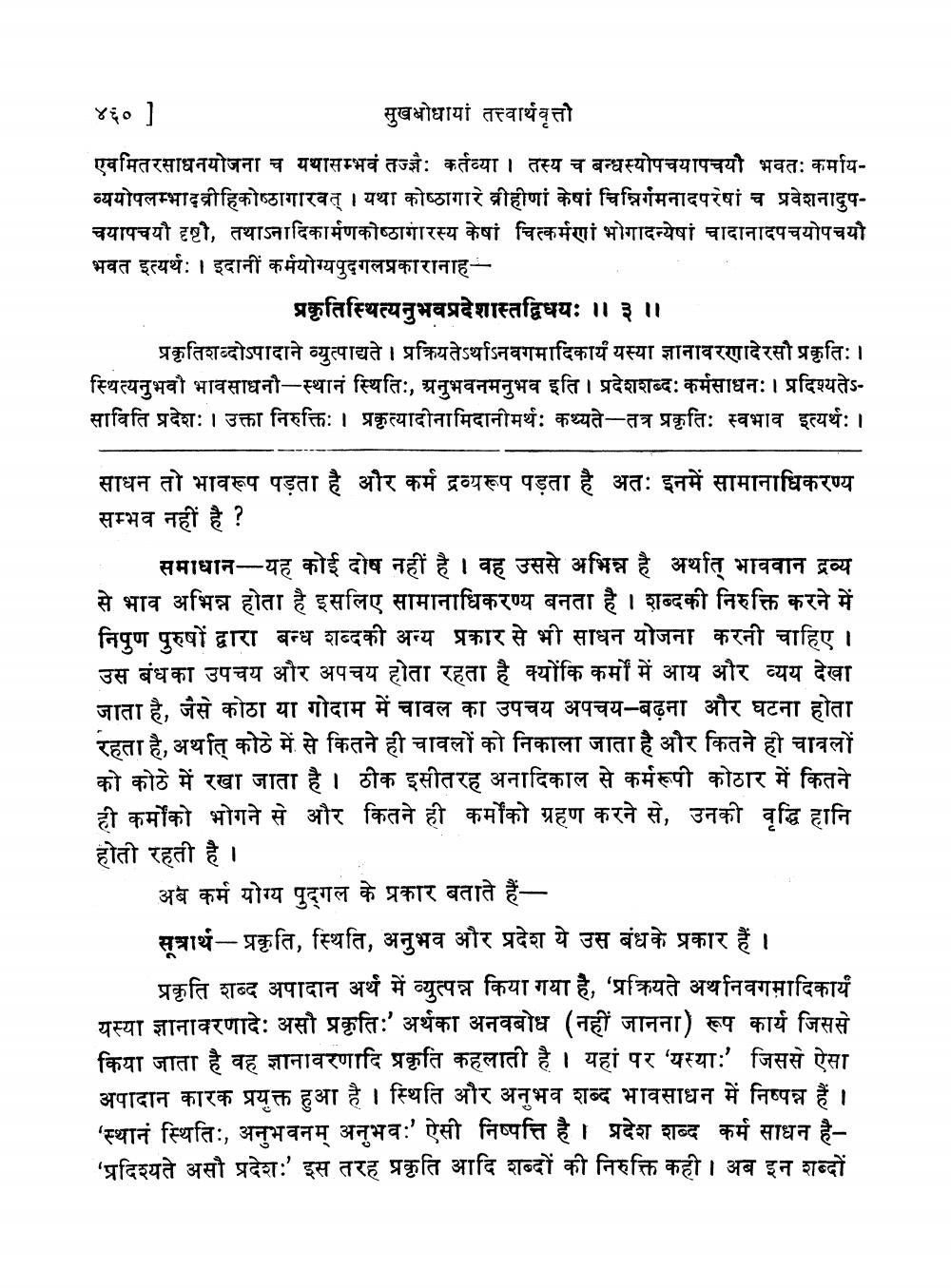________________
४६० ]
सुखबोधायां तत्त्वार्थवृत्ती एवमितरसाधनयोजना च यथासम्भवं तज्ज्ञैः कर्तव्या। तस्य च बन्धस्योपचयापचयौ भवतः कर्मायव्ययोपलम्भादव्रीहिकोष्ठागारवत् । यथा कोष्ठागारे व्रीहीणां केषां चिन्निर्गमनादपरेषां च प्रवेशनादुपचयापचयौ दृष्टौ, तथाऽनादिकार्मणकोष्ठागारस्य केषां चित्कर्मणां भोगादन्येषां चादानादपचयोपचयौ भवत इत्यर्थः । इदानीं कर्मयोग्यपुद्गलप्रकारानाह
प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशास्तद्विधयः ॥ ३ ॥ प्रकृतिशब्दोऽपादाने व्युत्पाद्यते । प्रक्रियतेऽर्थाऽनवगमादिकार्य यस्या ज्ञानावरणादेरसौ प्रकृतिः । स्थित्यनुभवौ भावसाधनौ-स्थानं स्थितिः, अनुभवनमनुभव इति । प्रदेशशब्दः कर्मसाधनः । प्रदिश्यतेऽसाविति प्रदेशः । उक्ता निरुक्तिः । प्रकृत्यादीनामिदानीमर्थः कथ्यते तत्र प्रकृतिः स्वभाव इत्यर्थः ।
साधन तो भावरूप पड़ता है और कर्म द्रव्यरूप पड़ता है अतः इनमें सामानाधिकरण्य सम्भव नहीं है ? _समाधान-यह कोई दोष नहीं है । वह उससे अभिन्न है अर्थात् भाववान द्रव्य से भाव अभिन्न होता है इसलिए सामानाधिकरण्य बनता है । शब्दकी निरुक्ति करने में निपुण पुरुषों द्वारा बन्ध शब्दकी अन्य प्रकार से भी साधन योजना करनी चाहिए। उस बंध का उपचय और अपचय होता रहता है क्योंकि कर्मों में आय और व्यय देखा जाता है, जैसे कोठा या गोदाम में चावल का उपचय अपचय-बढ़ना और घटना होता रहता है, अर्थात् कोठे में से कितने ही चावलों को निकाला जाता है और कितने ही चावलों को कोठे में रखा जाता है। ठीक इसीतरह अनादिकाल से कर्मरूपी कोठार में कितने ही कर्मोको भोगने से और कितने ही कर्मोंको ग्रहण करने से, उनकी वृद्धि हानि होती रहती है।
अब कर्म योग्य पुद्गल के प्रकार बताते हैंसूत्रार्थ-प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश ये उस बंध के प्रकार हैं ।
प्रकृति शब्द अपादान अर्थ में व्युत्पन्न किया गया है, 'प्रक्रियते अर्थानवगमादिकार्य यस्या ज्ञानावरणादेः असौ प्रकृतिः' अर्थका अनवबोध (नहीं जानना) रूप कार्य जिससे किया जाता है वह ज्ञानावरणादि प्रकृति कहलाती है। यहां पर 'यस्याः' जिससे ऐसा अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है । स्थिति और अनुभव शब्द भावसाधन में निष्पन्न हैं । 'स्थानं स्थितिः, अनुभवनम् अनुभवः' ऐसी निष्पत्ति है। प्रदेश शब्द कर्म साधन है'प्रदिश्यते असौ प्रदेशः' इस तरह प्रकृति आदि शब्दों की निरुक्ति कही। अब इन शब्दों