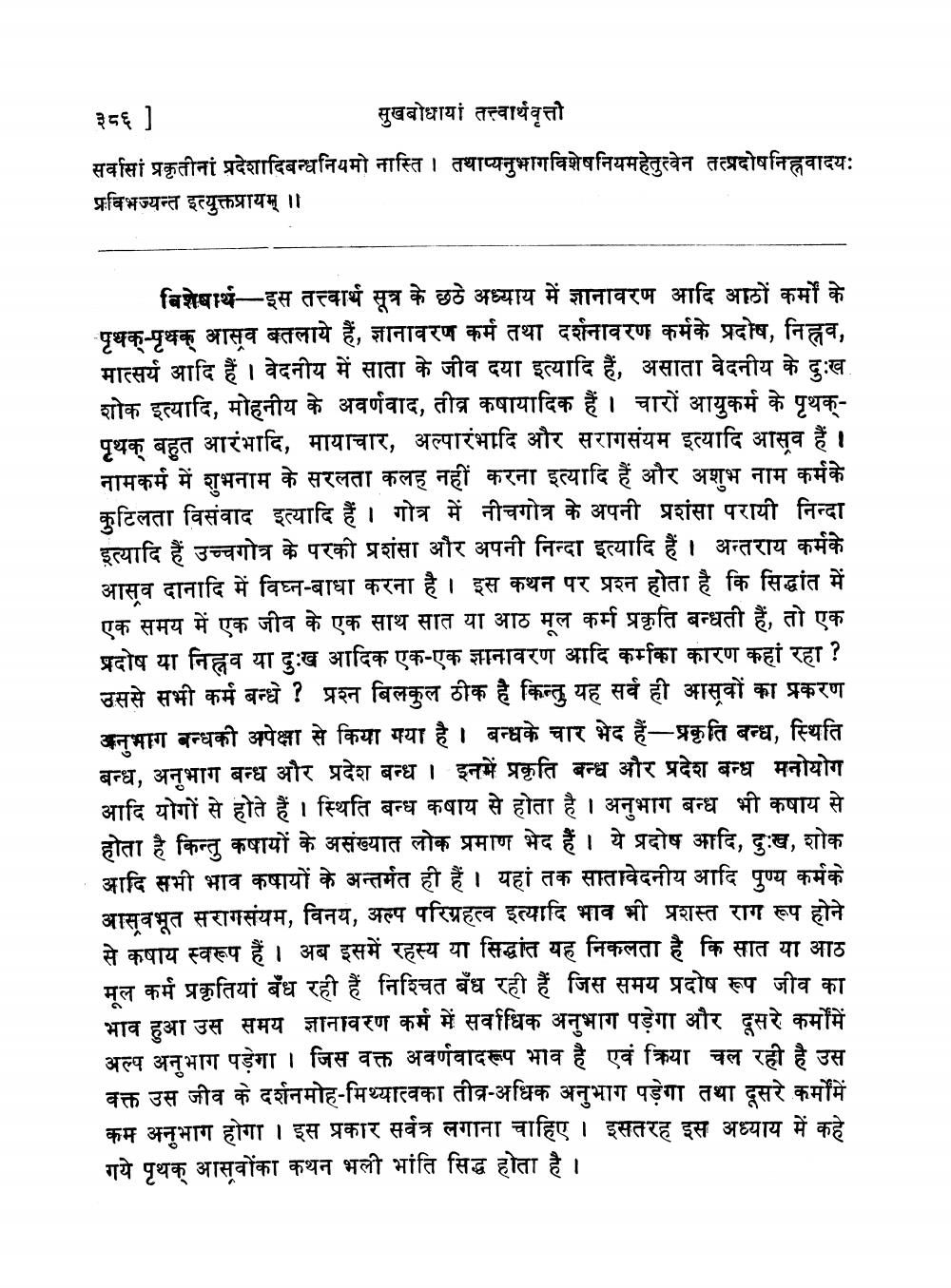________________
३८६ ]
सुखबोधायां तत्त्वार्थवृत्ती सर्वासां प्रकृतीनां प्रदेशादिबन्धनियमो नास्ति । तथाप्यनुभागविशेषनियमहेतुत्वेन तत्प्रदोषनिह्नवादयः प्रविभज्यन्त इत्युक्तप्रायम् ॥
विशेषार्थ-इस तत्त्वार्थ सूत्र के छठे अध्याय में ज्ञानावरण आदि आठों कर्मों के पृथक्-पृथक् आसव बतलाये हैं, ज्ञानावरण कर्म तथा दर्शनावरण कर्मके प्रदोष, निह्नव, मात्सर्य आदि हैं । वेदनीय में साता के जीव दया इत्यादि हैं, असाता वेदनीय के दुःख शोक इत्यादि, मोहनीय के अवर्णवाद, तीव्र कषायादिक हैं। चारों आयुकर्म के पृथक्पृथक् बहुत आरंभादि, मायाचार, अल्पारंभादि और सरागसंयम इत्यादि आसव हैं। नामकर्म में शुभनाम के सरलता कलह नहीं करना इत्यादि हैं और अशुभ नाम कर्मके कुटिलता विसंवाद इत्यादि हैं। गोत्र में नीचगोत्र के अपनी प्रशंसा परायी निन्दा इत्यादि हैं उच्चगोत्र के परकी प्रशंसा और अपनी निन्दा इत्यादि हैं। अन्तराय कर्मके आसव दानादि में विघ्न-बाधा करना है। इस कथन पर प्रश्न होता है कि सिद्धांत में एक समय में एक जीव के एक साथ सात या आठ मूल कर्म प्रकृति बन्धती हैं, तो एक प्रदोष या निह्नव या दुःख आदिक एक-एक ज्ञानावरण आदि कर्मका कारण कहां रहा ? उससे सभी कर्म बन्धे ? प्रश्न बिलकुल ठीक है किन्तु यह सर्व ही आसवों का प्रकरण अनुभाग बन्धकी अपेक्षा से किया गया है। बन्धके चार भेद हैं-प्रकृति बन्ध, स्थिति बन्ध, अनुभाग बन्ध और प्रदेश बन्ध । इनमें प्रकृति बन्ध और प्रदेश बन्ध मनोयोग आदि योगों से होते हैं । स्थिति बन्ध कषाय से होता है । अनुभाग बन्ध भी कषाय से होता है किन्तु कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। ये प्रदोष आदि, दुःख, शोक आदि सभी भाव कषायों के अन्तर्गत ही हैं। यहां तक सातावेदनीय आदि पुण्य कर्मके आसवभूत सरागसंयम, विनय, अल्प परिग्रहत्व इत्यादि भाव भी प्रशस्त राग रूप होने से कषाय स्वरूप हैं। अब इसमें रहस्य या सिद्धांत यह निकलता है कि सात या आठ मूल कर्म प्रकृतियां बँध रही हैं निश्चित बँध रही हैं जिस समय प्रदोष रूप जीव का भाव हुआ उस समय ज्ञानावरण कर्म में सर्वाधिक अनुभाग पड़ेगा और दूसरे कर्मों में अल्प अनुभाग पड़ेगा। जिस वक्त अवर्णवादरूप भाव है एवं क्रिया चल रही है उस वक्त उस जीव के दर्शनमोह-मिथ्यात्वका तीव्र-अधिक अनुभाग पड़ेगा तथा दूसरे कर्मों में कम अनुभाग होगा । इस प्रकार सर्वत्र लगाना चाहिए। इसतरह इस अध्याय में कहे गये पृथक् आसवोंका कथन भली भांति सिद्ध होता है ।