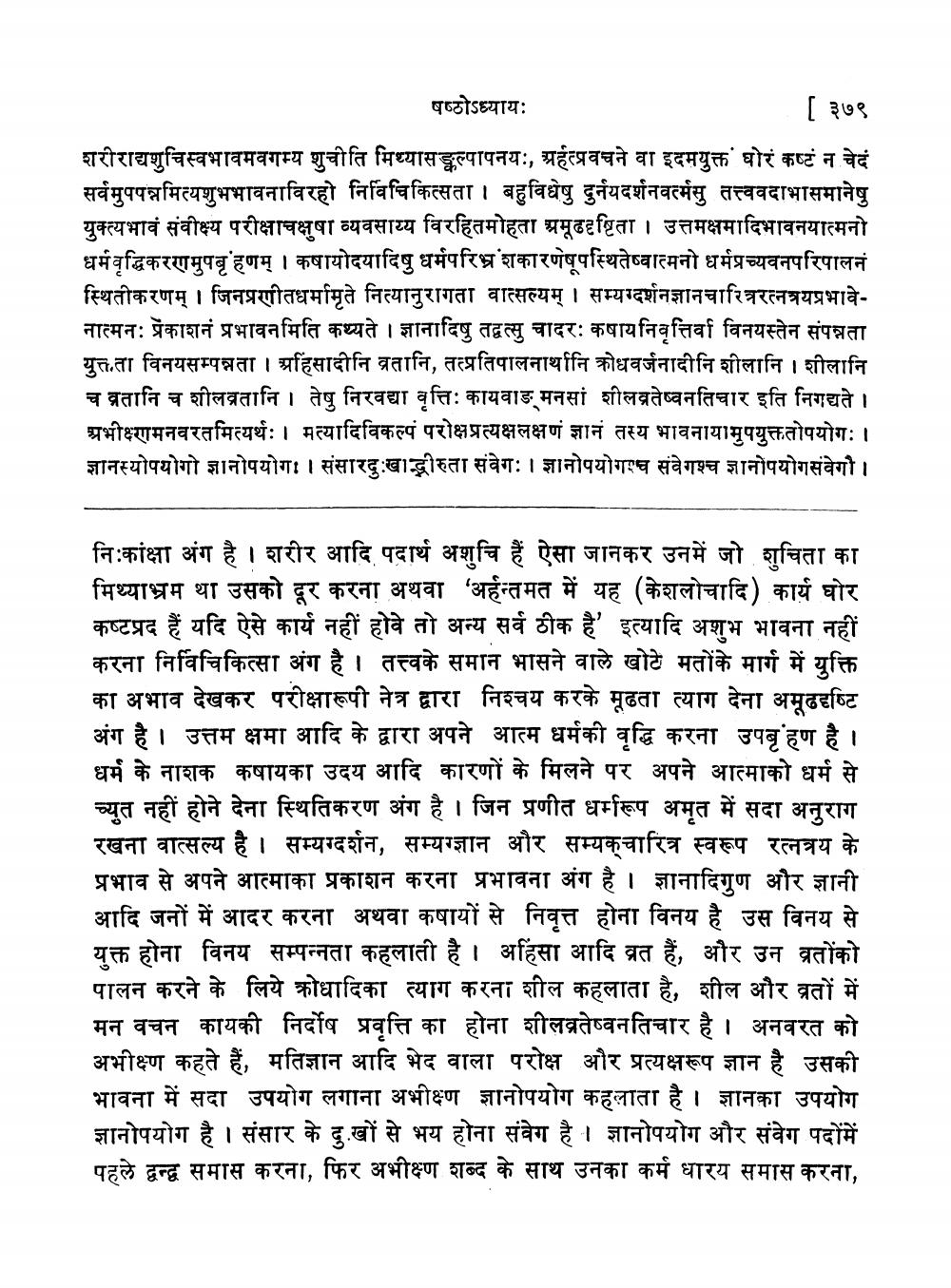________________
षष्ठोऽध्यायः
[ ३७९ शरीराद्यशुचिस्वभावमवगम्य शुचीति मिथ्यासङ्कल्पापनयः, अहत्प्रवचने वा इदमयुक्त घोरं कष्टं न चेदं सर्वमुपपन्नमित्यशुभभावनाविरहो निर्विचिकित्सता। बहुविधेषु दुर्नयदर्शनवर्त्मसु तत्त्ववदाभासमानेषु युक्त्यभावं संवीक्ष्य परीक्षाचक्षुषा व्यवसाय्य विरहितमोहता अमूढदृष्टिता । उत्तमक्षमादिभावनयात्मनो धर्मवृद्धिकरणमुपबृहणम् । कषायोदयादिषु धर्मपरिभ्र कारणेपस्थितेष्वात्मनो धर्मप्रच्यवनपरिपालनं स्थितीकरणम् । जिनप्रणीतधर्मामृते नित्यानुरागता वात्सल्यम् । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररत्नत्रयप्रभावेनात्मनः प्रकाशनं प्रभावन मिति कथ्यते । ज्ञानादिषु तद्वत्सु चादरः कषाय निवृत्तिर्वा विनयस्तेन संपन्नता युक्तता विनयसम्पन्नता । अहिंसादीनि व्रतानि, तत्प्रतिपालनार्थानि क्रोधवर्जनादीनि शीलानि । शीलानि च व्रतानि च शीलव्रतानि । तेषु निरवद्या वृत्तिः कायवाङ् मनसां शीलव्रतेष्वनतिचार इति निगद्यते । अभीक्ष्णमनवरतमित्यर्थः । मत्यादिविकल्पं परोक्षप्रत्यक्षलक्षणं ज्ञानं तस्य भावनायामुपयुक्ततोपयोगः । ज्ञानस्योपयोगो ज्ञानोपयोगः । संसारदुःखाद्भीरुता संवेगः । ज्ञानोपयोगएच संवेगश्च ज्ञानोपयोगसंवेगौ।
निःकांक्षा अंग है । शरीर आदि पदार्थ अशुचि हैं ऐसा जानकर उनमें जो शुचिता का मिथ्याभ्रम था उसको दूर करना अथवा 'अर्हन्तमत में यह (केशलोचादि) कार्य घोर कष्टप्रद हैं यदि ऐसे कार्य नहीं होवे तो अन्य सर्व ठीक है' इत्यादि अशुभ भावना नहीं करना निर्विचिकित्सा अंग है। तत्त्वके समान भासने वाले खोटे मतोंके मार्ग में युक्ति का अभाव देखकर परीक्षारूपी नेत्र द्वारा निश्चय करके मूढता त्याग देना अमूढदृष्टि अंग है। उत्तम क्षमा आदि के द्वारा अपने आत्म धर्मकी वृद्धि करना उपबृहण है। धर्म के नाशक कषायका उदय आदि कारणों के मिलने पर अपने आत्माको धर्म से च्युत नहीं होने देना स्थितिकरण अंग है । जिन प्रणीत धर्मरूप अमृत में सदा अनुराग रखना वात्सल्य है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र स्वरूप रत्नत्रय के प्रभाव से अपने आत्माका प्रकाशन करना प्रभावना अंग है। ज्ञानादिगुण और ज्ञानी आदि जनों में आदर करना अथवा कषायों से निवृत्त होना विनय है उस विनय से युक्त होना विनय सम्पन्नता कहलाती है। अहिंसा आदि व्रत हैं, और उन व्रतोंको पालन करने के लिये क्रोधादिका त्याग करना शील कहलाता है, शील और व्रतों में मन वचन कायकी निर्दोष प्रवृत्ति का होना शीलवतेष्वनतिचार है। अनवरत को अभीक्ष्ण कहते हैं, मतिज्ञान आदि भेद वाला परोक्ष और प्रत्यक्षरूप ज्ञान है उसकी भावना में सदा उपयोग लगाना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहलाता है। ज्ञानका उपयोग ज्ञानोपयोग है । संसार के दु.खों से भय होना संवेग है । ज्ञानोपयोग और संवेग पदोंमें पहले द्वन्द्व समास करना, फिर अभीक्ष्ण शब्द के साथ उनका कर्म धारय समास करना,