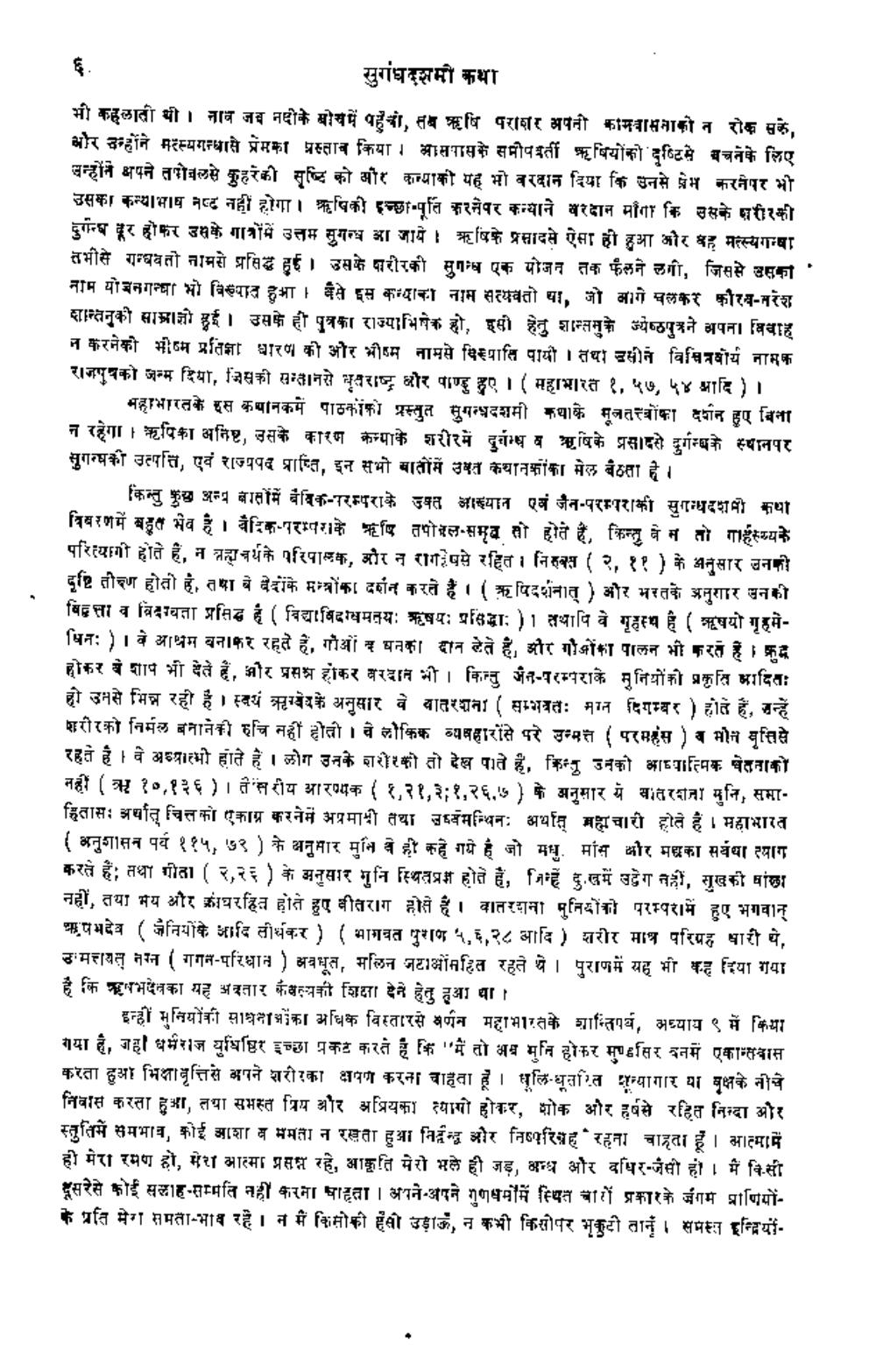________________
सुगंधदशमी कथा भी कहलाती थी। नाव जब नदीके खोचमें पहुँची, सब ऋषि पराशर अपनी कामवासनाको न रोक सके, और उन्होंने मत्स्यगन्धासे प्रेमका प्रस्ताव किया। आसपास के समीपवर्ती ऋषियोंको दृष्टिमे बचने के लिए उन्होंने अपने तोवलसे कुहरेकी सृष्टि को और कन्याकी यह भी वरदान दिया कि उनसे प्रेम करनेपर भी उसका कन्याभाष नष्ट नहीं होगा। ऋषिकी इच्छा पूर्ति करनेपर कन्याने वरदान मांगा कि उसके शरीरकी दुर्गन्ध दूर होकर उसके गात्रों में उत्तम सुगन्ध आ जाये । ऋषिके प्रसादसे ऐसा ही हुआ और वह मत्स्यगन्धा तभीसे गन्धव तो नामसे प्रसिद्ध हुई। उसके पारीरकी सुगन्ध एक योजन तक फैलने लगी, जिससे उसका नाम योजनगन्धा भो विख्यात हुआ। वैसे इस कन्याका नाम सत्यवतो था, जो आगे चलकर कौरव-नरेश शान्तनुको साम्राज्ञो हुई। उसके ही पुत्रका राज्याभिषेक हो, इसी हेतु शान्तमुके ज्येष्ठपुत्र ने अपना विवाह न करनेको भीष्म प्रतिज्ञा धारण की ओर भीडम नामसे विस्थाति पायो । तथा उसीने विचित्रवीर्य नामक राजपुषको जन्म दिया, जिसकी सन्तानसे धृतराष्ट्र और पाण्डु हुए । ( महाभारत १, ५७, ५४ आदि)।
__ महाभारतके इस कथानकमें पाठकोंको प्रस्तुत सुगन्धदशमी कथाके मूलतत्त्वोंका दर्शन हुए बिना न रहेगा। ऋपिका अनिष्ट, उसके कारण कन्याके शरीरमै दुर्गन्ध व ऋषिके प्रसादसे दुर्गन्धके स्थानपर सुगन्धकी उत्पत्ति, एवं राज्यपद प्राप्ति, इन सभी बातों में उक्त कथानकोंका मेल बैठता है।
किन्तु कुछ अन्य बातोंमें बैविक-परम्पराके उक्त आख्यान एवं जैन-परम्पराकी सुगन्धदशमी कथा विवरण में बहुत भेव है । वैदिक परम्पराके ऋषि तपोरल-समृब तो होते हैं, किन्तु वे म तो गार्हस्थ्यके परित्यागी होते हैं, न ब्रह्मचर्य के परिपालक, और न रागोषसे रहित । निरुक्स ( २, ११ ) के अनुसार उनकी दृष्टि तीक्ष्ण होती है, तथा बे वेदोंके मन्त्रोंका दर्शन करते हैं । ( ऋषिदर्शनात् ) और भरतके अनुसार उनकी विद्वत्ता व विदश्यता प्रसिद्ध है ( विद्याविदग्धमतयः ऋषयः प्रसिद्धाः )। तथापि वे गृहस्थ है ( ऋषयो गृहमेपिनः ) । वे आश्रम बनाकर रहते हैं, गौओं व घनका दान लेते हैं, और गौओंका पालन भी करते हैं। क्रुद्ध होकर वे शाप भी देते हैं, और प्रसन्न होकर वरदान भी। किन्तु जैन-परम्पराके मुनियों को प्रकृति मादितः हो उनसे भिन्न रही है। स्वयं ऋग्वेरके अनुसार वे वातरशना ( सम्भवतः मग्न दिगम्बर ) होते हैं, उन्हें शरीरको निर्मल बनाने की रुचि नहीं होती। वे लौकिक व्यवहारोंसे परे उन्मत्त ( परमहंस ) व मोन सिसे रहते है । वे अध्यात्मी होते हैं । लोग उनके शरीर को तो देख पाते है, किन्तु उनको आध्यात्मिक चेतनाको नहीं ( ऋ१०,१३६ ) । तेसरीय आरण्यक ( १,२१,३,१,२६.७ ) के अनुसार ये बात रयाना मुनि, समाहितासः अर्थात् चित्त को एकाग्र करनेमें अप्रमाथी तथा उध्वमन्थिनः अर्थात् ब्रह्मचारी होते हैं । महाभारत ( अनुशासन पर्व ११५, ७२ ) के अनुसार मुभि वे ही कहे गये है जो मधु. मांस और मछका सर्वथा त्याग करते हैं; तथा गीता ( २,२६ ) के अनुसार मुनि स्थितप्रज्ञ होते हैं, जिन्हें दु.खमें उद्वेग नहीं, सुख की पांछा नहीं, तया भय और कंाघरहित होते हुए वीतराग होते हैं। वातरदाना मुनियोंको परम्परामें हुए भगवान् ऋषभदेव (जैनियोंके आदि तीर्थकर ) ( भागवत पुराण ५,६,२८ आदि ) शरीर मात्र परिग्रह पारी थे, उमत्तयत् नग्न ( गगन-परिधान ) अवधूत, मलिन जटाओमहित रहते थे । पुराण में यह भी कह दिया गया है कि ऋषभदेवका यह अवतार कंबल्यकी शिक्षा देने हेतु हुआ था।
इन्हीं मुनियोंत्री साधनाओं का अधिक विस्तारसे वर्णन महाभारतके शान्तिपर्व, अध्याय ९ में किया गया है, जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर इच्छा प्रकट करते है कि "मैं तो अब मुनि होकर मुसिर वनमें एकान्तवास करता हुआ भिक्षावृत्ति से अपने शरीरका क्षपण करना चाहता हूँ। धूलि-धूतरित अन्यागार या वृक्षके नीचे निवास करता हुआ, तया समस्त प्रिय और अप्रियका त्यागो होकर, शोक और हर्षसे रहित निन्दा और स्तुतिमें समभाव, कोई आशा व ममता न रखता हुआ निन्द्र और निष्परिग्रह रहना चाहता हूँ। आत्मा में ही मेरा रमण हो, मेरा आत्मा प्रसन्न रहे, आकृति मेरो भले ही जड़, अन्ध और दघिर-जैसी हो । मैं किसी दूसरेसे कोई सलाह-सम्मति नहीं करना चाहता । अपने-अपने गुणधर्मामें स्थित चारों प्रकारके जंगम प्राणियोंके प्रति मेग समता-भाव रहै । न मैं किमोकी हँसी उड़ाऊँ, न कभी किसीपर भुकुटी तानें। समस्त इन्द्रियों