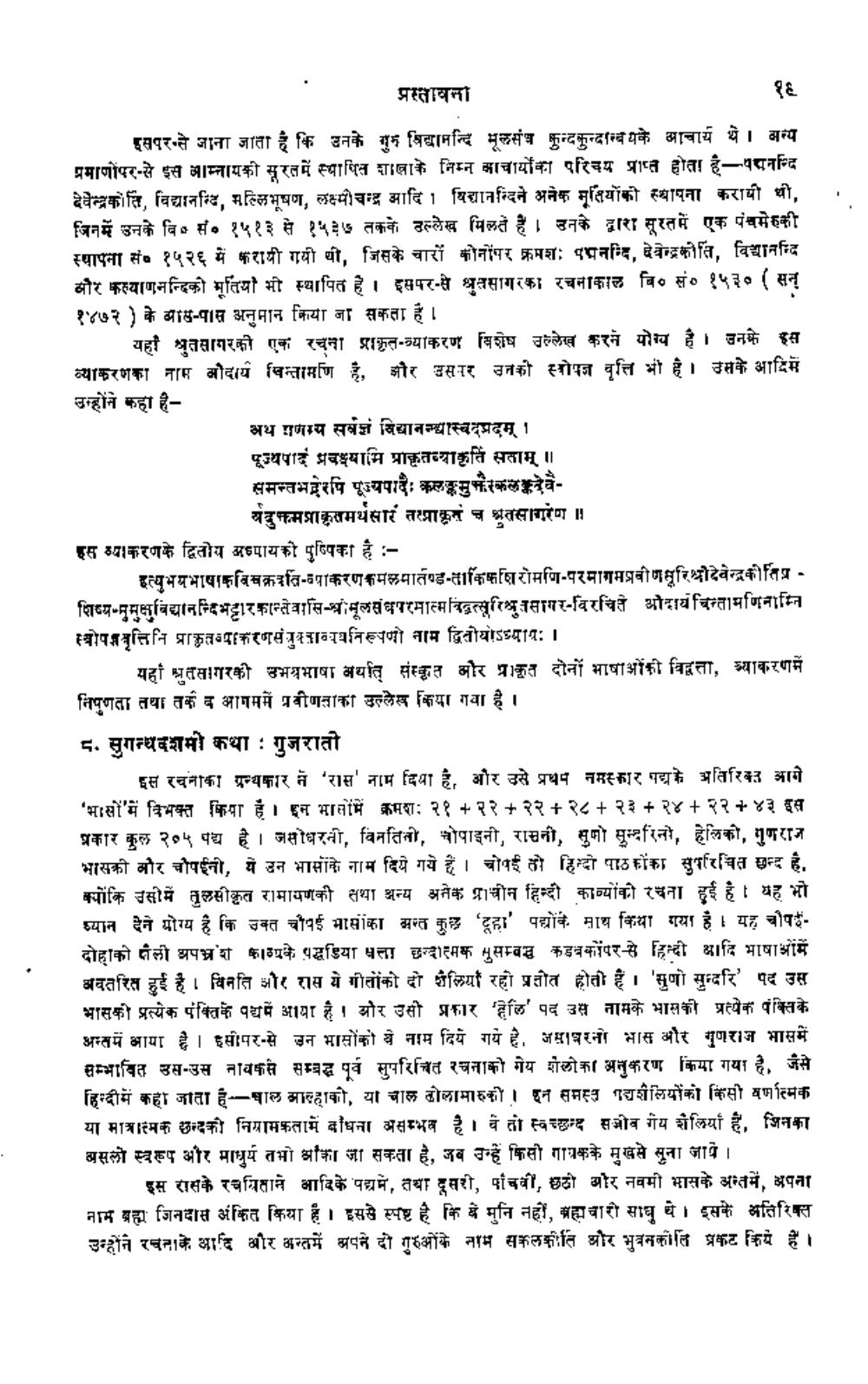________________
प्रस्तावना
१६
इसपरन्ते जाना जाता है कि उनके गुरु विद्यामन्दि मूलसंत्र कुन्दकुन्दान्ब यके आचार्य थे। अन्य प्रमाणोंपर-से इस आम्नायकी सूरत में स्थापित शाखाके निम्न काचार्योंका परिचय प्राप्त होता है-पपनन्दि देवेन्द्रकोति, विद्यानन्दि, मल्लिभूषण, लक्ष्मीचन्द्र आदि । विद्यानन्दिने अनेक मूर्तियोंको स्थापना करायी थी, जिनमें उनके वि सं० १५१३ से १५३७ तकके उल्लेख मिलते हैं। उनके द्वारा सूरत में एक पंचमेरुकी स्थापना सं० १५२६ में करायी गयी थी, जिसके चारों कोनोंपर क्रमशः पपनन्दि, देवेन्द्रकोति, विधानन्दि
और कल्याणमन्दिको भूतियो भी स्थापित है । इसपर-से श्रुतसागरका रचनाकाल वि० सं० १५३० ( सन् १४७२ ) के आस-पास अनुमान किया जा सकता है ।
यहाँ श्रुतसागर की एक रचना प्राकृत व्याकरण विशेष उल्लेख करने योग्य है। उनके इस व्याकरणका नाम औदाय चिन्तामणि है, और उस पर उनको स्वोपज्ञ वृत्ति भी है। उसके आदिम उन्होंने कहा है
अथ प्रणम्य सर्वज्ञं विद्यानन्धास्वदमदम् । पूज्यपाद प्रवक्ष्यामि प्राकृतव्याकृति सताम् ।। समन्तभद्रेरपि पूज्यपादै कलङ्कमुस्कलकदेव
यदुक्रमप्राकृतमर्थसारं तत्प्राकून च श्रुतसागरेण ॥ इस व्याकरणके द्वितीय अध्यायको पुष्पिका है :
इत्युभयभाषाकविश्चक्रवति-पाकरणकमलमार्तण्ड-ताकिफशिरोमणि-परमागमप्रवीणभूरिश्रौदेवेन्द्रकीर्तित - शिष्य-मुमुक्षुबिद्यानन्दिभट्टारकान्लेवासि-मूलसंधपरमात्मविद्वत्सरिश्रुतसागर-विरचिते ओदाय चिन्तामणिनाम्नि स्वोपावृत्तिनि प्राकृतव्याकरणसंयुक्ताव्यनिरूपणो नाम द्वितीयोऽध्यायः ।
यहां श्रुतसागरकी उभयभाषा अर्थात् संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओंकी विद्वत्ता, ज्याकरणमें निपुणता तथा तर्क व आगममें प्रवीणताका उल्लेख किया गया है । ८. सुगन्यवशमी कथा : गुजराती
इस रचनाका ग्रन्थकार में 'रास' नाम दिया है, और उसे प्रथम नमस्कार पद्मके अतिरिक्त आगे 'भासों में विभक्त किया है। इन भालों में क्रमश: २१ + २२ + २२ + २८ + २३ + २४ + २२ + ४३ इस प्रकार कुल २०५ पद्य है । जसोधरनी, विनतिनी, चोपाइनी, रामनी, सुणो सुन्दरिनो, हेलिको, गुणरान भासकी और चौपईनी, ये उन भासाँके नाम दिये गये हैं। चोपई तो हिन्दो पाठकोंका सुपरिचित छन्द है, क्योंकि उसी में तुलसीकृत रामायणकी तथा अन्य अनेक प्राचीन हिन्दी काव्योंको रचना हुई है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि उक्त चौपई भासीका अन्त कुछ 'टूहा' पयोंके. माथ किया गया है। यह चौपईदोहाको पौली अपभ्रश कायके पद्धडिया पत्ता छन्दात्मक मुसम्बद्ध कड़वकोंपर से हिन्दी आदि भाषाओं में अवतरित हुई है। विनति और रास ये गीतोंको दो शैलियाँ रहो प्रतीत होती हैं । 'सुणो सुन्दरि' पद उस भासको प्रत्येक पंक्तिके पद्यमें आया है । और उसी प्रकार 'हेलि' पद उस नामके भासको प्रत्येक पंक्तिके अन्समें आया है। इसीपर-से उन भासोंको वे नाम दिये गये है, सायरनो भास और गुणराज भासमें सम्भावित उस-उस नावफसे सम्बद्ध पूर्व सुपरिचित रचनाको मेय शैलोका अनुकरण किया गया है, जैसे हिन्दीमें कहा जाता है-चाल आल्हाको, या चाल ढोलामारुकी। इन समस्त गद्यशैलियोंको किसी वर्णात्मक या मात्रात्मक छन्दको नियामकतामें बाँधना असम्भव है। वे तो स्वच्छन्द सजीव जय शैलियाँ है, जिनका असलो स्वरूप और माधुर्य तभो आंका जा सकता है, जब उन्हें किसी गायकके मुखसे सुना जाये ।
इस रासके रचयिताने आदिके पद्म में, तथा दूसरी, पांचवीं, छठी और नवमी भासके अन्तमें, अपना नाम ब्रह्म जिनदास अंकित किया है। इससे स्पष्ट है कि में मुनि नहीं, ब्रह्मचारी साधु थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने रचनाके आदि और अन्तमें अपने दो गुरुओं के नाम सकलकीति और भुवनकोलि प्रकट किये हैं।