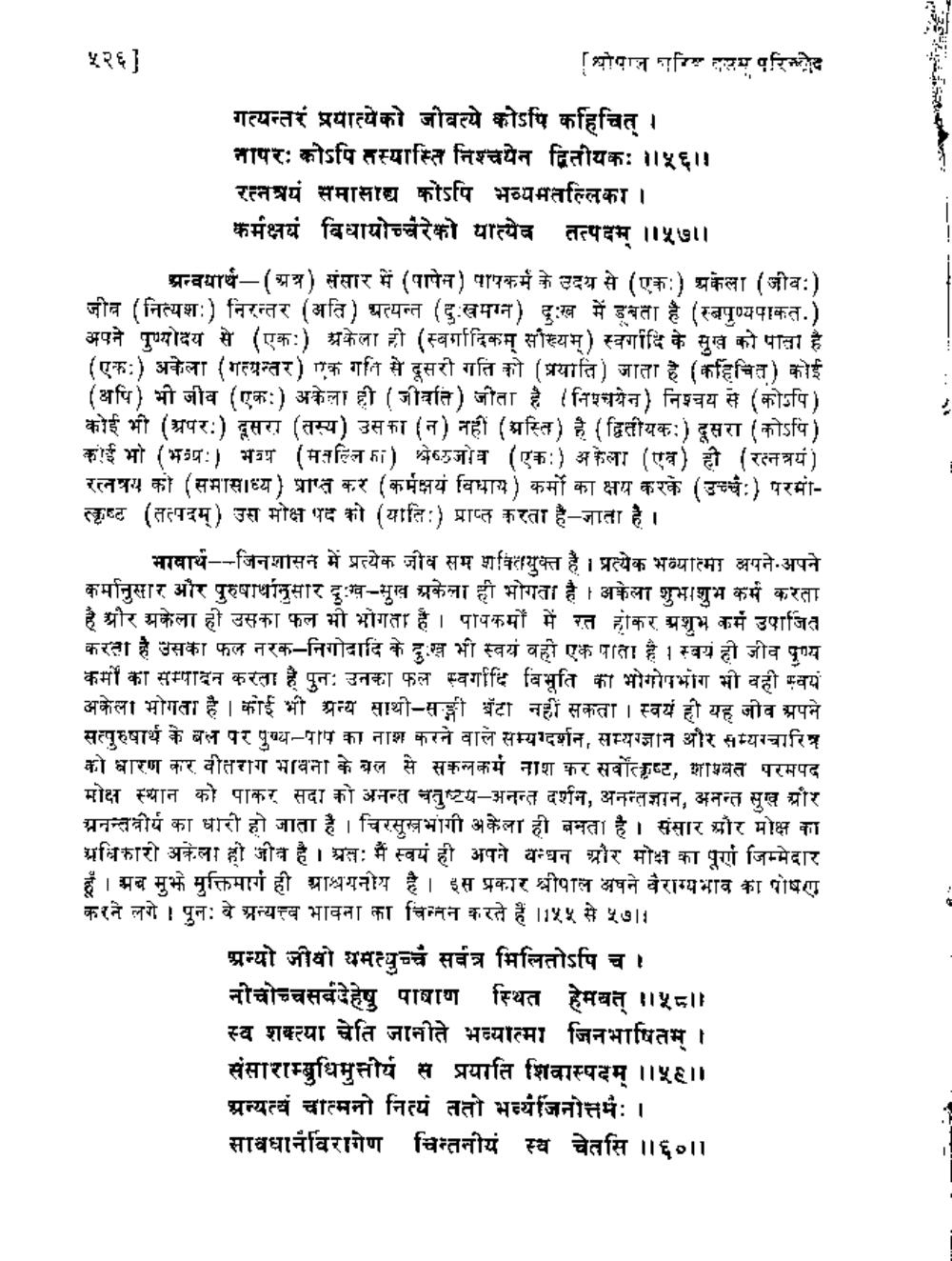________________
५२६]
योपाल रिसालम परिमोद
गत्यन्तरं प्रयात्येको जीवत्ये कोऽपि हिचित् । नापरः कोऽपि तस्यास्ति निश्चयेन द्वितीयकः ॥५६॥ रत्नत्रयं समासाद्य कोऽपि भव्यमल्लिका।
कर्मक्षयं विधायोच्चैरेको यात्येव तत्पदम् ॥५७।। अन्वयार्थ-(अत्र) संसार में (पापेन) पापकर्म के उदय से (एकः) अकेला (जीव:) जीव (नित्यशः) निरन्तर (अति) अत्यन्त (दुःखमग्न) दुःख में डुबता है (स्वपुण्यपाकत.) अपने पुण्योदय से (एकः) अकेला ही (स्वर्गादिकम् सौख्यम्) स्वर्गादि के सुख को पाता है (एक:) अकेला (गत्यन्तर) एक गति से दूसरी गति को (प्रयाति) जाता है (कहिचित) कोई (अपि) भी जीव (एक:) अकेला ही ( जीवति) जीता है (निश्चयेन) निश्चय से (कोऽपि ) कोई भी (अपर:) दूसरा (तस्य) उसका (न) नहीं (अस्ति) है (द्वितीयकः) दूसरा (कोऽपि) कोई भो (भव्यः) भव्य (मतल्लिा ) श्रेष्ठजोव (एक:) अकेला (एव) ही (रत्नत्रयं) रत्नत्रय को (समासाध्य ) प्राप्त कर (कर्मक्षयं विधाय) कमों का क्षय करके (उच्चः) परमीस्कृष्ट (सत्पदम् ) उस मोक्ष पद को (याति:) प्राप्त करता है-जाता है ।
भावार्थ---जिनशासन में प्रत्येक जीव सम शक्तियुक्त है। प्रत्येक भव्यात्मा अपने अपने कर्मानुसार और पुरुषार्थानुसार दुःख-सुख अकेला ही भोगता है । अकेला शुभाशुभ कर्म करता है और अकेला ही उसका फल भी भोगता है। पापकों में रत होकर अशुभ कर्म उपाजित करता है उसका फल नरक-निगोदादि के दुःख भी स्वयं वही एक पाता है । स्वयं ही जीव पुण्य कर्मों का सम्पादन करता है पुन: उनका फल स्वर्गादि विभूति का भोगोपभोग भी वही स्वयं अकेला भोगता है। कोई भी अन्य साथी-सङ्गी बँटा नहीं सकता । स्वयं ही यह जीव अपने सत्पुरुषार्थ के बल पर पुण्य-पाप का नाश करने वाले सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र को धारण कर वीतराग भावना के बल से सकल कर्म नाश कर सर्वोत्कृष्ट, शाश्वत परमपद मोक्ष स्थान को पाकर सदा को अनन्त चतुष्टय-अनन्त दर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्त सुख और अनन्तवीर्य का धारी हो जाता है । चिरसुखभागी अकेला ही बनता है। संसार और मोक्ष का अधिकारी अकेला ही जीव है। अत: मैं स्वयं ही अपने बन्धन और मोक्ष का पूर्ण जिम्मेदार हूँ । अब मुझे मुक्तिमार्ग ही प्राश्चयनीय है। इस प्रकार श्रीपाल अपने वैराग्यभाव का पोषण करने लगे। पुनः वे अन्यत्त्व भावना का चिन्तन करते हैं ।१५५ से ५७।।
अन्यो जीवो यमत्युच्च सर्वत्र भिलितोऽपि च । नीचोच्चसर्वदेहेषु पाषाण स्थित हेमवत् ॥५॥ स्व शक्त्या चेति जानीते भच्यात्मा जिनभाषितम् । संसाराम्बुधिमुत्तीर्य स प्रयाति शिवास्पदम् ।।५।। अन्यत्वं चात्मनो नित्यं ततो भन्यजिनोत्तमैः ।। सावधानविरागेण चिन्तनीयं स्व चेतसि ॥६॥