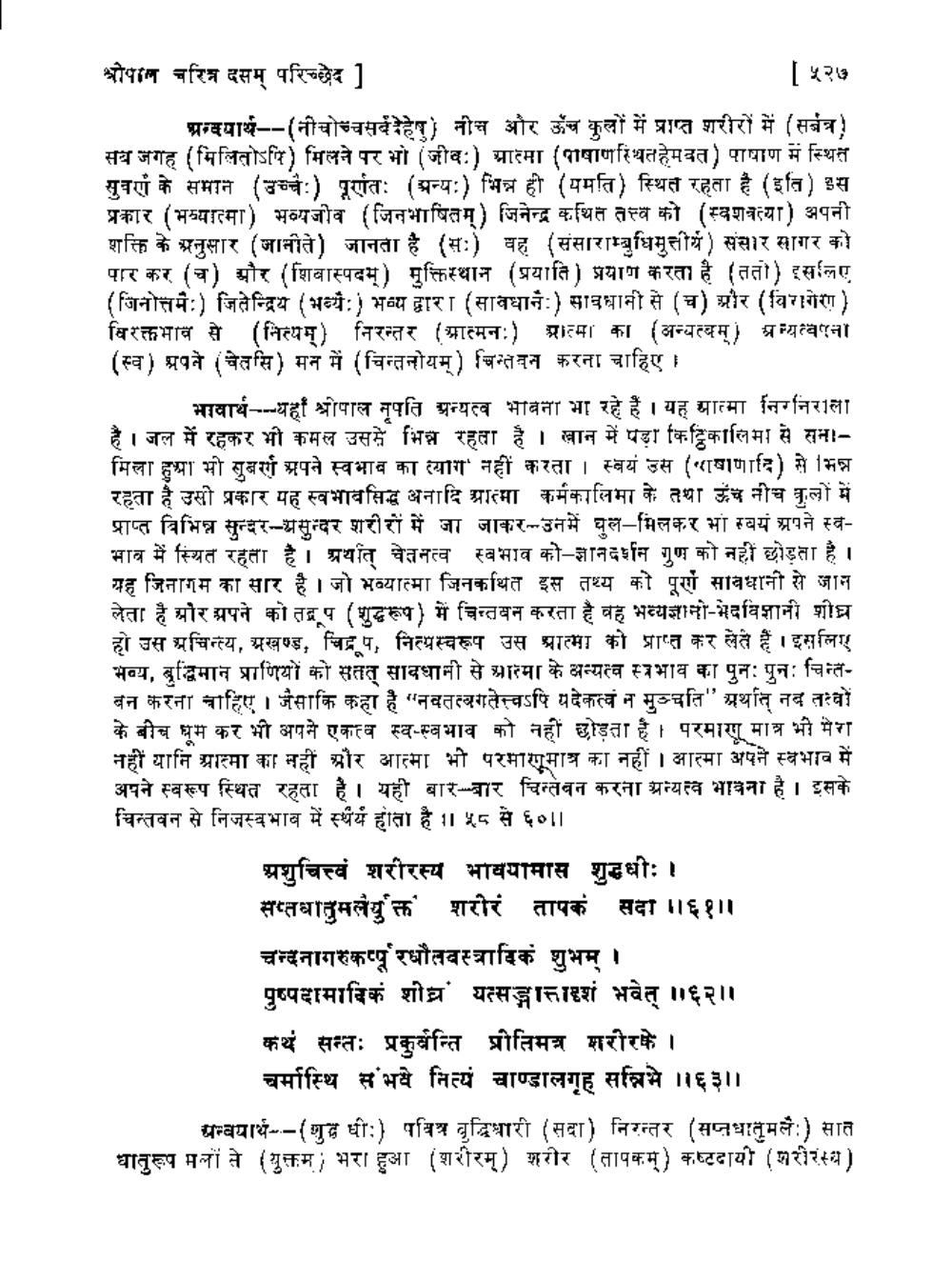________________
श्रीपाल चरित्र दसम् परिच्छेद ]
[ ५२७ अन्वयार्थ--(नीचोच्चसईदेहेष) नीच और ऊँच कुलों में प्राप्त शरीरों में (सर्वत्र सब जगह (मिलितोऽपि) मिलने पर भो (जीव:) आत्मा (पाषाणस्थित हेमवत) पाषाण में स्थित सुवर्ण के समान (उच्चैः) पूर्णतः (अन्यः) भिन्न ही (यमति) स्थित रहता है (इति) इस प्रकार (भव्यात्मा) भव्यजीव (जिनभाषितम्) जिनेन्द्र कथित तत्व को (स्वशत्रत्या) अपनी शक्ति के अनुसार (जानीते) जानता है (सः) वह (संसाराम्बुधिमुत्तीर्य) संसार सागर को पार कर (च) और (शिवास्पदम्) मुक्तिस्थान (प्रयाति ) प्रयाण करता है (ततो) इसलिए (जिनोत्तमैः) जितेन्द्रिय (भव्यैः) भव्य द्वारा (सावधानः) सावधानी से (च) और (विरागरण) विरक्तभाव से (नित्यम्) निरन्तर (आत्मनः) आत्मा का (अन्यत्वम्) अन्यत्वाना (स्व) अपने (चेतसि ) मन में (चिन्तनोयम् ) चिन्तवन करना चाहिए।
भावार्थ---यहाँ श्रीपाल मपति अन्यत्व भावना भा रहे हैं । यह यात्मा निरनिराला है । जल में रहकर भी कमल उसमें भिन्न रहता है । खान में पड़ा किटिकालिमा से सनामिला हुआ भी सुबर्ग अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता। स्वयं उस (षाणादि) से भिन्न रहता है उसी प्रकार पह स्वभाबसिद्ध अनादि अात्मा कर्मकालिमा के तथा ऊंच नीच वृलों में प्राप्त विभिन्न सुन्दर-असुन्दर शरीरों में जा जाकर उनमें घुल-मिलकर भा स्वयं अपने स्वभाव में स्थित रहता है। अर्थात् चेतनत्व स्वभाव को-ज्ञानदर्शन गुण को नहीं छोड़ता है। यह जिनागम का सार है। जो भव्यात्मा जिनकथित इस तथ्य को पूर्ण सावधानी से जान लेता है और अपने को तद् प (शुद्धरूप) में चिन्तयन करता है वह भव्यज्ञानो-भेदविज्ञानी शीघ्र हो उस अचिन्त्य, अखण्ड, चिद्र प, नित्यस्वरूप उस प्रात्मा को प्राप्त कर लेते हैं । इसलिए भव्य, बुद्धिमान प्राणियों को सतत् सावधानी से प्रात्मा के अन्यत्व स्त्रभाव का पुन: पुन: चिन्तबन करना चाहिए । जैसाकि कहा है पनवतत्वगतेवऽपि यदेकत्वं न मुञ्चति" अर्थात् नब तत्वों के बीच धूम कर भी अपने एकात्व स्व-स्वभाव को नहीं छोड़ता है। परमारण मात्र भी मेरा नहीं यानि प्रात्मा का नहीं और आत्मा भी परमाणूमात्र का नहीं । आत्मा अपने स्वभाव में अपने स्वरूप स्थित रहता है। यही बार-बार चिन्तेवन करना अन्यत्व भावना है। इसके चिन्तवन से निजस्वभाव में स्थर्य होता है ।। ५.८ से ६०||
अशुचित्त्वं शरीरस्य भावयामास शुद्धधीः । सप्तधातुमलयुक्त' शरीरं तापकं सदा ।।६१॥ चन्दनागरुकप्रधौलवस्त्रादिक शुभम् । पुष्पदामाविकं शीघ्र यत्सङ्गात्ताशं भवेत् ॥६२॥ कथं सन्तः प्रकुर्वन्ति प्रीतिमत्र शरीरके ।
चर्मास्थि संभवे नित्यं चाण्डालगृह सन्निभे ॥६३।।
अन्वयार्थ---(शुद्ध धी:) पवित्र बुद्धिधारी (सदा) निरन्तर (सप्तधातुमलैः) सात धातुरूप मला ते (युक्तम | भरा हुआ (शरीरम् ) शरीर (तापकम् ) कष्टदायी (शरीरस्य)