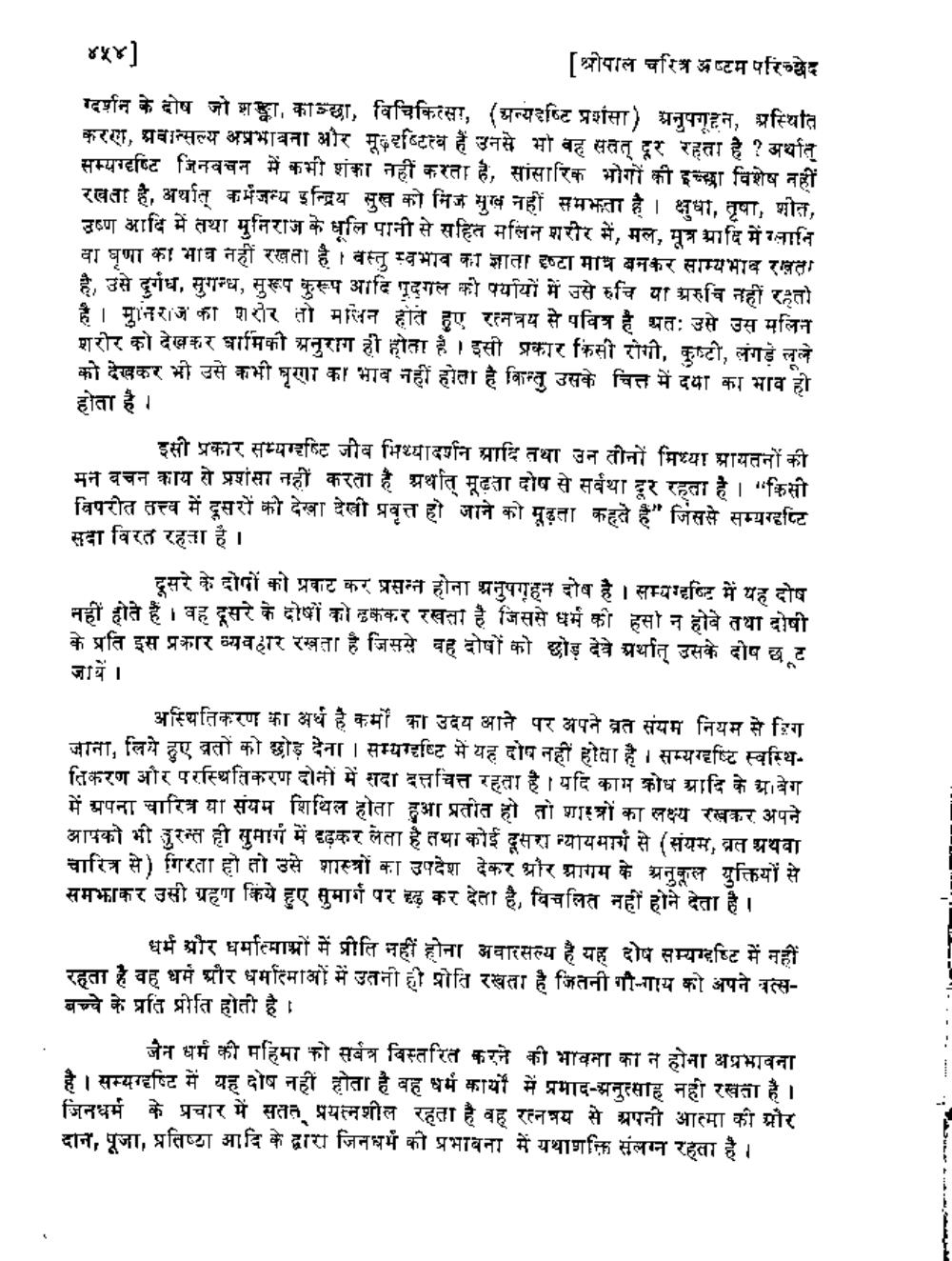________________
४५४]
[श्रीपाल चरित्र अष्टम परिच्छेद ग्दर्शन के दोष जो शङ्का, काञ्छा, विचिकित्सा, (अन्यदृष्टि प्रशंसा) अनुपगहन, अस्थिति करण, अचान्सल्य अप्रभावना और मूढष्टित्व हैं उनसे भो वह सतत् दूर रहता है ? अर्थात सम्यग्दृष्टि जिनवचन में कभी शंका नहीं करता है, सांसारिक भोगों की इच्छा विशेष नहीं रखता है, अर्थात् कर्मजन्य इन्द्रिय सुख को निज मुख नहीं समझता है । क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण आदि में तथा मुनिराज के धूलि पानी से सहित मलिन शरीर में, मल, मूत्र आदि में ग्लानि वा घृणा का भाव नहीं रखता है । वस्तु स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा मात्र बनकर साम्य भाव रखता है, उसे दुर्गध, सुगन्ध, सुरूप कुरूप आदि पदगल को पर्यायों में उसे रुचि या अरुचि नहीं रहतो है। मुनिराज का शरीर तो मलिन होते हुए रत्नत्रय से पवित्र है अत: उसे उस मलिन शरीर को देखकर धामिकी अनुराग ही होता है । इसी प्रकार किसी रोगी, कुष्टी, लंगड़े लले को देखकर भी उसे कभी प्रेरणा का भाव नहीं होता है किन्तु उसके चित्त में दया का भाव ही होता है।
इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यादर्शन आदि तथा उन तीनों मिथ्या पायतनों की मन बचन काय से प्रशंसा नहीं करता है अर्थात् मूढता दोष से सर्वथा दूर रहता है । "किसी विपरीत तत्त्व में दूसरों को देखा देखी प्रवृत्त हो जाने को मूढ़ता कहते हैं" जिससे सम्यग्दृष्टि सदा विरत रहता है।
दूसरे के दोषों को प्रवाट कर प्रसन्न होना अनुपगृहन दोष है । सम्यग्दृष्टि में यह दोष नहीं होते हैं। वह दूसरे के दोषों को ढककर रखता है जिससे धर्म की हसो न होबे तथा दोषी के प्रति इस प्रकार व्यवहार रखता है जिसमे वह दोषों को छोड़ देवे अर्थात् उसके दोष छ ट जायें।
___अस्थितिकरण का अर्थ है कर्मों का उदय आने पर अपने व्रत संयम नियम से हिंग जाना, लिये हुए व्रतों को छोड़ देना । सम्यग्दृष्टि में यह दोष नहीं होता है। सम्यग्दृष्टि स्वस्थितिकरण और परस्थितिकरण दोनों में सदा दत्तचित्त रहता है। यदि काम क्रोध प्रादि के पावेग में अपना चारित्र या संयम शिथिल होता हुआ प्रतीत हो तो शास्त्रों का लक्ष्य रखकर अपने आपको भी तुरन्त ही सुमार्ग में दृढ़कर लेता है तथा कोई दूसरा न्यायमार्ग से (संयम, व्रत अथवा चारित्र से) गिरता हो तो उसे शास्त्रों का उपदेश देकर और प्रागम के अनुकूल युक्तियों से समझाकर उसी ग्रहण किये हुए सुमार्ग पर दृढ़ कर देता है, विचलित नहीं होने देता है।
धर्म और धर्मात्मानों में प्रीति नहीं होना अवारसल्य है यह दोष सम्यग्दृष्टि में नहीं रहता है वह धर्म और धर्मात्माओं में उतनी ही प्रोति रखता है जितनी गौ-गाय को अपने वत्सबच्चे के प्रति प्रीति होती है।
जैन धर्म की महिमा को सर्वत्र विस्तरित करने की भावना का न होना अप्रभावना है। सम्यग्दृष्टि में यह दोष नहीं होता है वह धर्म कार्यों में प्रमाद-अनुत्साह नही रखता है। जिनधर्म के प्रचार में सतत प्रयत्नशील रहता है वह रत्नत्रय से अपनी आत्मा की और दान, पूजा, प्रतिष्ठा आदि के द्वारा जिनधर्म को प्रभावना में यथाशक्ति संलग्न रहता है।