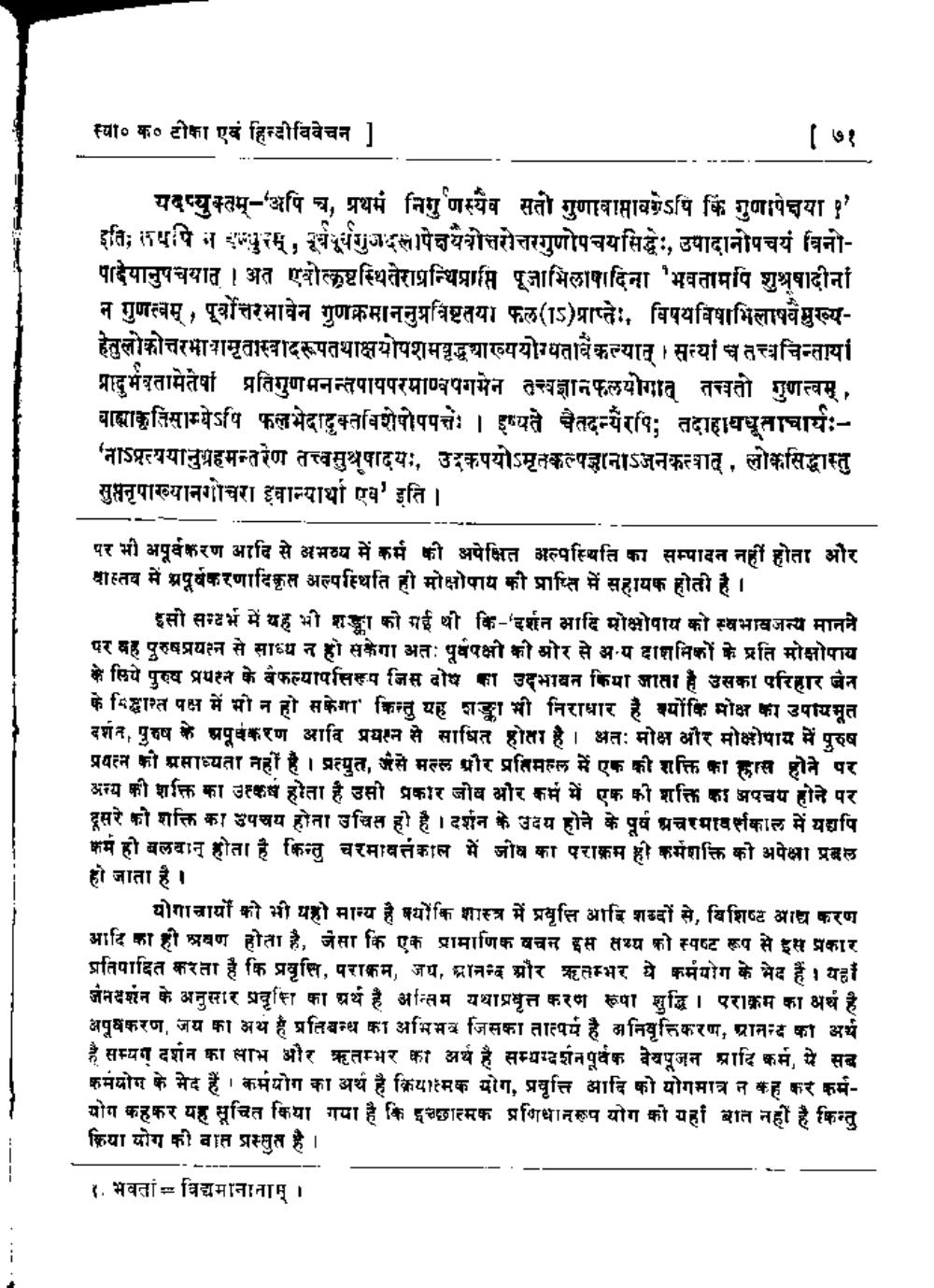________________
स्या० क० टीका एवं हिन्दीविवेचन ]
यदप्युक्तम्-'अपि च, प्रथमं निगुणस्यैव सतो गुणावातावणेऽपि किं गुणापेक्षया ?' इति; रुपपि न सम्पुरम् , पूर्वगुजदलापेक्षयोत्तरोत्तरगुणोपचयसिद्धेः, उपादानोपचयं विनोपादेयानुपचयात । अत एवोत्कृष्ट स्थितेराप्रन्धिप्राप्ति पूजाभिलाषादिना 'भवतामपि शुश्रषादीनां न गुणत्वम् , पूर्वोत्तरभावेन गुणक्रमाननुप्रविष्टतया फल(राज)प्राप्तः, विषयविषाभिलापमुख्यहेतुलोकोत्तरभाषामृतास्वादरूपतथाक्षयोपशमवृद्धयाख्ययोग्यताकल्यान् । सत्यां च तत्त्वचिन्तायां प्रादुर्भवतामेतेषां प्रतिगुणमनन्तपायपरमाण्वपगमेन तत्वज्ञानफलयोगात तवतो गुणत्वम् , बाझाकृतिसाम्येऽपि फलभेदादुक्तविशेपोपपत्तेः । इष्यते चैतदन्यैरपि; तदाहायधूताचार्य:'नाऽप्रत्ययानुग्रहमन्तरेण तत्त्वसुश्रुषादयः, उदकपयोऽमृतकल्पज्ञानाऽजनकत्वाद , लोकसिद्धास्तु सुप्शनृपाख्यानगोचरा इवान्यार्था एव' इति।।
पर भी अपूर्वकरण आदि से अभव्य में कर्म की अपेक्षित अल्पस्थिति का सम्पादन नहीं होता और वास्तव में अपूर्वकरणादिकृत अल्पस्थिति ही मोक्षोपाय की प्राप्ति में सहायक होती है ।
इसी सन्दर्भ में यह भी शङ्गा को गई थी कि-'दर्शन मादि मोक्षोपाय को स्वभावजन्य मानने पर वह पुरुषप्रयत्न से साध्य न हो सकेगा अतः पूर्वपक्षी की ओर से अ य दाशनिकों के प्रति मोक्षोपाय के लिये पुरुष प्रयत्न के वैफल्यापतिहप जिस दोष का उदभाबन किया जाता है उसका परिहार जैन के सिद्धान्त पक्ष में मो न हो सकेगा किन्तु यह शङ्का भी निराधार है क्योंकि मोक्ष का उपायभूत दर्शन, पुरुष के अपूर्वकरण आदि प्रयत्न से साधित होता है। अतः मोक्ष और मोक्षोपाय में पुरुष प्रयत्न को प्रसाध्यता नहीं है। प्रत्युत, जैसे मल्ल और प्रतिमल्ल में एक की शक्ति का ह्रास होने पर अन्य की शक्ति का उत्कर्ष होता है उसी प्रकार जीव और कर्म में एक की शक्ति का अपचय होने पर दूसरे को शक्ति का उपयय होना उचित हो है । दर्शन के उदय होने के पूर्व प्रचारमावर्शकाल में यद्यपि कम हो बलवान होता है किन्तु चरमावर्तकाल में जीव का पराक्रम ही कर्मशक्ति को अपेक्षा प्रबल हो जाता है।
योगाचार्यों को भी यहो मान्य है क्योंकि शास्त्र में प्रवृत्ति आदि शब्दों से, बिशिष्ट आध करण आदि का ही प्रवण होता है, जैसा कि एक प्रामाणिक वचन इस तथ्य को स्पष्ट रूप से इस प्रकार प्रतिपादित करता है कि प्रवृत्ति, पराक्रम, जय, मानन्द और ऋतम्भर ये कर्मयोग के भेद हैं। यहाँ जैनदर्शन के अनुसार प्रवृति का अर्थ है अन्तिम यथाप्रवृत्त करण रूपा शुद्धि । पराक्रम का अर्थ है अपूर्वकरण, जय का अथ है प्रतिबन्ध का अभिमव जिसका तात्पर्य है अनिवृक्तिकरण, प्रानन्द का अर्थ है सम्यग दर्शन का लाभ और ऋतम्भर का अर्थ है सम्यग्दर्शन पूर्वक वेयपूजन प्रादि कर्म, ये सब कमयोग के भेद हैं । कर्मयोग का अर्थ है क्रियात्मक योग, प्रवृत्ति आदि को योगमात्र न कह कर कर्मयोग कहकर यह सूचित किया गया है कि इच्छात्मक प्रणिधानरूप योग को यहां बात नहीं है किन्तु किया योग की वात प्रस्तुत है । १. भवतां विद्यमानानाम् ।