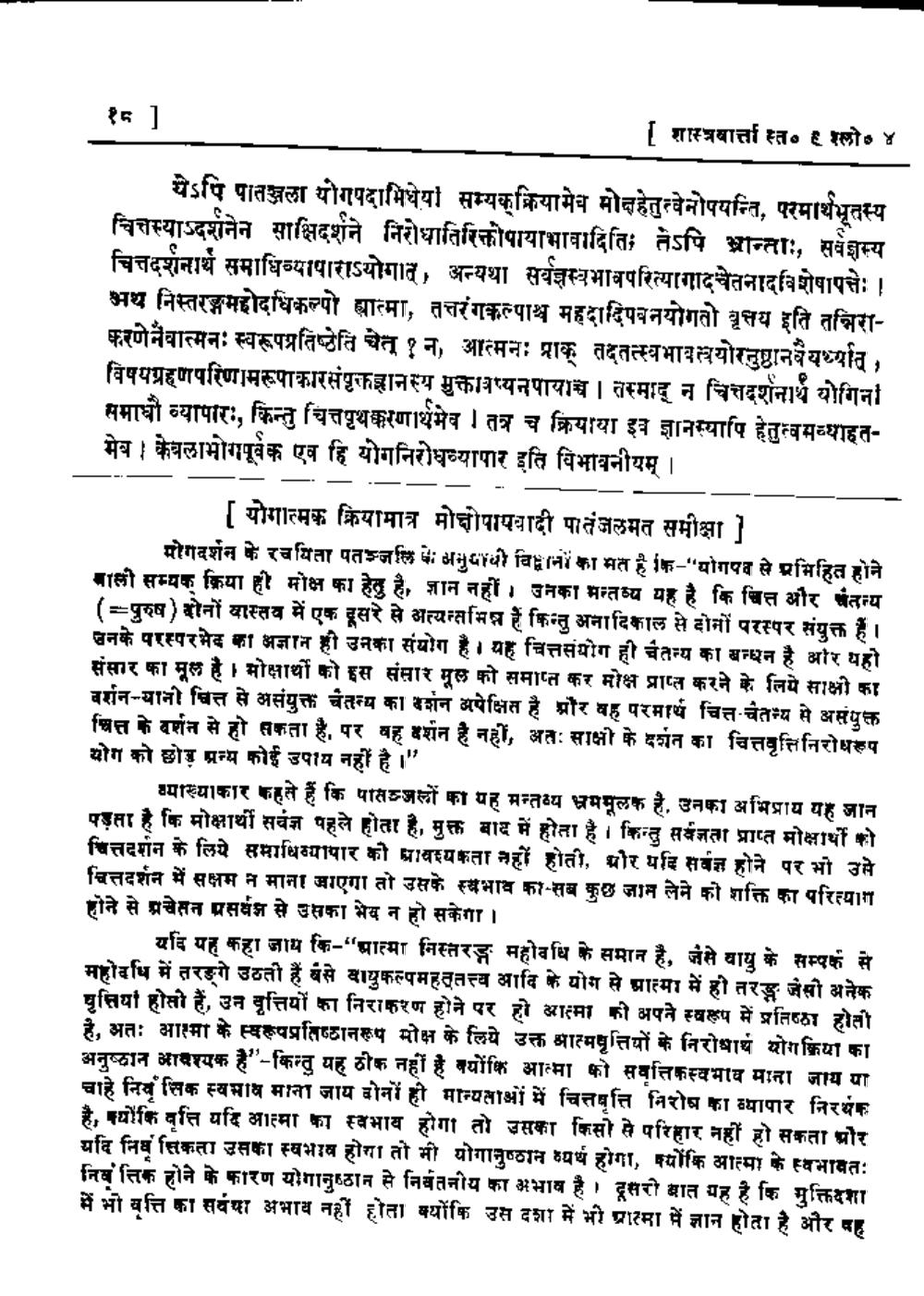________________
१८ ]
[ शास्त्रया स्त०६ श्लो. ४
येऽपि पातञ्जला योगपदाभिधेयो सम्यक्रियामेव मोक्षहेतुत्वेनोपयन्ति, परमार्थभूतस्य चित्तस्याऽदर्शनेन साक्षिदर्शने निरोधातिरिक्तोपायाभावादितिः तेऽपि भ्रान्ताः, सर्वज्ञस्य चित्तदर्शनार्थ समाधिव्यापाराऽयोगात् , अन्यथा सर्वज्ञस्वभावपरित्यागादचेतनादविशेषापत्तेः । अथ निस्तरङ्गमहोदधिकल्पो ह्यात्मा, तत्तरंगकल्पाच महदादिपवनयोगतो वृत्तय इति तन्निराफरणेनैवात्मनः स्वरूपप्रतिष्ठेति चेत् १ न, आत्मनः प्राक् तदतत्स्वभावत्वयोरनुष्ठानयाद , विषयग्रहणपरिणामरूपाकारसंपृक्तज्ञानस्य मुक्तावप्यनपायाच । तस्माद् न चित्तदर्शनार्थ योगिनी समाधौ व्यापारः, किन्तु चित्तपृथक्करणार्थमेव । तत्र च क्रियाया इव ज्ञानस्यापि हेतुत्वमव्याहतमेव । केवलाभोगपूर्वक एव हि योगनिरोधव्यापार इति विभावनीयम् ।
[ योगात्मक क्रियामात्र मोक्षोपायवादी पातंजलमत समीक्षा ] मोगदर्शन के रचयिता पतञ्जलि के अनुपाधी विद्वानों का मत है क-"योगपत से प्रमिहित होने माली सम्यक क्रिया ही मोक्ष का हेतु है, ज्ञान नहीं। उनका मन्तव्य यह है कि चित्त और चैतन्य (पुरुष) दोनों वास्तव में एक दूसरे से अत्यन्तभिन्न हैं किन्तु अनादिकाल से दोनों परस्पर संयुक्त हैं। जनके परस्परभेद का अज्ञान ही उनका संयोग है। यह चित्तसंयोग ही चैतन्य का बन्धन है और यहो संसार का मूल है। मोक्षार्थो को इस संसार मूल को समाप्त कर मोक्ष प्राप्त करने के लिये साक्षी का वर्शन-यानी चित्त से असंयुक्त चैतन्य का दर्शन अपेक्षित है और वह परमार्थ चित्त-चैतन्य से असंयुक्त चित्त के दर्शन से हो सकता है, पर वह दर्शन है नहीं, अतः साक्षी के दर्शन का चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग को छोड़ अन्य कोई उपाय नहीं है।"
व्याख्याकार कहते हैं कि पातञ्जलों का यह मन्तव्य भ्रममूलक है, उनका अभिप्राय यह जान पड़ता है कि मोक्षार्थी सर्वज्ञ पहले होता है, मुक्त बाद में होता है। किन्तु सर्वज्ञता प्राप्त मोक्षार्थी को चित्तदर्शन के लिये समाधिव्यापार को प्रावश्यकता नहीं होती, और यदि सर्वज्ञ होने पर भी उसे चित्तदर्शन में सक्षम न माना जाएगा तो उसके स्वभाव का सब कुछ जान लेने को शक्ति का परित्याग होने से प्रचेतन प्रसर्वज्ञ से उसका भेव न हो सकेगा।
यदि यह कहा जाय कि-"मात्मा निस्तरङ्ग महोवधि के समान है, जैसे वायु के सम्पर्क से माहोदधि में तरङगे उठती हैं बसे वायुकल्पमहत्तत्त्व आदि के योग से प्रात्मा में हो तरङ्ग जैसी अनेक त्तियां होती हैं, उन वृत्तियों का निराकरण होने पर हो आत्मा को अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा होती है, अतः आस्मा के स्वरूपप्रतिष्ठानरूप मोक्ष के लिये उक्त आत्मवृत्तियों के निरोधार्थ योग क्रिया का अनुष्ठान आवश्यक है"-किन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि आत्मा को सवृत्तिकस्वभाव माना जाय या चाहे निवंतिक स्वमाय माना जाय दोनों ही मान्यताओं में चित्तवृत्ति निरोष का व्यापार निरर्थक है, क्योंकि वृत्ति यदि आत्मा का स्वभाव होगा तो उसका किसी से परिहार नहीं हो सकता और यदि निर्षसिकता उसका स्वभाव होगा तो भी योगानुष्ठान व्यर्थ होगा, क्योंकि आत्मा के स्वभावत: नियंतिक होने के कारण योगानुष्ठान से निर्वतनीय का अभाव है। दूसरी बात यह है कि मुक्तिदशा में भी यत्ति का सर्वका अभाव नहीं होता क्योंकि उस दशा में भी प्रात्मा में ज्ञान होता है और वह