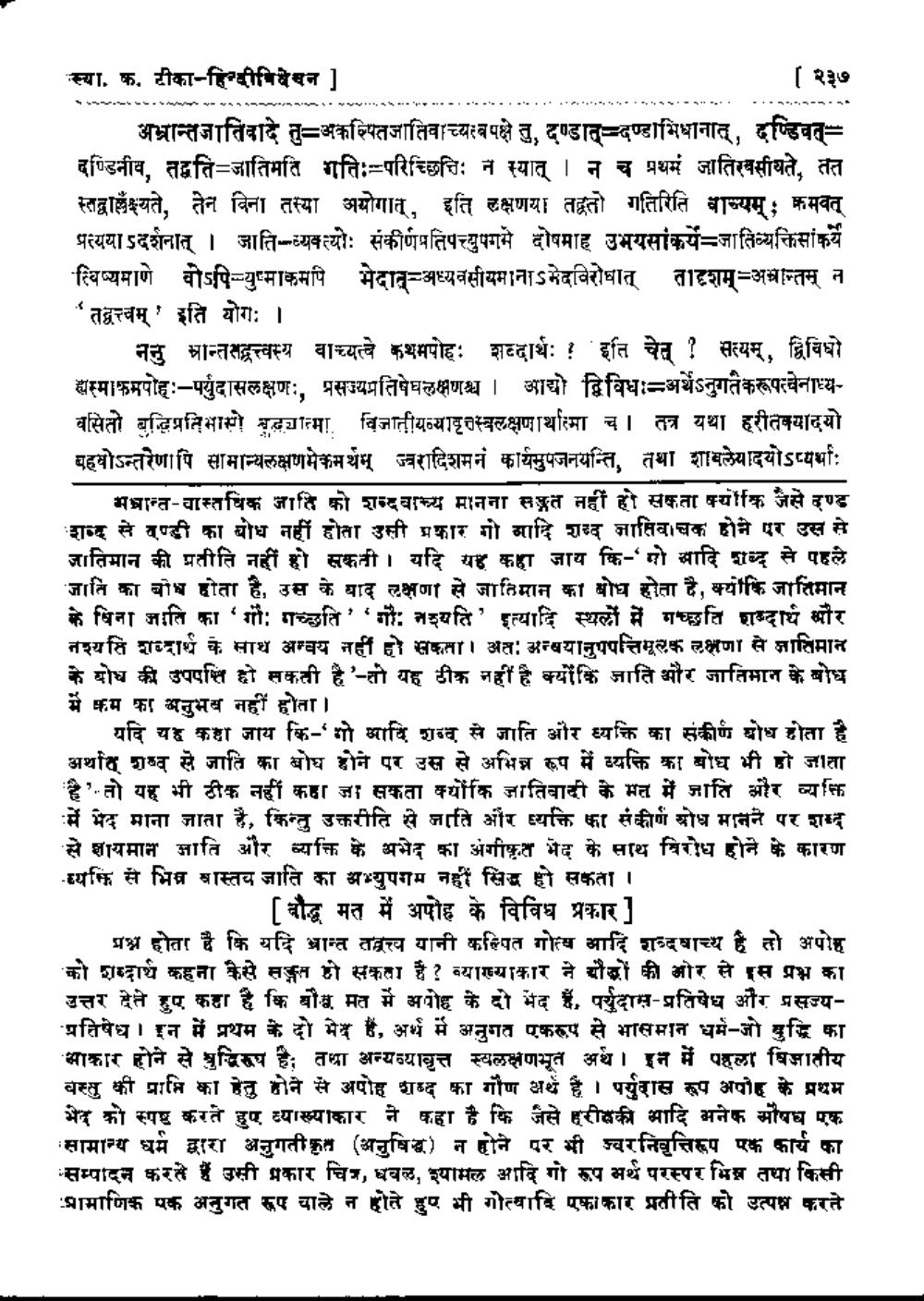________________
स्या. क. टीका-हिन्दीविवेचन ]
[ २३७ अभ्रान्तजातिवादे तु अस्पितजातिवाच्यस्त्रपक्षे तु, दण्डात् दण्डाभिधानात्, दण्डिवत्दण्डिनीव, तद्वति–जातिमति गतिः परिच्छित्तिः न स्यात् । न च प्रथमं जातिवसीयते, तत स्तवाल्लक्ष्यते, तेन विना तस्या अयोगात्, इति लक्षणया तद्वतो गतिरिति वाच्यम् : क्रमवत् प्रत्ययाऽदर्शनात् । जाति-व्यक्त्योः संकीर्णप्रतिपत्त्युपगमे दोषमाह उभयसांकर्ये जातिव्यक्तिसांकर्य विष्यमाणे वोऽपियुष्माकमपि भेदाअध्यवसीयमानाऽभेदविरोधात् तादृशम् अभ्रान्तम् न 'तद्वत्त्वम् । इति योगः ।
ननु भ्रान्तसत्त्वस्य वाच्यत्त्वे कथमपोहः शब्दार्थः ! इति चेत् ? सत्यम् , द्विविधो ह्यस्माकमपोहः-पर्युदासलक्षणः, प्रसज्यप्रतिषेघलक्षणश्च । आयो द्विविधा अर्थेऽनुगतकरूपत्वेनाध्यवसितो बुद्धिप्रतिभासो बुद्धधात्मा. विजातीयव्यावृत्तस्वलक्षणार्थात्मा च । तत्र यथा हरीतक्यादयो बहवोऽन्तरेणापि सामान्यलक्षणमेकमर्थम् ज्वरादिशमनं कार्यमुपजनयन्ति, तथा शायलेयादयोऽप्यर्थाः
भधान्त-वास्तविक जाति को शब्द वाच्य मानना सतत नहीं हो सकता क्योकि जैसे दण्ड शन्द से वण्डी का बोध नहीं होता उसी प्रकार गो आदि शब्द जातिवाचक होने पर उस से जातिमान की प्रतीति नहीं हो सकती। यदि यह कहा जाय कि-'यो आदि शब्द से पहले जाति का बोध होता है, उस के बाद लक्षणा से जातिमान का बोध होता है, क्योंकि जातिमान के धिना जाति का 'गो: गच्छति' 'गौ: नश्यति' इत्यादि स्थलों में गच्छति शब्दार्थ और नश्यप्ति शब्दार्थ के साथ अन्वय नहीं हो सकता। अतः अन्वयानुपपत्तिमूलक लक्षणा से जातिमान के बोध की उपपत्ति हो सकती है'-तो यह ठीक नहीं है क्योंकि जाति और जातिमान के बोध में कम का अनुभव नहीं होता।
यदि यह कहा जाय कि-'गो आदि शब्च से जाति और ध्यक्ति का संकीर्ण बोध होता है अदि शव से जाति का बोध होने पर उस से अभिन्न रूप में व्यक्ति का बोध भी हो जाता है..तो यह भी ठीक नहीं कहा जा सकता क्योंकि जातिवादी के मत में जाति और व्यक्ति में भेद माना जाता है, किन्तु उक्तरीति से जाति और ध्यक्ति का संकीर्ण सोध मानने पर शम्द से शायमान जाति और व्यक्ति के अभेद का अंगीकृत भेद के साथ विरोध होने के कारण व्यक्ति से भिन्न वास्तव जाति का अभ्युपगम नहीं सिद्ध हो सकता ।
[बौद्ध मत में अपोह के विविध प्रकार] प्रश्न होता है कि यदि भ्रान्त तवृत्त्व यानी कल्पित गोत्व आदि शब्दषाच्य है तो अपोह को शब्दार्थ कहना कैसे सङ्गत हो सकता है ? व्याख्याकार ने यौद्धों की ओर से इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि बौद्ध मत में अपोह के दो भेद हैं, पर्युदास-प्रतिषेध और प्रसज्यप्रतिषेध । इन में प्रथम के दो भेद हैं, अर्थ में अनुगत एकरूप से भासमान धर्म-जो बुद्धि का साकार होने से श्रुद्धिरुप है, तथा अन्यव्यावृत्त स्वलक्षणभूत अर्थ । इन में पहला विजातीय वस्तु की प्राप्ति का हेतु होने से अपोह शब्द का गौण अर्थ है । पर्युदास रूप अपोह के प्रथम भेद को स्पष्ट करते हुए व्याख्याकार ने कहा है कि जैसे हरीतकी आदि अनेक औषध एक सामान्य धर्म द्वारा अनुगतीकत (अनषिद्ध) न होने पर भी ज्वरनिवृत्तिरूप एक कार्य का सम्पादन करते हैं उसी प्रकार चित्र, धवल, श्यामल आदि गो रूप मर्थ परस्पर भिन्न तथा किसी प्रामाणिक पक अनुगत रूप वाले न होते हुए भी गोत्यादि पफाकार प्रतीति को उत्पन्न करते