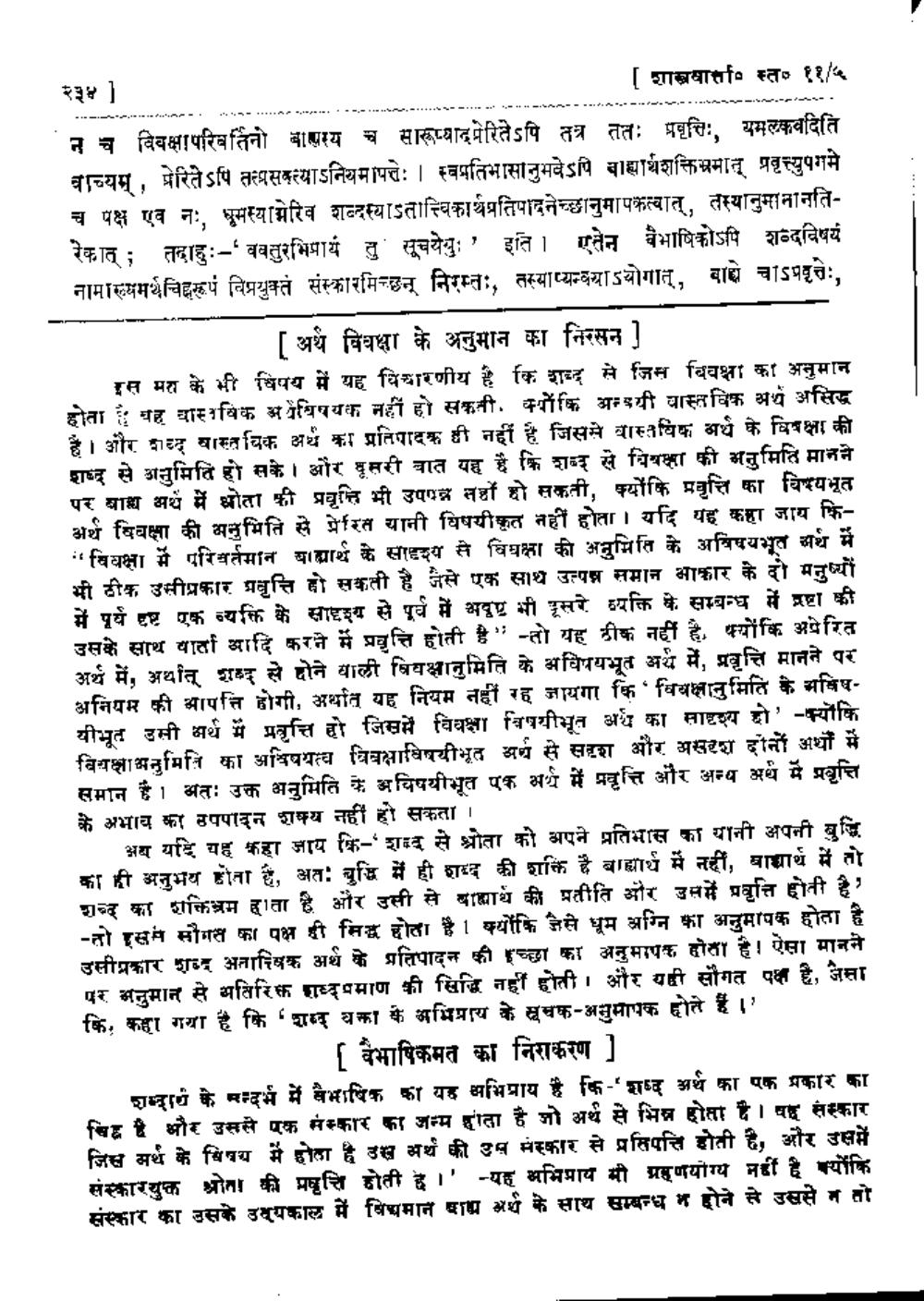________________
२३५ ]
[ शास्रवार्ताः स्त० ११/५ न च विवक्षापरिवर्तिनी बापस्य च सारूप्यादप्रेरितेऽपि तत्र ततः प्रवृत्तिः, यमलकवदिति वाच्यम् , प्रेरितेऽपि तत्प्रसक्त्याऽनियमापत्तेः । स्वप्रतिभासानुमवेऽपि बाह्याथशक्तिभ्रमात् प्रवृत्त्युपगमे च पक्ष एव नः, धूमस्याग्नेरिव शब्दस्याऽतात्त्विकार्थप्रतिपादनेच्छानुमापकत्वात्, तस्यानुमानानतिरेकात् ; तदाहु:-' ववतुरभिप्रायं तु सूचयेयुः' इति । एतेन वैभाषिकोऽपि शब्दविषय नामारूयमर्थचिहरूपं विप्रयुक्तं संस्कारमिच्छन् निरम्तः, तस्याप्यन्वयाऽयोगात्, वाद्ये चाऽप्रवृत्तेः,
[ अर्थ विवक्षा के अनुमान का निरसन ] इस मरा के भी विषय में यह विचारणीय है कि शब्द से जिम विवक्षा का अनुमान होता वह वास्तविक विषयक नहीं हो सकती. क्योंकि अन्यी पास्तविक अर्थ असिद्ध है। और शब्द वास्तविक अर्थ का प्रतिपादक ही नहीं है जिससे वास्तविक अर्थ के विषक्षा की शब्द से अनुमिति हो सके। और वृसरी बात यह है कि शब्द से विवक्षा की भनुमिति मानने पर बाच अर्थ में श्रोता की प्रवृत्ति भी उपपन्न नही हो सकती, क्योंकि प्रवृत्ति का विश्यभूत अर्थ विवक्षा की अनुमिति से प्रेरित यानी विषयीकृत नहीं होता। यदि यह कहा जाय कि"विवक्षा में परिवर्तमान याद्वार्थ के सादृश्य से विषक्षा की अनुमिति के अविषयभूत अर्थ में भी ठीक उसीप्रकार प्रवृत्ति हो सकती है जैसे एक साथ उत्पन्न समान आकार के दो मनुष्यों में पूर्य दृष्ट एक व्यक्ति के सादृश्य से पूर्व में अवृष्ट भी दूसरे व्यक्ति के सम्बन्ध में द्रष्टा की उसके साथ वार्ता आदि करने में प्रवृत्ति होती है" -तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि अप्रेरित अर्थ में, अर्थात् शब्द से होने वाली विवक्षानुमिति के अविषयभूत अर्थ में, प्रवृत्ति मानने पर अनियम की आपत्ति होगी, अर्थात यह नियम नहीं रह जायगा कि वियक्षानुमिति के अविषयीभूत उसी अर्थ में प्रवृत्ति हो जिसमें विवक्षा विषयीभूत अर्थ का साष्टश्य हो' -क्योंकि विद्यक्षाअनुमिति का अविषयत्व विवक्षाविषयीभूत अर्थ से सत्श और असरश दोनों अर्थों में समान है। अतः उक्त अनुमिति के अविषयीभूत पक अर्थ में प्रवृत्ति और अन्य अर्थ में प्रवृत्ति के अभाव का उपपादन शक्य नहीं हो सकता।
अब यदि यह कहा जाय कि-' शब्द से श्रोता को अपने प्रतिभास का यानी अपनी बुद्धि काही अनुभव होता है, अत: बुद्धि में ही शब्द की शक्ति है बाह्यार्थ में नहीं, बाधार्थ में तो शब्द का शक्तिभ्रम हाता है और उसी से बाह्यार्थ की प्रतीति और उसमें प्रवृत्ति होती है। -तो इसमें मौगत का पक्ष ही सिद्ध होता है। क्योंकि जैसे धूम अग्नि का अनुमापक होता है उसीप्रकार शब्द अतात्त्विक अर्थ के प्रतिपादन की इच्छा का अनुमापक होता है। ऐसा मानने पर अनुमान से अतिरिक्त शब्दप्रमाण की सिद्धि नहीं होती। और यही सौगत पक्ष है, जैसा कि, कहा गया है कि 'शब्द धक्का के अभिप्राय के सूचक-अनुमापक होते हैं।'
1 [वैभाषिकमत का निराकरण ] शम्दार्थ के सन्दर्भ में वैभाषिक का यह अभिप्राय है कि-'शब्द अर्थ का पक प्रकार का चित है और उससे एक मस्कार का जन्म होता है जो अर्थ से भिन्न होता है। वह संस्कार जिस मर्थ के विषय में होता है उस अर्थ की उस मस्कार से प्रसिपत्ति होती है, और उसमें संस्कारयुक्त श्रोता की प्रवृत्ति होती है।' -यह अभिप्राय मी ग्रहणयोग्य नहीं है क्योंकि संस्कार का उसके उश्यकाल में विद्यमान पान अर्थ के साथ सम्बन्ध होने से उससे न तो