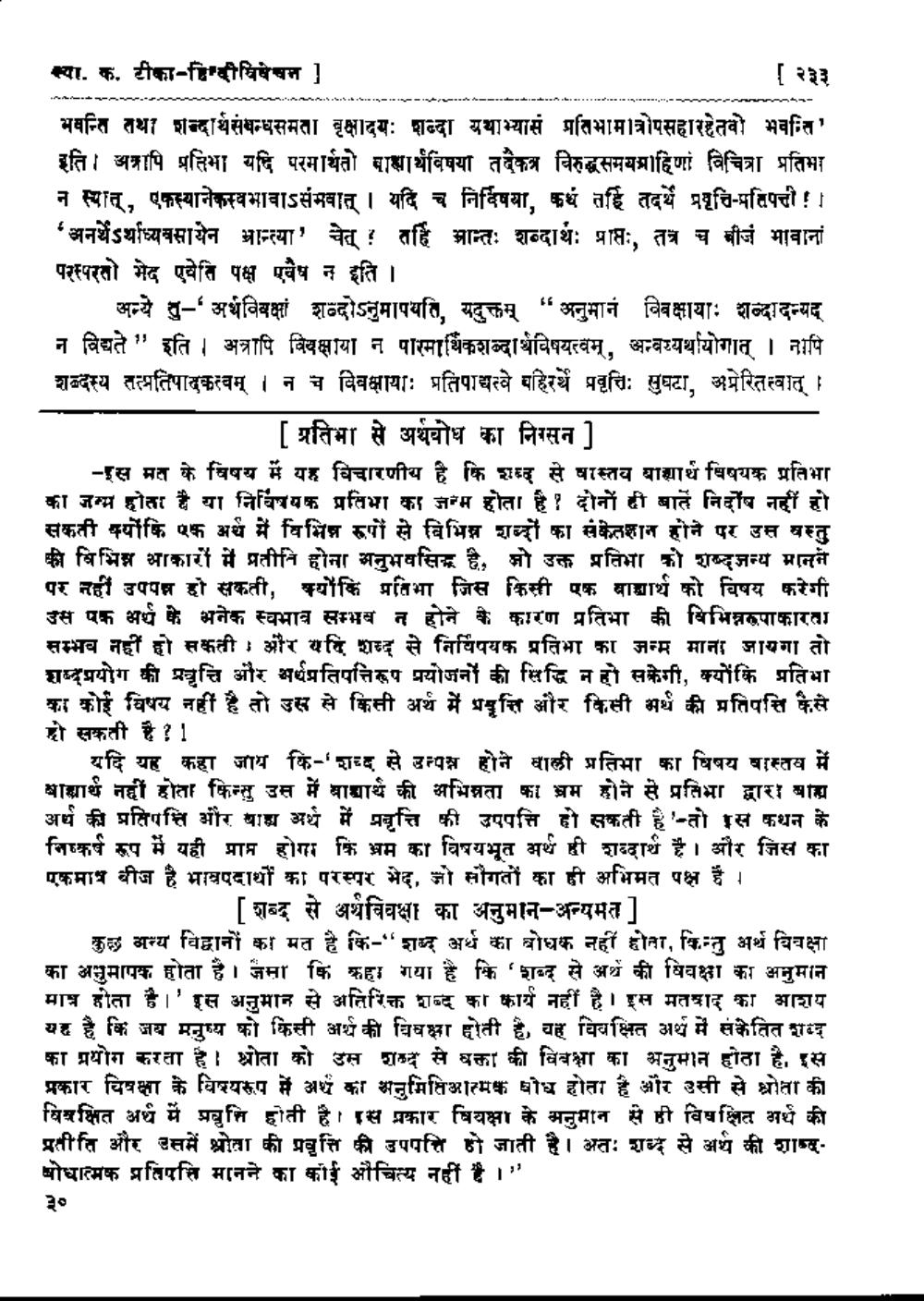________________
[ २३३
स्था. क. टीका-हिन्दीविषेचन ] भवन्ति तथा शब्दार्थसंबन्धसमता वृक्षादयः शन्दा यथाभ्यासं प्रतिभामात्रोपसहारहेतवो भवन्ति' इति। अत्रापि प्रतिभा यदि परमार्थतो पामार्थविषया तदैका विरुद्धसमयग्राहिणां विचित्रा प्रतिमा न स्यात्, एफस्यानेकस्वभावाऽसंमवात् । यदि च निर्दिषया, कथं तईि तदर्थे प्रवृत्ति-प्रतिपत्ती! । 'अनर्थेऽर्थाध्यवसायेन प्रान्त्या' चेत् ! तर्हि आन्तः शब्दार्थः प्राप्तः, तत्र च बीजं भावानां परस्परतो भेद एवेति पक्ष एवैध न इति ।
अन्ये तु- अर्थविवक्षां शब्दोऽनुमापयति, यदुक्तम् “ अनुमानं विवक्षायाः शब्दादन्यद् न विद्यते " इति । अत्रापि विवझाया न पारमार्थिक शब्दार्थविषयत्वम् , अन्वयर्थायोगात् । नापि शब्दस्य तत्प्रतिपादकत्वम् । न च विवक्षायाः प्रतिपाद्यत्वे पहिरर्थे प्रवृत्तिः सुघटा, अमेरितत्वात् ।
[प्रतिभा से अर्थबोध का निरसन ] -इस मत के विषय में यह विचारणीय है कि शब्द से वास्तव बायार्थ विषयक प्रतिभा का जन्म होता है या निविषयक प्रतिभा का जन्म होता है। दोनों ही बातें निदोष नहीं हो सकती क्योंकि एक अर्थ में विभिन्न रूपों से विभिन्न शब्दों का संकेतशान होने पर उस वस्तु की विभिन्न आकारों में प्रतीति होना अनुभवसिद्ध है, जो उक्त प्रतिभा को शब्दजन्य मानने पर नहीं उपपन्न हो सकती, क्योंकि प्रतिभा जिस किसी एक बाचार्थ को विषय करेगी उस पक अर्थ के अनेक स्वभाव सम्भव न होने के कारण प्रतिभा की विभिन्नरूपाकारता सम्भव नहीं हो सकती। और यदि शब्द से निर्विषयक प्रतिभा का जन्म माना जायगा तो शब्दप्रयोग की प्रवृत्ति और अर्थप्रतिपत्तिरूप प्रयोजनों की सिद्धि न हो सकेगी, क्योंकि प्रतिभा का कोई विषय नहीं है तो उस से किसी अर्थ में प्रकृति और किसी अर्थ की प्रतिपत्ति कैसे हो सकती है?
यदि यह कहा जाय कि-शब्द से उत्पन्न होने वाली प्रतिभा का विषय वास्तव में बाशार्थ नहीं होता किन्तु उस में बाधार्थ की अभिन्नता का भ्रम होने से प्रतिभा द्वारा बाह्य अर्थ की प्रतिपत्ति और बाय अर्थ में प्रवृत्ति की उपपत्ति हो सकती है'-तो इस कथन के निष्कर्ष रूप में यही प्राम होगा कि भ्रम का विषयभूत अर्थ ही शब्दार्थ है। और जिस का एकमात्र बीज है भानपदार्थों का परस्पर भेद, जो सौगतों का ही अभिमत पक्ष हैं ।
[शब्द से अर्थविवक्षा का अनुमान-अन्यमत ] कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि-"शब्द अर्थ का बोधक नहीं होता, किन्तु अर्थ विवक्षा का अनुमापक होता है। जमा कि कहा गया है कि 'शब्द से अर्थ की विवक्षा का अनुमान मात्र होता है।' इस अनुमान से अतिरिक्त शब्द का कार्य नहीं है। इस मतवाद का आशय यह है कि जब मनुष्य को किसी अर्थ की विषक्षा होती है, वह विवक्षित अर्थ में संकेतित शब्द का प्रयोग करता है। श्रोता को उस शब्द से धक्ता की विवक्षा का अनुमान होता है, इस प्रकार विवक्षा के विषयरूप में अर्थ का अनुमितिआत्मक बोध होता है और उसी से श्रोता की विवक्षित अर्थ में प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार घियक्षा के अनुमान से ही विधक्षित अर्थ की प्रतीति और उसमें श्रोता की प्रवृत्ति की उपपत्ति हो जाती है। अतः शब्द से अर्थ की शाद. बोधात्मक प्रतिपत्ति मानने का कोई औचित्य नहीं है।"