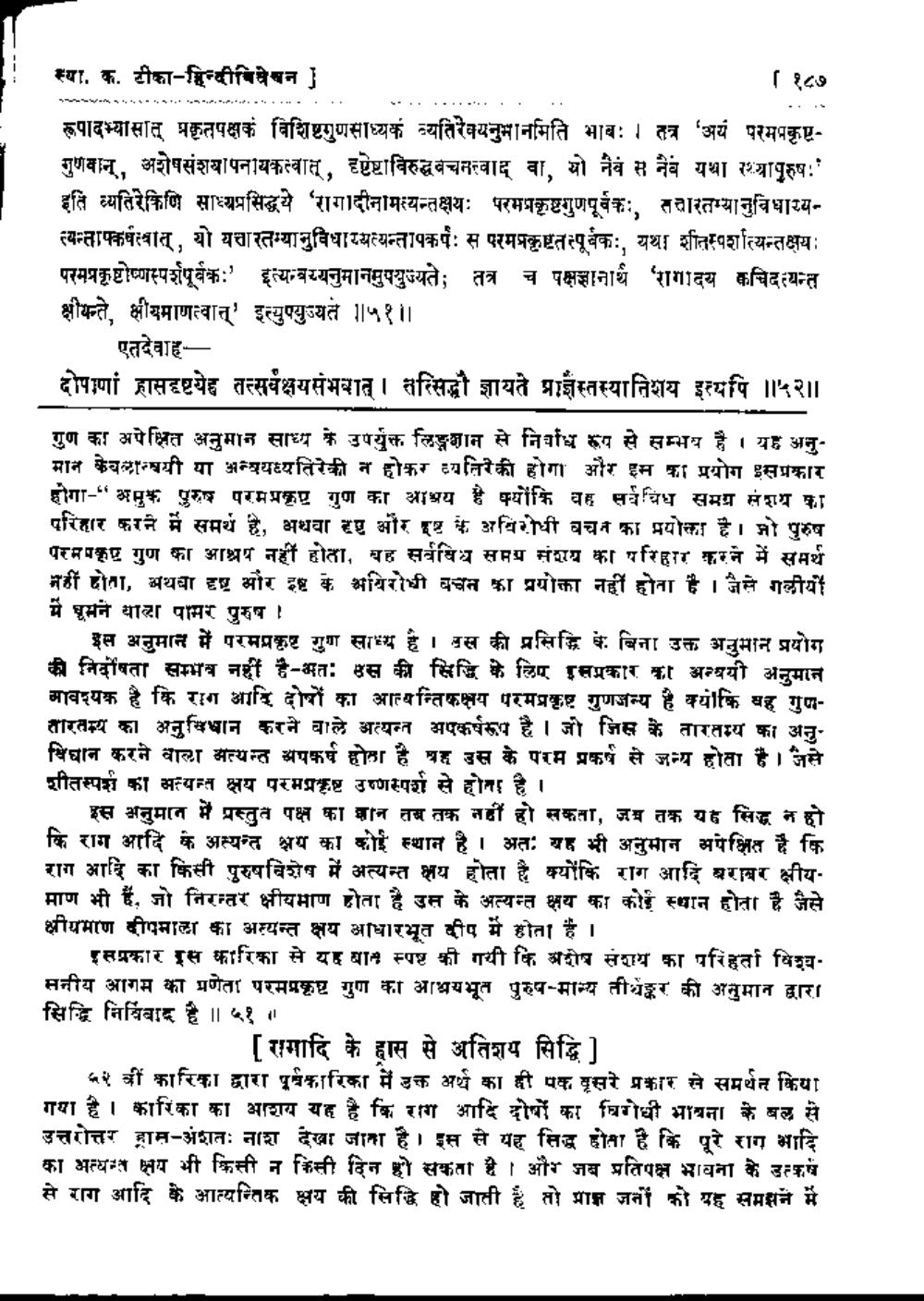________________
[ १८७
स्था. क. टीका-हिन्दीविवेचन ]
"
रूपादभ्यासात् प्रकृतपक्षकं विशिष्टगुणसाध्यकं व्यतिरेक्यनुभानमिति भावः । तत्र 'अयं परमप्रकृष्टगुणवान्, अशेषसंशयापनायकत्वात् दृष्टेष्टाविरुद्ध बचनत्वाद् वा, यो नैवं स नैवं यथा या पुरुषः इति व्यतिरेकिणि साध्यप्रसिद्धये ' रागादीनामत्यन्तक्षयः परमप्रकृष्टगुणपूर्वकः, सतारतम्यानुविधाय्यत्यन्तापकर्षत्वात्, यो यतारतम्यानुविधाय्यत्यन्तापकर्षः स परमप्रकृष्टतत्पूर्वकः, यथा शीतस्पर्शात्यन्तक्षयः परमप्रकृष्टोष्णस्पर्शपूर्वकः' इत्यन्वय्यनुमानमुपयुज्यते; तत्र च पक्षज्ञानार्थ 'रागादय कचिदत्यन्त श्रीयन्ते, श्रीयमाणत्वात्' इत्युपयुज्यते ॥ ५१ ॥
एतदेवाहदोपण हा
तत्सर्वक्षय संभवात् । तत्सिद्धौ ज्ञायते प्राज्ञस्तस्यातिशय इत्यपि ॥ ५२ ॥
गुण का अपेक्षित अनुमान साध्य के उपर्युक्त लिङ्गशान से निर्वाध रूप से सम्भव है । यह अनुमान केवलान्वयी या अन्ययध्यतिरेकी न होकर व्यतिरेकी होगा और इस का प्रयोग इसप्रकार होगा - " अमुक पुरुष परमप्रकृष्ट गुण का आश्रय है क्योंकि वह सर्वविध समग्र संशय का परिहार करने में समर्थ है, अथवा दृष्ट और इट के अविरोधी वचन का प्रयोक्ता है। जो पुरुष परमपकृष्ट गुण का आश्रम नहीं होता, वह सर्वविध समग्र संशय का परिहार करने में समर्थ नहीं होता, अथवा दृष्ट और इष्ट के अविरोधी वचन का प्रयोक्ता नहीं होता है । जैसे गलीयों में घूमने याला पामर पुरुष !
इस अनुमान में परमप्रकृष्ट गुण साध्य है । उस की प्रसिद्धि के बिना उक्त अनुमान प्रयोग की निर्दोषता सम्भव नहीं है अतः उस की सिद्धि के लिए इसप्रकार का अन्ययी अनुमान आवश्यक है कि राग आदि दोषों का आत्यन्तिकक्षय परमप्रकृष्ट गुणजन्य है क्योंकि वह गुणतारतम्य का अनुविधान करने वाले अत्यन्त अपकर्षरूप है । जो जिस के तारतम्य का अनुविधान करने वाला अत्यन्त अपकर्ष होता है वह उस के परम प्रकर्ष से जन्य होता है। जैसे शीतस्पर्श का अत्यन्त क्षय परमप्रकृष्ट उष्णस्पर्श से होता है ।
इस अनुमान भें प्रस्तुत पक्ष का ज्ञान तब तक नहीं हो सकता, जब तक यह सिद्ध न हो कि राग आदि के अत्यन्त क्षय का कोई स्थान है । अतः यह भी अनुमान अपेक्षित है कि राग आदि का किसी पुरुषविशेष में अत्यन्त क्षय होता है क्योंकि राग आदि बराबर क्षीयमाण भी है, जो निरन्तर क्षीयमाण होता है उस के अत्यन्त क्षय का कोई स्थान होता है जैसे श्रीयमाण दीपमाला का अत्यन्त क्षय आधारभूत दीप में होता है ।
इसप्रकार इस कारिका से यह बात स्पष्ट की गयी कि अशेष संशय का परिहर्ता विश्वसनीय आगम का प्रणेता परमप्रकृष्ट गुण का आश्रयभूत पुरुष मान्य तीर्थेङ्कर की अनुमान द्वारा सिद्धि निर्विवाद है ।। ५१ ।।
[ रामादि के द्वास से अतिशय सिद्धि ]
५२ वीं कारिका द्वारा पूर्वकारिका में उक्त अर्थ का ही एक दूसरे प्रकार से समर्थन किया गया है । कारिका का आशय यह है कि राग आदि दोषों का विरोधी भावना के बल से उत्तरोत्तर हाम - अंशतः नाश देखा जाता है। इस से यह सिद्ध होता है कि पूरे राग भादि का अत्यन्त क्षय भी किसी न किसी दिन हो सकता है। और जब प्रतिपक्ष भावना के उत्कर्ष से राग आदि के आत्यन्तिक क्षय की सिद्धि हो जाती है तो प्राप्त जनों को यह समझने में