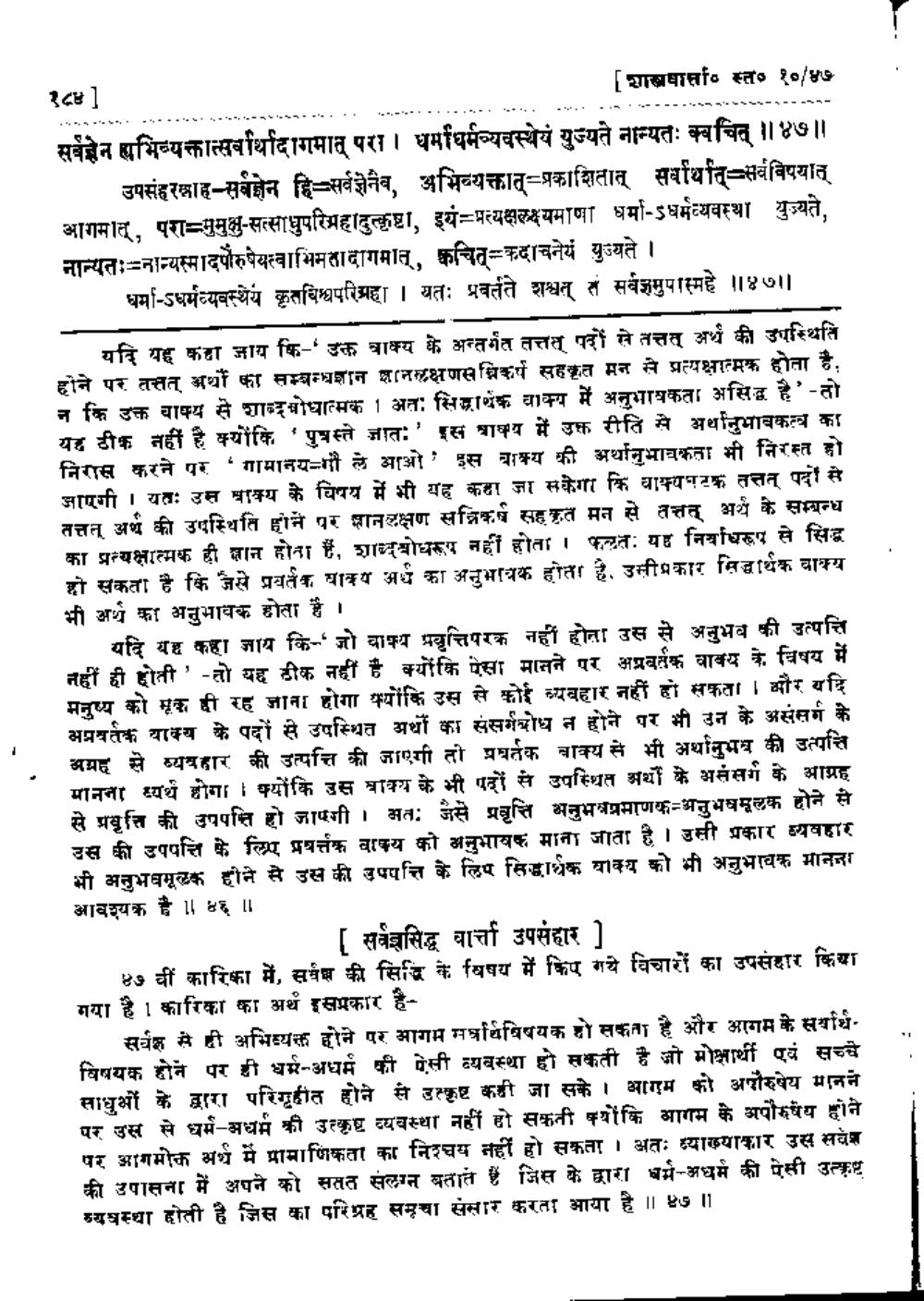________________
१८४]
[शास्त्रपा० स्त० १०/४७ सर्वज्ञेन यभिव्यक्तात्सर्वार्थादागमात् पस। धर्माधर्मव्यवस्थेयं युज्यते नान्यतः क्वचित् ॥४७॥
उपसंहरनाह-सर्वज्ञेन हि-सर्वज्ञेनैव, अभिव्यक्तात्-प्रकाशितात् सर्वार्थात् सर्वविषयात् आगमात् , परा=मुमुक्षु-सत्साधुपरिग्रहादुत्कृष्टा, इयं प्रत्यक्षलक्ष्यमाणा धर्मा-ऽधर्मव्यवस्था युज्यते, नान्यतः नान्यस्मादपौरुषेयत्वाभिमतादागमात्, कचित् कदाचनेयं युज्यते ।
धर्मा-ऽधर्मव्यवस्थेय कृतविश्वपरिग्रहा । यतः प्रवर्तते शश्वत् त सर्वज्ञमुपास्महे ॥४७॥
___ यदि यह कहा जाय कि-'उक्त वाक्य के अन्तर्गत तत्तत् पदों से तत्तत् अर्थ की उपस्थिति होने पर तत्तत् अर्थों का सम्बन्धज्ञान ज्ञानमक्षणसन्निकर्ष सहकृत मन से प्रत्यक्षात्मक होता है, न कि उक्त वाक्य से शाब्दबोधात्मक 1 अत: सिद्धार्थक वाक्य में अनुभाषकता असिद्ध है' -तो यह ठीक नहीं है क्योंकि 'पुत्रस्ते जातः' इस वाक्य में उक्त रीति से अर्थानुभावकत्व का निरास करने पर 'गामानय-गौ ले आओ' इस बाश्य की अर्थानुभावकता भी निरस्त हो जाएगी । यतः उस वाक्य के विषय में भी यह कहा जा सकेगा कि चास्यपटक तत्तत् पदों से तत्तत् अर्थ की उपस्थिति होने पर ज्ञानलक्षण सन्निकर्ष सह कृत मन से तत्तत् अर्थ के सम्बन्ध का प्रत्यक्षात्मक ही ज्ञान होता है, शाब्दबोधरूप नहीं होता । फलतः यह निर्वाधरूप से सिद्ध हो सकता है कि जैसे प्रवर्तक वाक्य अर्ध का अनुभात्रक होता है. उसीप्रकार सिद्धार्थक वाक्य भी अर्थ का अनुभावक होता है ।
यदि यह कहा जाय कि- जो वाक्य प्रवृत्तिपरक नहीं होता उस से अनुभव की उत्पत्ति नहीं ही होती' -तो यह ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर अप्रवर्तक वाक्य के विषय में मनुष्य को मृक ही रह जाना होगा क्योंकि उस से कोई व्यवहार नहीं हो सकता । और यदि अप्रवर्तक याक्य के पदों से उपस्थित अर्थों का संसर्गबोध न होने पर भी उन के असंसर्ग के अग्रह से व्यवहार की उत्पत्ति की जाएगी तो प्रवर्तक वाक्य से भी अर्थानुभव की उत्पत्ति मानना व्यर्थ होगा । क्योंकि उस वाक्य के भी पदों से उपस्थित अर्थों के असंसर्ग के आग्रह से प्रवृत्ति की उपपत्ति हो जाएगी। अत: जैसे प्रवृत्ति अनुभवप्रमाणक-अनुभषमूलक होने से उस की उपपत्ति के लिए प्रवर्तक वाक्य को अनुभायक माना जाता है। उसी प्रकार व्यवहार भी अनुभवमूलक होने से उस की उपपत्ति के लिए सिद्धार्थक याक्य को भी अनुभावक मानना आवश्यक है ।। ४६ ।।
[ सर्वज्ञसिद्ध वार्ता उपसंहार ] ४७ वीं कारिका में, सर्वश की सिद्धि के विषय में किए गये विचारों का उपसंहार किया गया है 1 कारिका का अथं इसप्रकार है
सर्व से ही अभिव्यक्त होने पर आगम मार्थविषयक हो सकता है और आगम के साथविषयक होने पर ही धर्म-अधर्म की ऐसी व्यवस्था हो सकती है जो मोक्षार्थी एवं सच्चे। साधुओं के द्वारा परिगृहीत होने से उस्कृष्ट कही जा सके। आगम को अपौरुषेय मानने पर उस से धर्म-अधर्म की उत्कृष्ट व्यवस्था नहीं हो सकती क्योंकि आगम के अपौरुषेय होने पर आगमोक अर्थ में प्रामाणिकता का निश्चय नहीं हो सकता । अतः ध्याख्याकार उस सर्वज्ञ की उपासना में अपने को सतत संलग्न बताते हैं जिस के द्वारा धर्म-अधर्म की ऐसी उत्कृष्ट व्यवस्था होती है जिस का परिग्रह समृचा संसार करता आया है ।। ५७ ।।