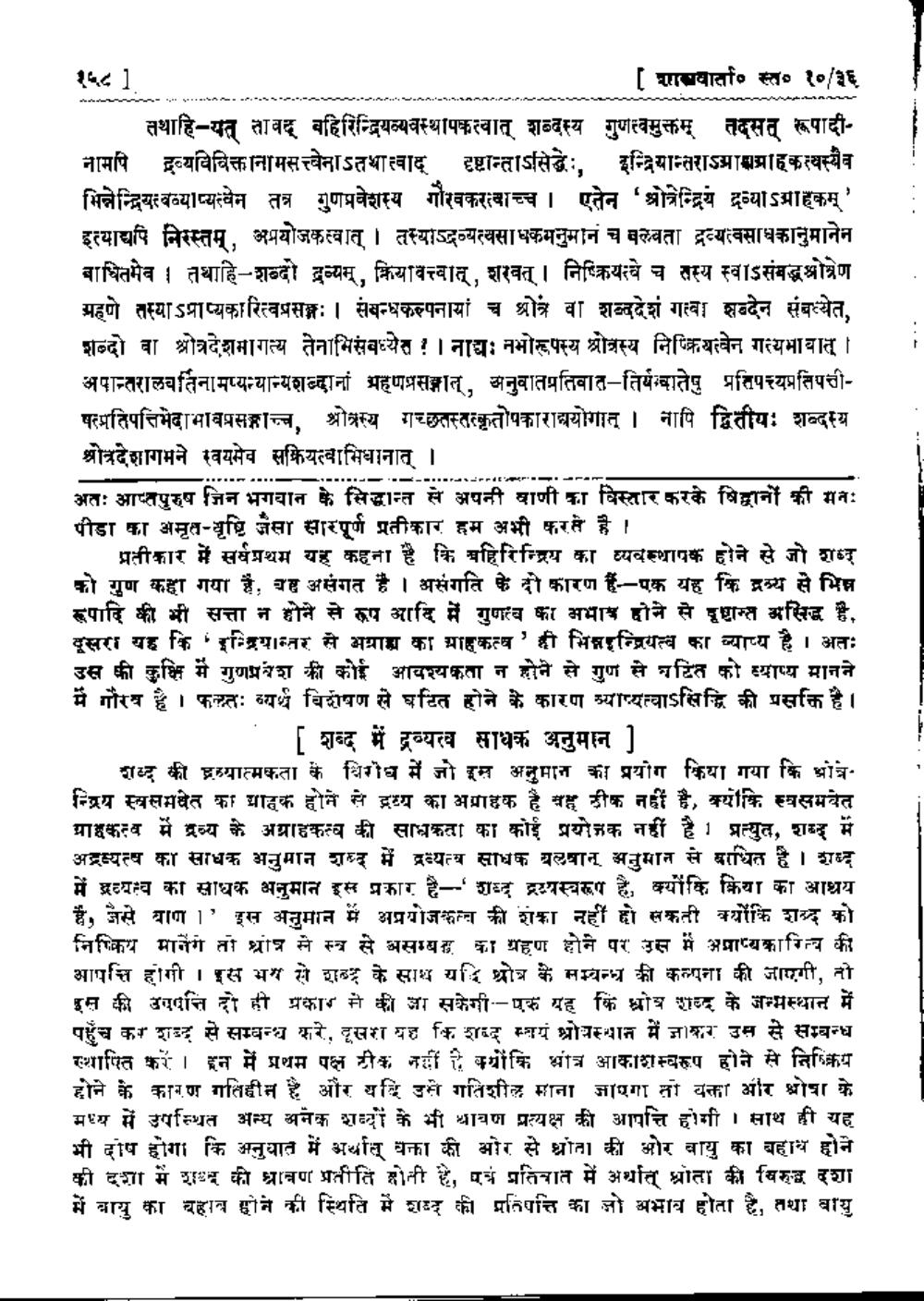________________
r
er--
रुपा
१५८1
[शासवार्ता० स्त० १०/३६ ___ तथाहि-यत् तावद् बहिरिन्द्रियव्यवस्थापकत्वात् शब्दस्य गुणत्वमुक्तम् तदसत् रूपादीनामपि द्रव्यविविक्तानामसत्त्वेनाऽतथात्वाद् दृष्टान्ताऽसिद्धेः, इन्द्रियान्तराऽग्रामग्राहकत्यस्यैव भिन्नेन्द्रियस्वव्याप्यत्वेन तत्र गुणप्रवेशस्य गौरवकरत्वाच्च । एतेन 'श्रोत्रेन्द्रिय द्रव्याऽग्राहकम्' इत्याद्यपि निरस्तम् , अभयोजकत्वात् । तस्याऽदव्यत्वसाधकमनुमानं च बलवता द्रव्यत्वसाधकानुमानेन बाधितमेव । तथाहि-शब्दो द्रव्यम् , कियावत्त्वात् , शरवत् । निष्क्रियत्वे च तस्य स्वाऽसंबद्धश्रोत्रेण ग्रहणे तस्याऽप्राप्यकारित्वप्रसङ्गः । संबन्धकल्पनायां च श्रोत्रं वा शब्ददेशं गत्वा शब्देन संबध्येत, शब्दो वा श्रोत्रदेशमागत्य तेनामिसंबध्येत ! । नायः नभोरूपस्य श्रोत्रस्य निष्क्रियत्वेन गत्यभावात् । अपान्तरालयतिनामप्यन्यान्यशब्दानां ग्रहणप्रसङ्गात्, अनुवातप्रतिवात-तिर्यग्वातेषु प्रतिपत्त्यप्रतिपत्तीषत्प्रतिपत्तिभेदाभावप्रसाच्च, श्रोत्रस्य गच्छतस्तत्कृतोपकाराग्रयोगात् । नापि द्वितीयः शब्दस्य श्रोत्रदेशागमने स्वयमेव सक्रियत्वामिधानात् । अतः आप्तपुरुष जिन भगवान के सिद्धान्त से अपनी वाणी का विस्तार करके षिद्वानों की मनः पीडा का अमृत-वृष्टि जैसा सारपूर्ण प्रतीकार हम अभी करते है।
प्रतीकार में सर्वप्रथम यह कहना है कि बहिरिन्द्रिय का व्यवस्थापक होने से जो शब्द को गुण कहा गया है, वह असंगत है। असंगति के दो कारण हैं-पक यह कि द्रव्य
सत्ता न होने से रूप आदि में गणत्व का अभाव होने से इधान्त सिद्ध दसरा यह किरन्द्रियान्तर से अग्राह्य का ग्राहकत्व'ही भिन्नन्त्रियत्व का व्याप्य है। अतः उस की कुक्षि में गुणप्रवेश की कोई आवश्यकता न होने से गुण से पटित को ध्याप्य मानने में गौरव है । फलतः व्यर्थ विशेषण से घटित होने के कारण व्याप्यत्वाऽसिद्धि की प्रसक्ति है।
[ शब्द में द्रव्यत्व साधक अनुमान ] शब्द की दृठ्यात्मकता के विरोध में जो इस अनुमान का प्रयोग किया गया कि श्रोत्रन्द्रिय स्वसमवेत का ग्राहक होने से द्रव्य का अग्राहक है वह ठीक नहीं है, क्योंकि स्वसमवेत ग्राहकत्व में द्रव्य के अनाहकत्व की साधकता का कोई प्रयोजक नहीं है 1 प्रत्युत, शब्द में अद्रष्यत्व का साधक अनुमान शब्द में द्रव्यत्य साधक बलवान् अनुमान से बाधित है । शब्द में व्यत्व का साधक अनुमान इस प्रकार है-' शब्द द्रव्यस्वरूप है, क्योंकि क्रिया का आश्रय जसे बाण ।' इस अनमान में अप्रयोजन की शंका नहीं हो सकती क्योंकि शरद को
य मानेंगे तो श्रांत्र से स्त्र से असम्बद्ध का ग्रहण होने पर उस में अप्राप्यकारिन्व की आपत्ति होगी । इस भय से शब्द के साथ यदि श्रोत्र के मम्बन्ध की कल्पना की जाएगी, नो इस की उपपत्ति दो ही प्रकार में की जा सकेगी--एक यह कि श्रोत्र शब्द के जन्मस्थान में पहुँच कर शब्द से सम्बन्ध सरे, दूसरा यह कि शब्द म्यं श्रोत्रस्थान में जाकर उस से सम्बन्ध स्थापित करें। इन में प्रथम पक्ष ठीक नहीं है क्योंकि श्रीत्र आकाशस्वरूप होने से निष्क्रिय होने के कारण गतिहीन है और यदि उसे गतिशील माना जाएगा तो वक्ता और श्रोत्रा के मध्य में उपस्थित अन्य अनेक शब्दों के भी थायण प्रत्यक्ष की आपत्ति होगी। साथ ही यह भी दोष होगा कि अनुपात में अर्थात् वक्ता की ओर से श्रोता की ओर वायु का बहाव होने की दशा में शब्द की प्रावण प्रीति होती है, पत्र प्रतिवात में अर्थात् श्रोता की विरुद्ध दशा में बायु का बहाव होने की स्थिति में शब्द की प्रतिपत्ति का जो अभाव होता है, तथा वायु