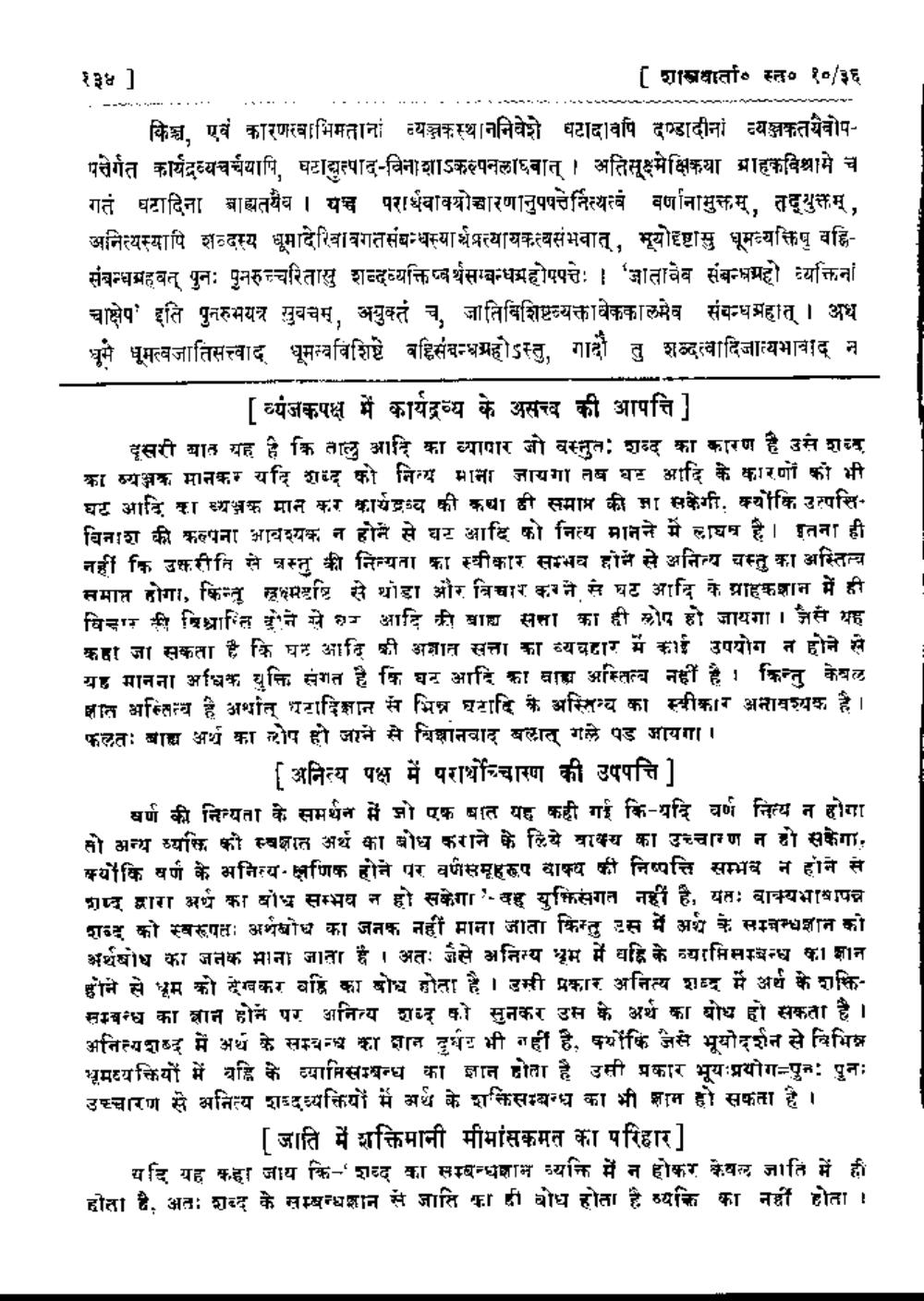________________
१३ ]
[शास्रधार्ताः स्त० १०/३६
किश्च, एवं कारणस्वाभिमतानां व्यञ्जकस्थाननिवेशे घटादावपि दण्डादीनां व्यञ्जकतयैवोपपत्तेर्गत कार्यद्रव्यचर्चयापि, घटाद्युत्पाद-विनाशाऽकल्पनलाघ्वान् । अतिसूक्ष्मेक्षिकया ग्राहकविश्रामे च गतं घटादिना ब्राह्यतयैव । यच्च परार्थवाक्योच्चारणानुपपत्तेनिस्यत्वं वर्णानामुक्तम् , तयुक्तम् , अनित्यस्यापि शब्दस्य धूमादेरिवावगतसंबन्धस्यार्थप्रत्यायकत्वसंभवात् , भूयोदृष्टासु धूमन्यक्तिषु वतिसंबन्धग्रहवत् पुनः पुनरुच्चरितासु शब्दव्यक्ति प्वर्थसम्बन्धमहोपपत्तेः । 'जातावेव संबन्धग्रहो व्यक्तिनां चाक्षेप' इति पुनरुभयन्त्र सुवचम् , अयुक्तं च, जातिविशिष्टव्यक्तावेककालमेव संबन्ध महात् । अध धूमे धूमत्वजातिसत्त्वाद धूमन्वविशिष्टे वहिसंबन्धग्रहोऽस्तु, गादी तु शब्दत्वादिजात्यभावाद् न
[व्यंजकपक्ष में कार्यद्रव्य के असव की आपत्ति] दूसरी बात यह है कि तालु आदि का व्यापार जो वस्तुत: शब्द का कारण है उसे शब्द का व्यञ्जक मानकर यदि शब्द को नित्य माना जायगा तब घट आदि के कारणों को भी घट आदि का व्याक मान कर कार्य द्रव्य की कथा ही समान की मा सकेगी. क्योंकि उत्पतिविनाश की कल्पना आवश्यक न होने से घर आदि को नित्य मानने में लायन है। इतना ही नहीं कि उत्तरीति से प्रस्तु की निन्यता का स्वीकार सम्भव होने से अनित्य वस्तु का अस्तित्व समाप्त होगा, किन्तु सूक्ष्मष्टि से थोड़ा और विचार करने से घट आदि के ग्राहकशान में ही विचार की विश्रान्ति देने से कर आदि की बाय सत्ता का ही लोप हो जायगा । जैसे यह कहा जा सकता है कि घट आदि की अज्ञात सत्ता का व्यवहार में काई उपयोग न होने से यह मानना अधिक युक्तिः संगत है कि घट आदि का वा अस्तित्व नहीं है। किन्तु केवल ज्ञात अस्तित्व है अर्थात् घटादिज्ञान से भिन्न घटादि के अस्तिन्य का स्वीकार अनावश्यक है। फलतः बाह्य अर्थ का टोप हो जाने से विज्ञानवाद बलात् गले पड़ जायगा ।
अनित्य पक्ष में परार्थोच्चारण की उपपत्ति ] वर्ण की निन्यता के समर्थन में जो एक बात यह कही गई कि-यदि वर्ण नित्य न होगा तो अन्य व्यक्ति को स्वस्त अर्थ का बोध कराने के लिये वाक्य का उच्चारण नहोस क्योकि वर्ण के भनित्य क्षणिक होने पर वर्णसमूहरूप वाक्य की निष्पत्ति सम्भव न होने से गद द्वारा अर्थ का बोध सम्भव न हो सकेगा'वह युक्तिसंगत नहीं है, यतः वाक्यभावापन्न शब्द को स्वरूपतः अर्थबोध का जनक नहीं माना जाता किन्तु उस में अर्थ के सम्बन्धज्ञान को अर्थबोध का जनक माना जाता है । अतः जैसे अनिन्य शृम में वहि के व्याप्तिसम्बन्ध का ज्ञान होने से धूम को देवकर वद्धि का बोध होता है। उसी प्रकार अनित्य शब्द में अर्थ के शक्ति
बन्ध का वान होने पर अनित्य शब्द को सुनकर उस के अर्थ का बोध हो सकता है। नित्य शब्द में अर्थ के सम्बन्ध का ज्ञान दृघर भी नहीं है, क्योंकि जसे भूयोदर्शन से विभिन्न धृमध्यक्तियों में बाढ़ के व्यामिसम्बन्ध का ज्ञान होता है उसी प्रकार भूयःप्रयोग-पुन: पुनः उच्चारण से अनित्य शब्दभ्यक्तियों में अर्थ के शक्तिसम्बन्ध का भी शाम हो सकता है।
[जाति में शक्तिमानी मीमांसकमत का परिहार] यदि यह कहा जाय कि-' शब्द का सम्बन्धशाम व्यक्ति में न होकर केवल जाति में ही होता है, अतः शब्द के सम्बन्ध ज्ञान से जाति का ही बोध होता है व्यकि का नहीं होता ।