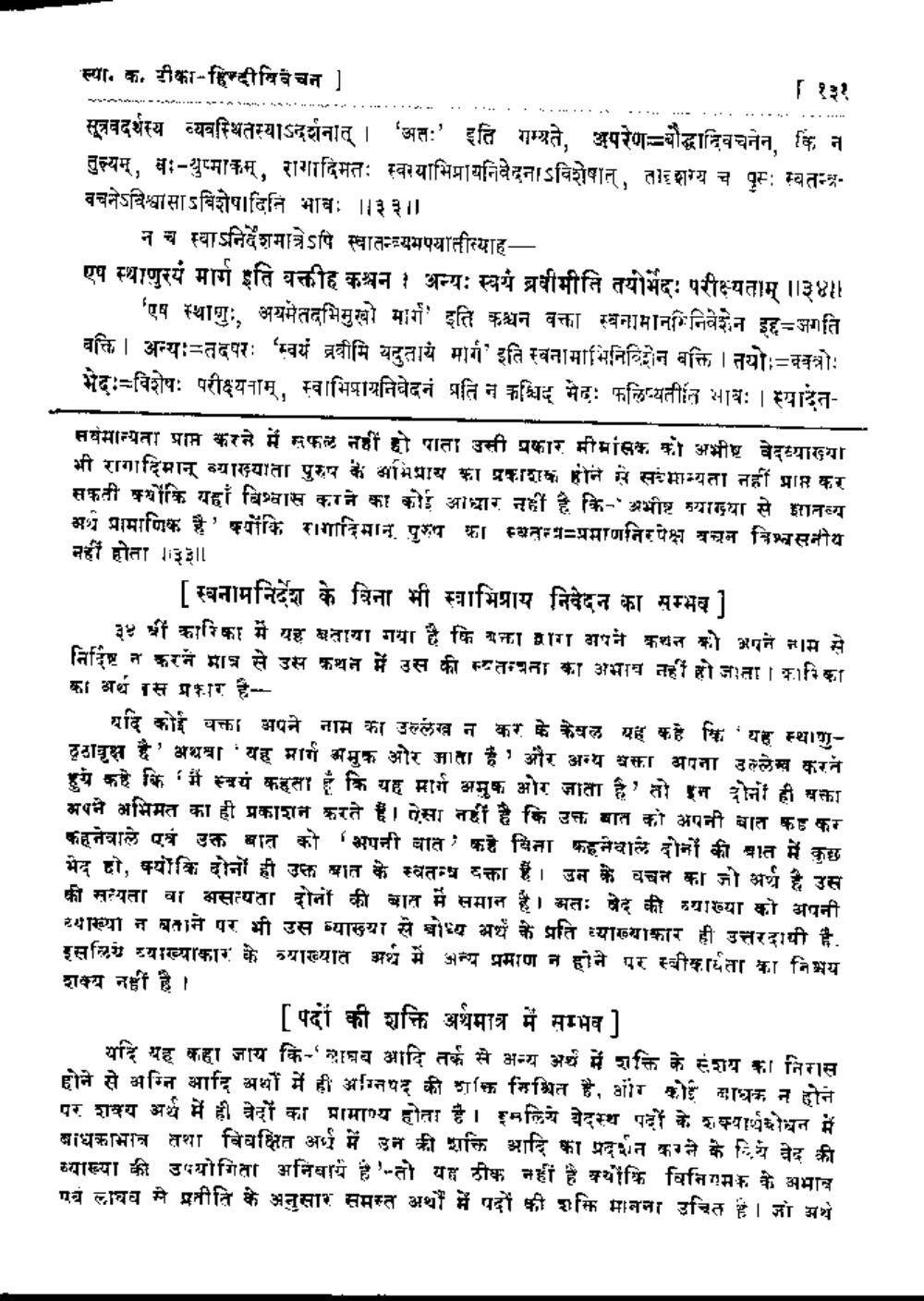________________
स्या. क. दीका-हिन्दीविवेचन ] सूत्रवदर्थस्य व्यवस्थितस्याऽदर्शनात् । 'अतः' इति गम्यते, अपरेण चौद्धादिवचनेन, कि न तुल्यम् , वा-युप्माकम् , रागादिमतः स्वरयाभिमायनिवेदनाऽविशेषात् , ताराग्य च पुर: स्वतन्त्रवचनेऽविश्वासाऽविशेषादिति भावः ।।३३।।
न च स्वाऽनिर्देशमात्रेऽपि स्वातन्त्र्यमण्यातीत्याहएप स्थाणुस्यं मार्ग इति वक्तीह कथन । अन्यः स्वयं ब्रवीमीति तयोर्भदः परीक्ष्यताम् ।।३४॥
'एष स्थाणुः, अयमेतदभिमुखो मार्ग' इति कश्चन वक्ता स्वनामाना निवेशेन इद्द-जगति वक्ति । अन्य तदपरः ‘स्वयं ब्रवीमि यदुताय मार्ग' इति स्वनामाभिनिविदोन बक्ति । तयोः कत्रोः भेदः-विशेषः परीक्ष्यताम् , स्वाभिप्रायनिवेदनं प्रति न कश्चिद् मेढ़ः फलिप्यतीत सावः । स्यादत
सर्वमान्यता प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाता उसी प्रकार मीमांसक को अभीष्ट वेदव्याख्या भी रागादिमान् व्याख्याता पुरुष के अभिप्राय का प्रकाशक होने से सामान्यता नहीं प्रार कर सकती क्योंकि यहाँ विश्वास करने का कोई आधार नहीं है कि-'अभीष्ट च्याख्या से ज्ञातव्य अर्थ प्रामाणिक है' क्योंकि रागादिमान पुरुष का स्वतन्त्र प्रमाणनिरपेक्ष वचन विश्वसनीय नहीं होता ।३३।।
[ स्वनामनिर्देश के बिना भी स्वाभिप्राय निवेदन का सम्भव ] ३४ / कारिका में यह बताया गया है कि गला नाग अपने कश्चन को अपने नाम से निर्दिष्ट न करने मात्र से उस कथन में उस की यतात्रता का अभाव नहीं हो जाता। कारिका का अर्थ इस प्रकार है---
यदि कोई वक्ता अपने नाम का उल्लेख न कर के केवल यह कहे कि यह स्थाणुढावृक्ष है' अथवा 'यह मार्ग अमुक ओर जाता है। और अन्य वक्ता अपना उल्लेख करते हुये कहे कि ' मैं स्वयं कहता है कि यह मार्ग अमुक ओर जाता है तो इन दोनों ही वक्ता अपने अभिमत का ही प्रकाशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि उक्त बात को अपनी बात कह कर कहनेवाले एवं उक्त बात को अपनी बात' कहे विना कहनेवाले दोनों की बात में कुछ भेद हो, क्योंकि दोनों ही उक्त बात के स्वतन्ध वक्ता हैं। उन के वचन का जो अर्थ है उस की सत्यता वा असत्यता दोनों की बात में समान है। अतः वेद की व्याख्या को अपनी स्याख्या न बताने पर भी उस व्याख्या से बोध्य अर्थ के प्रति व्याख्याकार ही उत्तरदायी है. इसलिये व्याख्याकार के व्याख्यात अर्थ में अन्य प्रमाण न होने पर स्वीकार्यता का निभय शक्य नहीं है।
[पदों की शक्ति अर्थमात्र में सम्भव ] यदि यह कहा जाय कि-'साय आदि तर्क से अन्य अर्थ में शक्ति के संशय का निरास होने से अग्नि आदि अर्थों में ही अग्निपद की शक्ति मिश्चित है, और कोई माधक न होने पर शक्य अर्थ में ही वेदों का प्रामाण्य होता है। इमलिये बेदस्थ पदों के शपयार्थबोधन में बाधकामात्र तथा विवक्षित अर्थ में उन की शक्ति आदि का प्रदर्शन करने के लिये वेद की व्याख्या की उपयोगिता अनिवार्य है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि विनिमक के अभाव एवं लायव मे प्रतीति के अनुसार समस्त अर्थों में पदों की शसि मानना उचित है । जो अर्थ