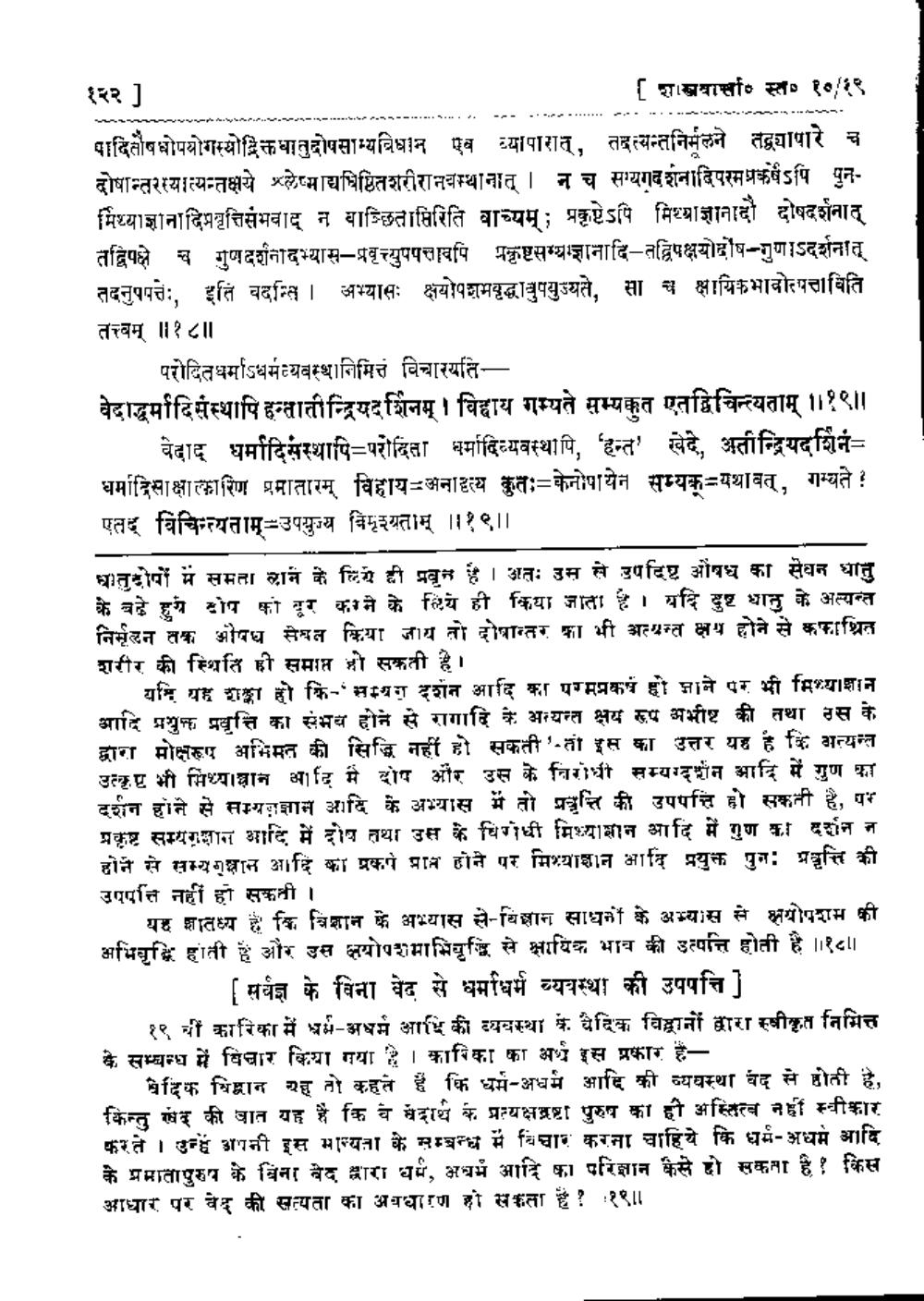________________
१२२]
[ शासवा० स्त. १०/१९ पादितौषधोपयोगस्योद्रिक्तधातुदोषसाम्यविधान एवं व्यापारात्, तदत्यन्तनिर्मलने तयापारे च दोषान्तरस्यात्यन्तक्षये लेष्माद्यधिष्ठितशरीरानवस्थानात् । न च सम्यगदर्शनादिपरमप्रकऽपि पुनमिथ्याज्ञानादिप्रवृत्तिसंभवाद् न याञ्छिताप्तिरिति वाच्यम् ; प्रकृष्टेऽपि मिथ्याज्ञानादौ दोषदर्शनात् तद्विपक्षे च गुणदर्शनादभ्यास-प्रवृत्त्युपपत्तावपि प्रकृष्टसम्य ज्ञानादि-तद्विपक्षयोदोष-गुणाऽदर्शनात् तदनुपपत्तेः, इति वदन्ति । अभ्यासः क्षयोपशमवृद्धावुपयुज्यते, सा च क्षायिकभावोत्पत्ताविति तत्त्वम् ॥१८॥
परोदितधर्माऽधर्मव्यवस्थानिमित्तं विचारयतिवेदाद्धर्मादिसंस्थापि हन्तातीन्द्रियदर्शिनम् । विद्दाय गम्यते सम्यकुत एतद्विचिन्त्यताम् ।।१९।।
वेदाद् धर्मादिसंस्थापि-परोदिता धर्मादित्यवस्थापि, 'हन्त' खेदे, अतीन्द्रियदर्शिनधर्मादिसाक्षात्कारिण प्रमातारम् विहाय अनादृत्य कुतः केनोपायेन सम्यक् यथावत्, गम्यते ? एतद् विचिन्त्यताम् उपयुज्य विमृश्यताम् ।।१९।।
धातुदोषों में समता लाने के दिये ही प्रवृन है । अतः उम से उपदिष्ट औषध का सेवन धातु के बढ़े हुये शेप को दूर करने के लिये ही किया जाता है। यदि दुष्ट धातु के अत्यन्त निर्मलन तक औषध सेवन किया जाय तो दोषान्तर का भी अत्यन्त क्षय होने से कफाश्रित शरीर की स्थिति ही समाप्त हो सकती है।
यदि यह शङ्का हो कि- सम्यग दर्शन आदि का परमप्रकर्ष हो जाने पर भी मिथ्याशान आदि प्रयुक्त प्रवृत्ति का संभव होने से रागादि के अत्यन्त क्षय रूप अभीष्ट की तथा उस के द्वान मोक्षरूप अभिमत की सिद्धि नहीं हो सकती' तो इस का उत्तर यह है कि अत्यन्त उत्कट भी मिथ्यावान आदि में दोप और उसके निधी सम्यग्दर्शन आदि में गुण का दर्शन होने से सम्यनज्ञान आदि के अभ्यास में तो प्रवृत्ति की उपपत्ति हो सकती है, पर प्रकृष्ट सम्यगशान आदि में दोष तथा उस के धिगंधी मिश्यामान आदि में गुण का दर्शन न होने से सम्यगशान आदि का प्रकर्ष प्रात होने पर मिश्याज्ञान आदि प्रयुक्त पुन: प्रवृत्ति की उपपत्ति नहीं हो सकती।
यह ज्ञातध्य है कि विज्ञान के अभ्यास ले-यिशान साधनों के अभ्यास से भयोपशम की अभिवृद्धि होती हैं और उस क्षयोपशमाभिवृद्धि से क्षायिक भाव की उत्पत्ति होती है ||१८||
सर्वज्ञ के विना वेद से धर्माधर्म व्यवस्था की उपपत्ति] १९ ची कारिका में धर्म-अधर्म आधि की व्यवस्था के चैदिक विद्वानों द्वारा स्वीकृत निमित्त के सभ्यन्ध में विचार किया गया है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है
धेदिक विद्वान यह तो कहते हैं कि धर्म-अधर्म आदि की व्यवस्था बंद से होती है, किन्तु वंद की बात यह है कि वे धंदार्थ के प्रत्यक्षवष्टा पुरुष का ही अस्तित्व नहीं स्वीकार करते । उन्हें अपनी इस मान्यता के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये कि धर्म-अधर्म आदि के प्रमातापुरुष के बिना वेद द्वारा धर्म, अधर्म आदि का परिज्ञान कैसे हो सकता है ? किस आधार पर वेद की सत्यता का अवधारण हो सकता है? :१९।।