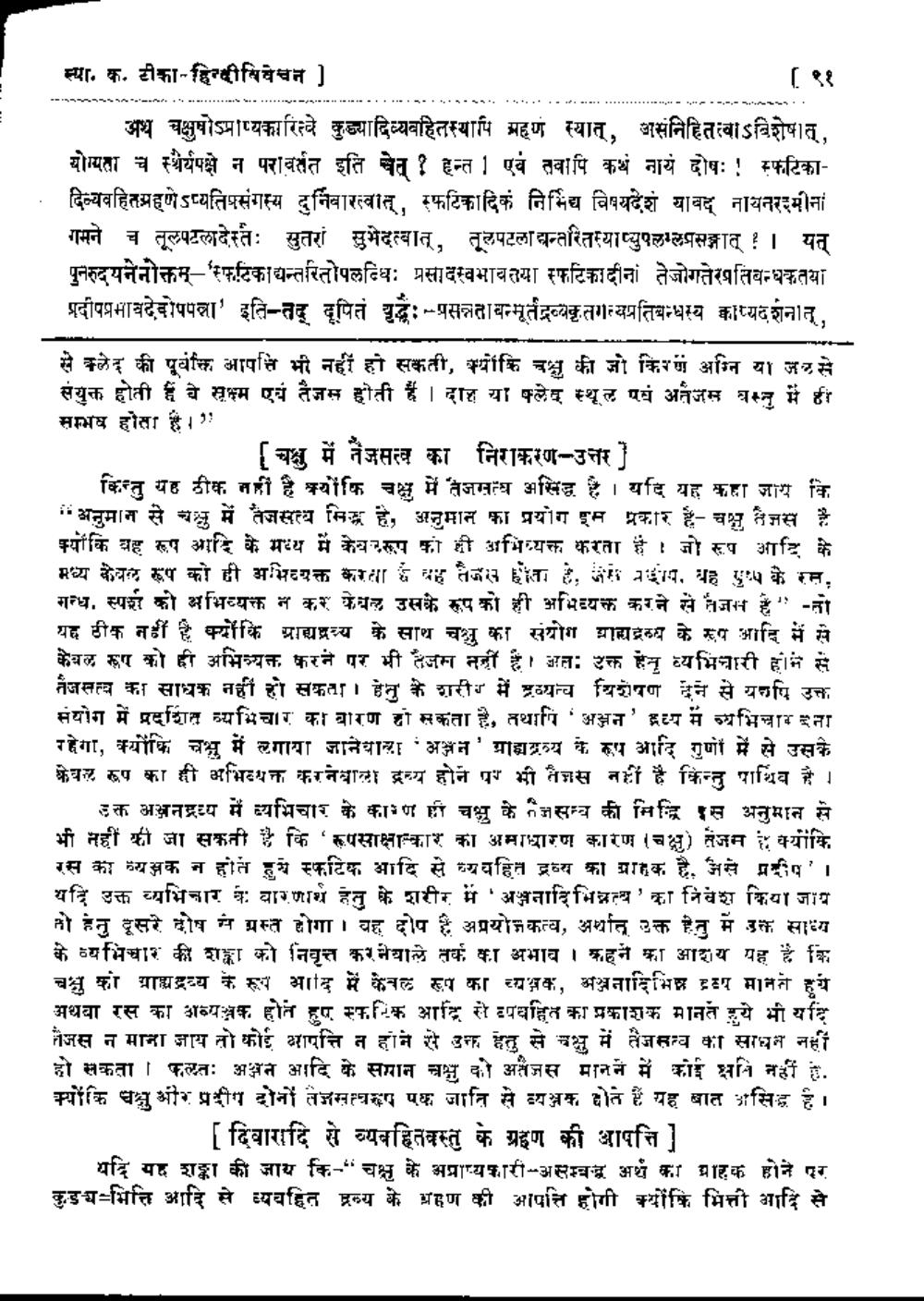________________
स्पा. क. टीका-हिन्दी विवेचन ]
1
अथ चक्षुषोsमाप्यकारित्वे कुच्यादिव्यवहितस्यापि ग्रहणं स्यात्, असंनिहितत्वाविशेषात् योग्यता च स्थैर्यपक्षे न परावर्तत इति चेत् ? हन्त । एवं तवापि कथं नायं दोषः ! स्फटिकादिव्यवहितग्रहणेऽप्यतिप्रसंगस्य दुर्निवारत्वात् स्फटिकादिकं निर्भिद्य विषयदेशं यावद् नायनरश्मीना गमने च तूलपटलादेस्तैः सुतरां सुभेदत्वात्, तूलपटला अन्तरितस्याप्युपलग्लासङ्गात् । यत् पुनरुदयने नोक्तम्- 'स्फटिकाद्यन्तरितोपलब्धिः प्रसादस्वभावतया स्फटिकादीनां तेजोगते खतिबन्धकतथा प्रदीपप्रभावदेवोपपन्ना' इति तद् दूषितं वृद्धै::- प्रसन्नता बन्मूर्त द्रव्यकृतगव्यप्रतिबन्धस्य काप्यदर्शनात्,
[ ९१
से क्लेद की पूर्वक आपत्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि चक्षु की जो किरणं अग्नि या जबसे संयुक्त होती हैं ये सूक्ष्म एवं तैजस होती हैं | दात या क्लेव स्थूल एवं अतेजस वस्तु में सम्भव होता है। "
[ चक्षु में
सत्व का निराकरण-उत्तर ]
किन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि चक्षु में तेजत्य असिद्ध है। यदि यह कहा जाय कि "अनुमान से चल में तेजय मिश्र है, अनुमान का प्रयोग इस प्रकार है- चल तेजस है क्योंकि यह रूप आदि के मध्य में केववरूप को ही अभिव्यक्त करता है। जो रूप आदि के मध्य केवल रूप को ही अभिव्यक्त करता है वह तेजस होता है, जैसे वह पुष्प के रम, गन्ध, स्पर्श को अभिव्यक्त न कर केवल उसके रूप को ही अभिव्यक्त करने से तेजस है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि माद्यद्रव्य के साथ चक्षु का संयोग प्रायद्रव्य के रूप आदि में से केवल रूप को ही अभिव्यक्त करने पर भी तेज नहीं है। अतः उक्त हेतु व्यभिचारी होने से
त्वका साधक नहीं हो सकता हेतु के शरीर में प्रव्यत्व विशेषण देने से यद्यपि उक्त संयोग में प्रदर्शित व्यभिचार का बारण हो सकता है, तथापि 'अञ्जन' द्रव्य में व्यभिचारा रहेगा, क्योंकि चभ्रु में लगाया जानेवाला अञ्जन ग्राह्मक्रय के रूप आदि गुणों में से उसके केवल रूप का ही अभिव्यक्त करनेवाला द्रव्य होने पर भी तेजस नहीं है किन्तु पार्थिव है ।
'
उक्त अञ्जनद्रव्य में व्यभिचार के कारण ही चक्षु के तेजसम्व की मिद्धि इस अनुमान से भी नहीं की जा सकती है कि 'रूपसाक्षात्कार का असाधारण कारण (चक्षु) तेजम है क्योंकि रस का व्यञ्जक न होते हुये स्फटिक आदि से व्यवहित द्रव्य का हक है. जैसे मदी । यदि उक्त व्यभिचार के वारणार्थ हेतु के शरीर में 'अञ्जनादिभिन्नत्व' का निवेश किया जाय तो हेतु दूसरे दोष से ग्रस्त होगा। यह दोष है अप्रयोजकत्व, अर्थात् उक्त हेतु में उक्त साध्य के व्यभिचार की शङ्का को निवृत्त करनेवाले तर्क का अभाव । कहने का आशय यह है कि चक्षु को ग्राद्रव्य के रूप आदि में केवल रूप का व्यञ्जक, अञ्जनादिभिन्न मानते हुये अथवा रस का अव्यञ्जक होते हुए स्फटिक आदि से व्यवहित का प्रकाशक मानते हुये भी यदि तेजस न माना जाय तो कोई आपत्ति न होने से उन् हेतु से चक्षु में तैजसत्व का साधन नहीं हो सकता । फलतः अञ्जन आदि के समान चक्षु को अतेजस मानने में कोई क्षति नहीं है. क्योंकि चक्षु और प्रदीप दोनों तेजस्वरूप एक जाति से व्यञ्जक होते है यह बात असिद्ध है ।
[ दिवारादि से व्यवहितवस्तु के ग्रहण की आपत्ति ]
यदि यह शङ्का की जाय कि " चक्षु के अप्राप्यकारी असस्वद्र अर्थ का ग्राहक होने पर कुड-भित्ति आदि से व्यवहित द्रव्य के ग्रहण की आपत्ति होगी क्योंकि मित्ती आदि से