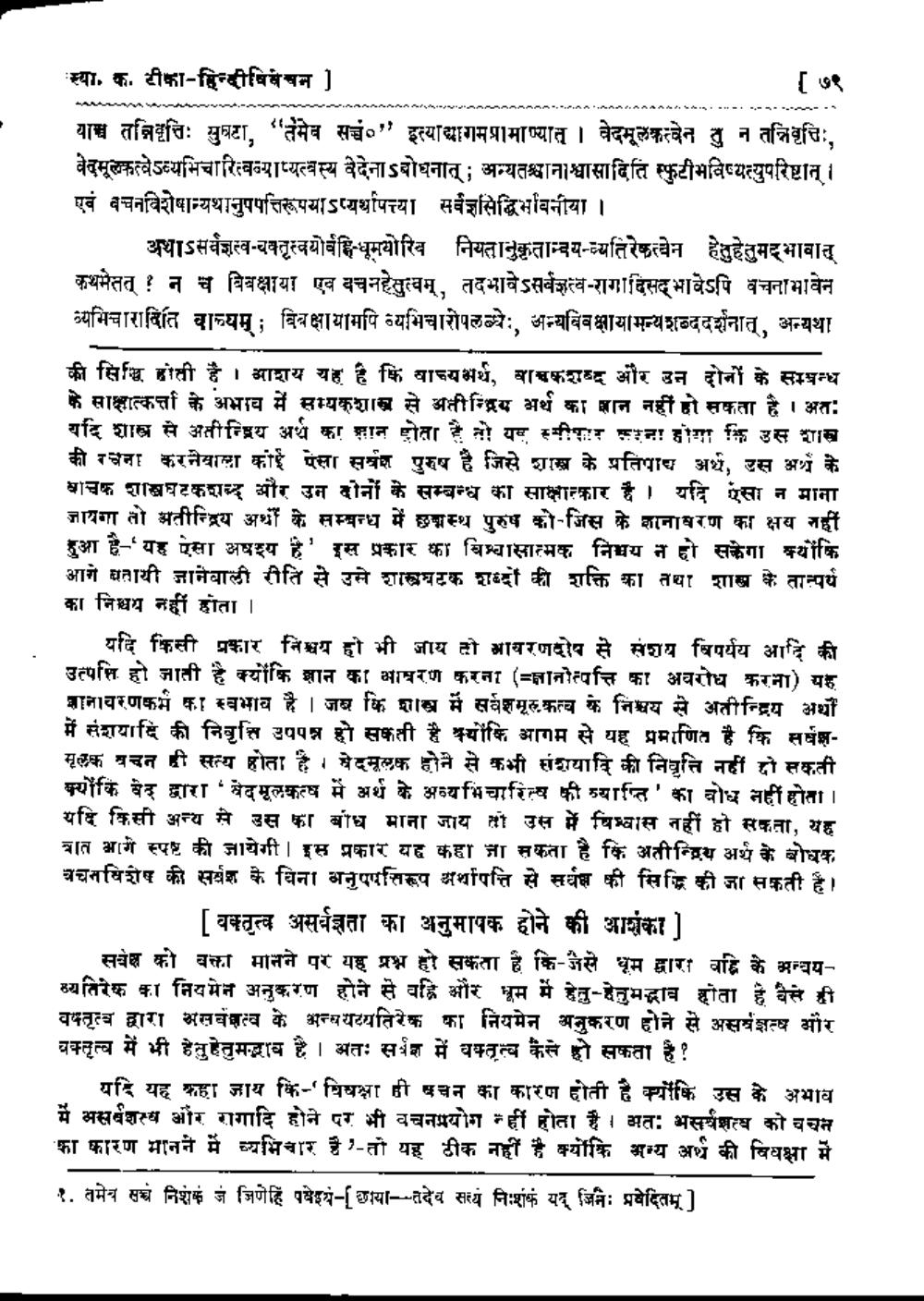________________
स्या. क. टीका-हिन्दी विवेचन ]
[ ७९
याच तन्निवृत्तिः सुघटा, "तेमेव सच्चं०" इत्याद्यागमप्रामाण्यात् । वेदमूलकत्वेन तु न तनिवृत्तिः, वेदमूलकत्वेऽव्यभिचारित्वव्याप्यत्वस्य वेदेनाऽबोधनात्; अन्यतश्वानाश्वासादिति स्फुटीभविष्यत्युपरिष्टात् । एवं वचनविशेषान्यथानुपपत्तिरूपयाऽप्यर्थापत्त्या सर्वज्ञसिद्धिर्भावनीया ।
अथाऽसर्वज्ञस्व-चक्तृत्वयोर्वहि धूमयोरिव नियतानुकृतान्वयव्यतिरेकत्वेन हेतुहेतुमद्भावात् कथमेतत् ? न च विवक्षाया एव बचनहेतुत्वम्, तदभावे ऽसर्वज्ञत्व-रागादिसद् भावेऽपि वचनाभावेन व्यभिचारादिति वाच्यम् विवक्षायामपि व्यभिचारोपलब्धेः अन्यविवक्षायामन्य शब्ददर्शनात्, अन्यथा
>
की सिद्धि होती है । आशय यह है कि वाच्यअर्थ, वाचकशब्द और उन दोनों के सम्बन्ध साक्षात्कर्त्ता के अभाव में सम्यकशास्त्र से अतीन्द्रिय अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता है । अतः यदि शास्त्र से अतीन्द्रिय अर्थ का ज्ञान होता है तो यह स्वीकार करना होगा कि उस शास्त्र की रचना करनेवाला कोई ऐसा सर्व पुरुष है जिसे शास्त्र के प्रतिपाच अर्थ, उस अर्थ के बाचक शास्त्रघटक शब्द और उन दोनों के सम्बन्ध का साक्षात्कार है। यदि ऐसा न माना जायगा तो अतीन्द्रिय अर्थो के सम्बन्ध में छमस्थ पुरुष को जिस के ज्ञानावरण का क्षय नहीं हुआ है - यह ऐसा अवश्य है' इस प्रकार का विश्वासात्मक निश्चय न हो सकेगा क्योंकि आगे बतायी जानेवाली रीति से उसे शास्त्रघटक शब्दों की शक्ति का तथा शाखा के तात्पर्य का निश्चय नहीं होता |
यदि किसी प्रकार निश्चय हो भी जाय तो आवरणदोष से संशय विपर्यय आदि की उत्पत्ति हो जाती है क्योंकि ज्ञान का आवरण करना (ज्ञानोत्पत्ति का अवरोध करना) यह ज्ञानावरणकर्म का स्वभाव है । जब कि शास्त्र में सर्वशमूलकत्व के निश्चय से अतीन्द्रिय अर्थो में संशयादि की निवृत्ति उपपन्न हो सकती है क्योंकि आगम से यह प्रमाणित है कि सर्वश मूलक वन्दन] ही सत्य होता है । वेदमूलक होने से कभी संशयादि की निवृत्ति नहीं हो सकती क्योंकि वेद द्वारा 'वेदमूलकत्व में अर्थ के अव्यभिचारित्व की व्याप्ति' का बोध नहीं होता । यदि किसी अन्य से उस का बांध माना जाय तो उस में विश्वास नहीं हो सकता, यह बात आगे स्पष्ट की जायेगी । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अतीन्द्रिय अर्थ के बोधक वचनविशेष की सर्वश के बिना अनुपपत्तिरूप अर्थापत्ति से सर्वेश की सिद्धि की जा सकती हैं।
[ वक्तृत्व असर्वज्ञता का अनुमापक होने की आशंका ]
सर्वेश को वक्ता मानने पर यह प्रश्न हो सकता है कि जैसे धूम द्वारा वह्नि के अन्वयव्यतिरेक का नियमेन अनुकरण होने से वह्नि और भ्रम में हेतुहेतुमद्भाव होता है वैसे ही वक्तृत्व द्वारा असवेशत्व के अन्वयव्यतिरेक का नियमेन अनुकरण होने से असत्य और वक्तृत्व में भी हेतुहेतुमद्भाव है। अतः सर्वश में वक्तृत्व कैसे हो सकता है ?
यदि यह कहा जाय कि ' विवक्षा ही बचन का कारण होती है क्योंकि उस के अभाव में सर्वशस्य और रागादि होने पर भी वचनप्रयोग नहीं होता है । अतः असर्वशत्व को वचन का कारण मानने में व्यभिचार है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि अन्य अर्थ की विवक्षा में
१. तमेव स निशंक जं जिणेहिं पवेश्यं - [ छाया -- तदेव सत्यं निःशंकं यद् जिनः प्रवेदितम् ]
: