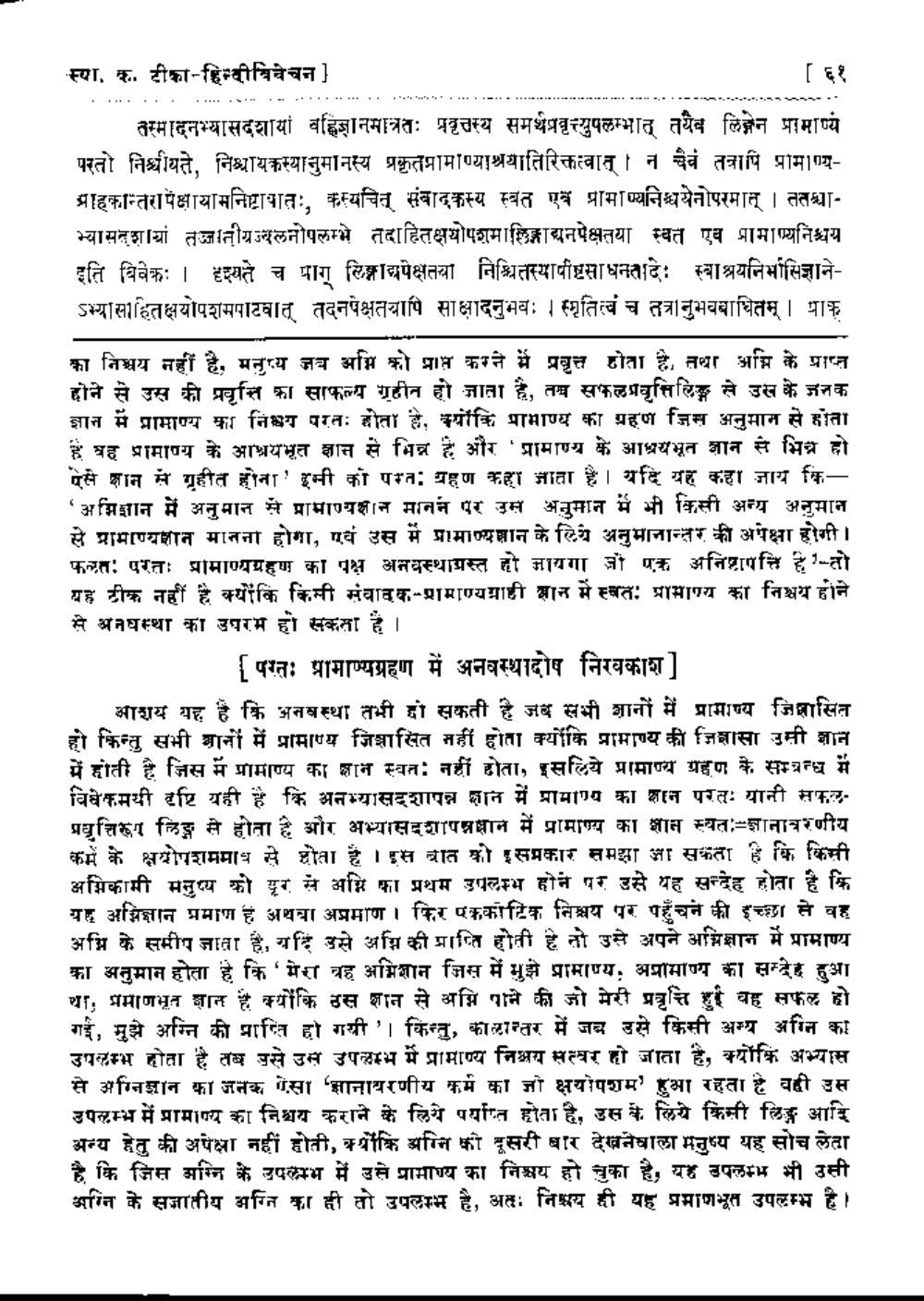________________
स्या. क. टीका-हिन्दी विवेचन ]
[ ६१
तस्मादभ्यासदशायां वह्निज्ञानमात्रतः प्रवृत्तस्य समर्थप्रवृत्युपलम्भात् तयैव लिनेन प्रामाण्य परतो निश्चीयते, निश्चायकस्यानुमानस्य प्रकृतप्रामाण्याश्रयातिरिक्तत्वात् । न चैवं तत्रापि प्रामाण्यग्राहकान्तरापेक्षायामनिष्टापातः कस्यचित् संवादकस्य स्वत एवं प्रामाण्यनिश्चयेनोपरमात् । ततश्चाभ्यासदृशायां तज्जातीयज्वलनोपलम्भे तदाहित क्षयोपशमा लिङ्गाद्यनपेक्षतया स्वत एव प्रामाण्यनिश्चय इति विवेकः । दृश्यते च प्राग् लिङ्गाद्यपेक्षतया निश्चितस्यापीष्टसाधनतादेः स्वाश्रयनिर्मासिज्ञानेऽभ्यासाहितक्षयोपशमपाटवात् तदनपेक्षतत्रापि साक्षादनुभवः । स्मृतित्वं च तत्रानुभवबाधितम् । प्राक
1
का निश्चय नहीं है, मनुष्य जब अभि को प्राप्त करने में प्रवृत्त होता है तथा अभि के प्राप्त होने से उस की प्रवृत्ति का साफल्य ग्रहीन हो जाता है, तब सफलप्रवृत्तिलिङ्ग से उस के जनक ज्ञान में प्रामाण्य का निश्चय परतः होता है, क्योंकि प्रामाण्य का ग्रहण जिस अनुमान से होता है वह प्रामाण्य के आश्रयभूत ज्ञान से भिन्न है और प्रामाण्य के आश्रयभूत ज्ञान से भिन्न हो ऐसे ज्ञान से गृहीत होना इसी को पस्तः ग्रहण कहा जाता है। यदि यह कहा जाय कि'अभिज्ञान में अनुमान से प्रामाण्यज्ञान मानने पर उस अनुमान में भी किसी अन्य अनुमान से प्रामाण्यज्ञान मानना होगा, एवं उस में प्रामान्यज्ञान के लिये अनुमानान्तर की अपेक्षा होगी । फलतः परतः प्रामाण्यग्रहण का पक्ष अनवस्थाग्रस्त हो जायगा जो एक अनिष्पत्ति है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि किमी संवादक- प्रामाण्यग्राही ज्ञान में स्वतः प्रामाण्य का निश्चय होने से अनवस्था का उपरम हो सकता है ।
[ परतः प्रामाण्यग्रहण में अनवस्थादोष निरवकाश ]
आशय यह है कि अनवस्था तभी हो सकती है जब सभी शानों में प्रामाण्य जिज्ञासित हो किन्तु सभी थानों में प्रामाण्य जिज्ञासित नहीं होता क्योंकि प्रामाण्य की जिज्ञासा उसी ज्ञान में होती है जिस में प्रामाण्य का ज्ञान स्वतः नहीं होता, इसलिये प्रामाण्य ग्रहण के सम्बन्ध में fasant दृष्टि यही है कि अनभ्यासदशापन्न ज्ञान में प्रामाण्य का शान परतः यानी सफलप्रवृत्तिरूप लिङ्ग से होता है और अभ्यासदशापान में प्रामाण्य का ज्ञान स्वतः ज्ञानावरणीय कमें के क्षयोपशमात्र से होता हैं । इस बात को इसप्रकार समझा जा सकता है कि किसी अशिकामी मनुष्य को दूर से अभि का प्रथम उपलम्भ होने पर उसे यह सन्देह होता है कि यह अभिज्ञान प्रमाण है अथवा अप्रमाण । फिर एककोटिक निश्चय पर पहुँचने की इच्छा से वह अभि के समीप जाता है, यदि उसे अग्नि की प्राप्ति होती है तो उसे अपने अभिज्ञान में प्रामाण्य का अनुमान होता है कि 'मेरा वह अभिज्ञान जिस में मुझे प्रामाण्य, अप्रामाण्य का सन्देद हुआ था, प्रमाणभूत ज्ञान है क्योंकि उस ज्ञान से अग्नि पाने की जो मेरी प्रवृत्ति हुई वह सफल हो गई, मुझे अग्नि की प्राप्ति हो गयी । किन्तु कालान्तर में जब उसे किसी अन्य अग्नि का उपलम्भ होता है तब उसे उस उपलम्भ में प्रामाण्य निक्षय सत्वर हो जाता है, क्योंकि अभ्यास से अग्निज्ञान का जनक ऐसा 'ज्ञानावरणीय कर्म का जो क्षयोपशम' हुआ रहता है वही उस उपलम्भ में प्रामाण्य का निश्चय कराने के लिये पर्याप्त होता है, उस के लिये किसी लिङ्ग आदि अन्य हेतु की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि अग्नि को दूसरी बार देखनेवाला मनुष्य यह सोच लेता है कि जिस अग्नि के उपलम्भ में उसे प्रामाण्य का निश्चय हो चुका है, यह उपलम्भ भी उसी अग्नि के सजातीय अग्नि का ही तो उपलम्भ है, अतः निश्चय ही यह प्रमाणभूत उपलम्भ है।