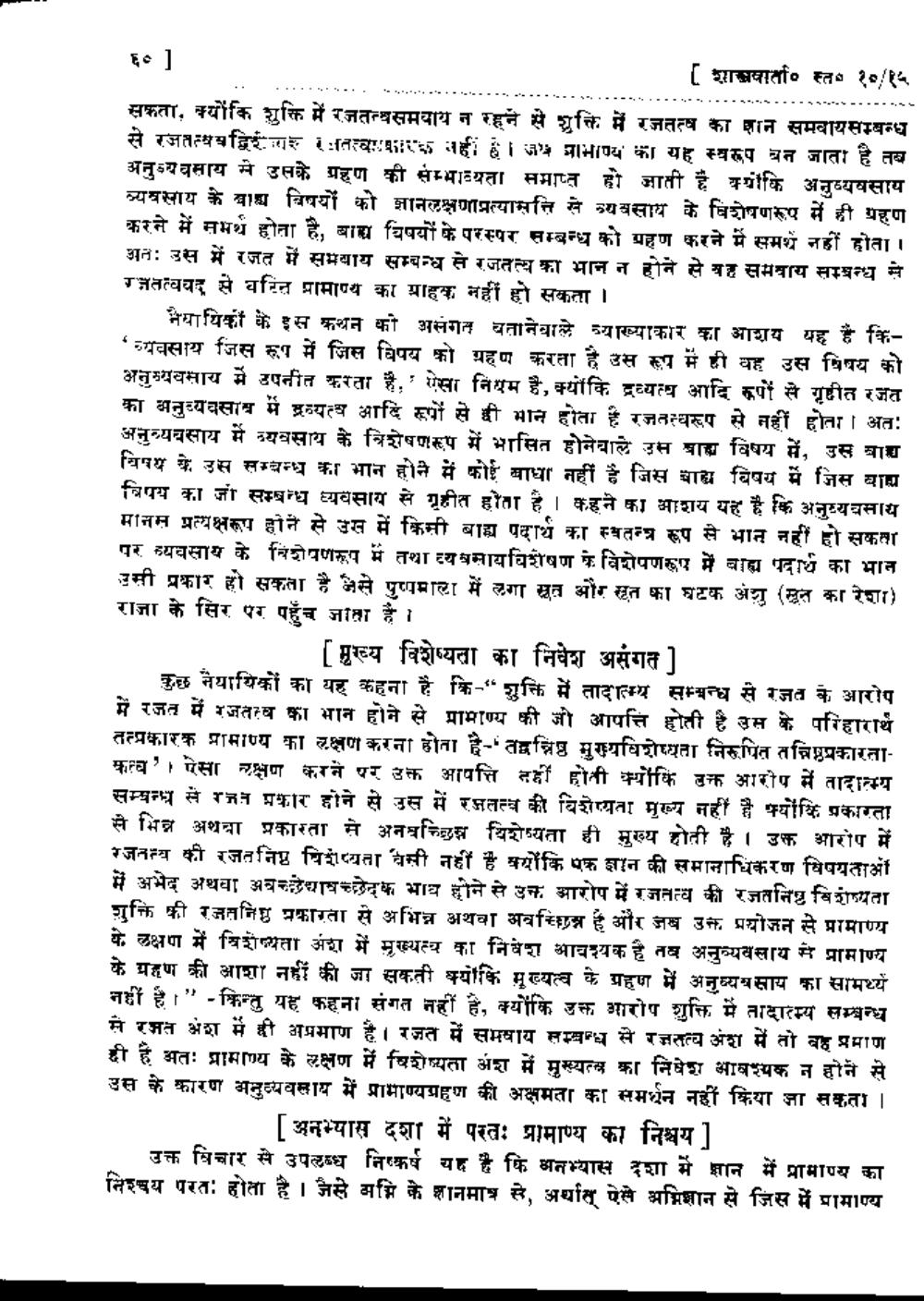________________
६. ]
[ शासवार्ता० स्तः १०/१५
सकता, क्योंकि शुक्ति में रजतन्यसमयाय न रहने से शुक्ति में रजतत्व का ज्ञान समवायसम्बन्ध से रजतत्वयाद्विरक तत्वा कारक नहीं। जय प्रामाण्य का यह स्वरूप बन जाता है तब अनुब्यवसाय मे उसके ग्रहण की सम्भाव्यता समाप्त हो जाती है क्योंकि अनुष्यवसाय व्यवसाय के बाद्य विषयों को ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति से व्यवसाय के विशेषणरूप में ही ग्रहण करने में समर्थ होता है, बाय विषयों के परस्पर सम्बन्ध को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता। अत: उस में रजत में समयाय सम्बन्ध से रजतत्व का भान न होने से यह समवाय सम्बन्ध में ग्जतत्ववद से पनि प्रामाण्य का ग्राहक नहीं हो सकता ।
नैयायिकों के इस कथन को असंगत बताने वाले व्याख्याकार का आशय यह है कि'व्यवसाय जिस रूप में जिस विषय को ग्रहण करता है उस रूप में ही वह उस विषय को अनुम्यवसाय में उपनीत करता है, ऐसा नियम है, क्योंकि द्रव्यत्य आदि रूपों से गृष्टीत रजत का अनुव्यवसाय में द्रव्यत्व आदि रूपों से ही मान होता है रजतस्वरूप से नहीं होता। अत: अनुन्यबसाय में व्यवसाय के विशेषणरूप में भासित होनेवाले उस बाह्य विषय में, उस वाद्य विषय के उस सम्बन्ध का भान होने में कोई बाधा नहीं है जिस बाह्य विषय में जिस बाय विषय का जो सम्बन्ध ध्यवसाय से गृहीत होता है। कहने का आशय यह है कि अनुय्यवसाय मानम प्रत्यक्षरूप होने से उस में किमी बाद्य पदार्थ का स्वतन्त्र रूप से भान नहीं हो सकता पर व्यवसाय के विशेषणरूप में तथा व्यवसायविशेषण के विशेपणरूप में बाह्य पदार्थ का भान उसी प्रकार हो सकता है जैसे पुष्पमाला में लगा सूत और सूत का घटक अंशु (मत का रेशा) राजा के सिर पर पहुँच जाता है।
[मुख्य विशेष्यता का निवेश असंगत ] कुछ नैयायिकों का यह कहना है कि-"शुक्ति में तादात्म्य सम्बन्ध से रजत के आरोप में रजत में रजताय का भान होने से मामाण्य की जो आपत्ति होती है उस के परिहारार्थ तत्प्रकारक प्रामाण्य का लक्षण करना होता है-'तनिष्ठ मुख्यविशेष्यता निरुपित तनिष्ठप्रकारताफत्व'। ऐसा लक्षण करने पर उक्त आपत्ति नहीं होती क्योंकि उक्त आरोप में तादात्म्य सम्बन्ध से गन प्रकार होने से उस में रजतत्व की विशेष्यता मुख्य नहीं है क्योंकि प्रकारता से भिन्न अथवा प्रकारता से अनवच्छिन्न विशेष्यता ही मुख्य होती है । उक्त आरोप में रजतत्य की रजत निष्ठ विशेयता बसी नहीं है क्योंकि पक ज्ञान की समानाधिकरण विषयताओं में अभेद अथवा अवच्छेद्यावच्छेदक भाव होने से उन आरोप में रजतत्व की रजतनिष्ट विशेष्यता शुक्ति की रजतनिष्ठ प्रकारता से अभिन्न अथवा अवभिन्न है और जब उन प्रयोजन से प्रामाण्य के लक्षण में विशेष्यता अंश में मुख्यत्व का निवेश आवश्यक है नव अनुव्यवसाय में प्रामाण्य के ग्रहण की आशा नहीं की जा सकती क्योंकि मुख्यत्व के ग्रहण में अनुव्यवसाय का सामर्थ्य नहीं है।" - किन्तु यह कहना संगत नहीं है, क्योंकि उक्त आरोप शुक्ति में तादात्म्य सम्बन्ध में रमत अंश में ही अप्रमाण है। रजत में समवाय सम्बन्ध से रजसत्व अंश में तो वह प्रमाण ही है अतः प्रामाण्य के लक्षण में विशेष्यता अंश में मुख्यत्म का निधेश आवश्यक न होने से उस के कारण अनुव्यवसाय में प्रामाण्यग्रहण की अक्षमता का समर्थन नहीं किया जा सकता ।
[अनभ्यास दशा में परतः प्रामाण्य का निश्चय ] उक्त विचार से उपलब्ध निष्कर्ष यह है कि अनभ्यास दशा में ज्ञान में प्रामाण्य का निश्चय परत: होता है । जैसे ममि के शानमात्र से, अर्थात् ऐसे अग्निशान से जिस में प्रामाण्य