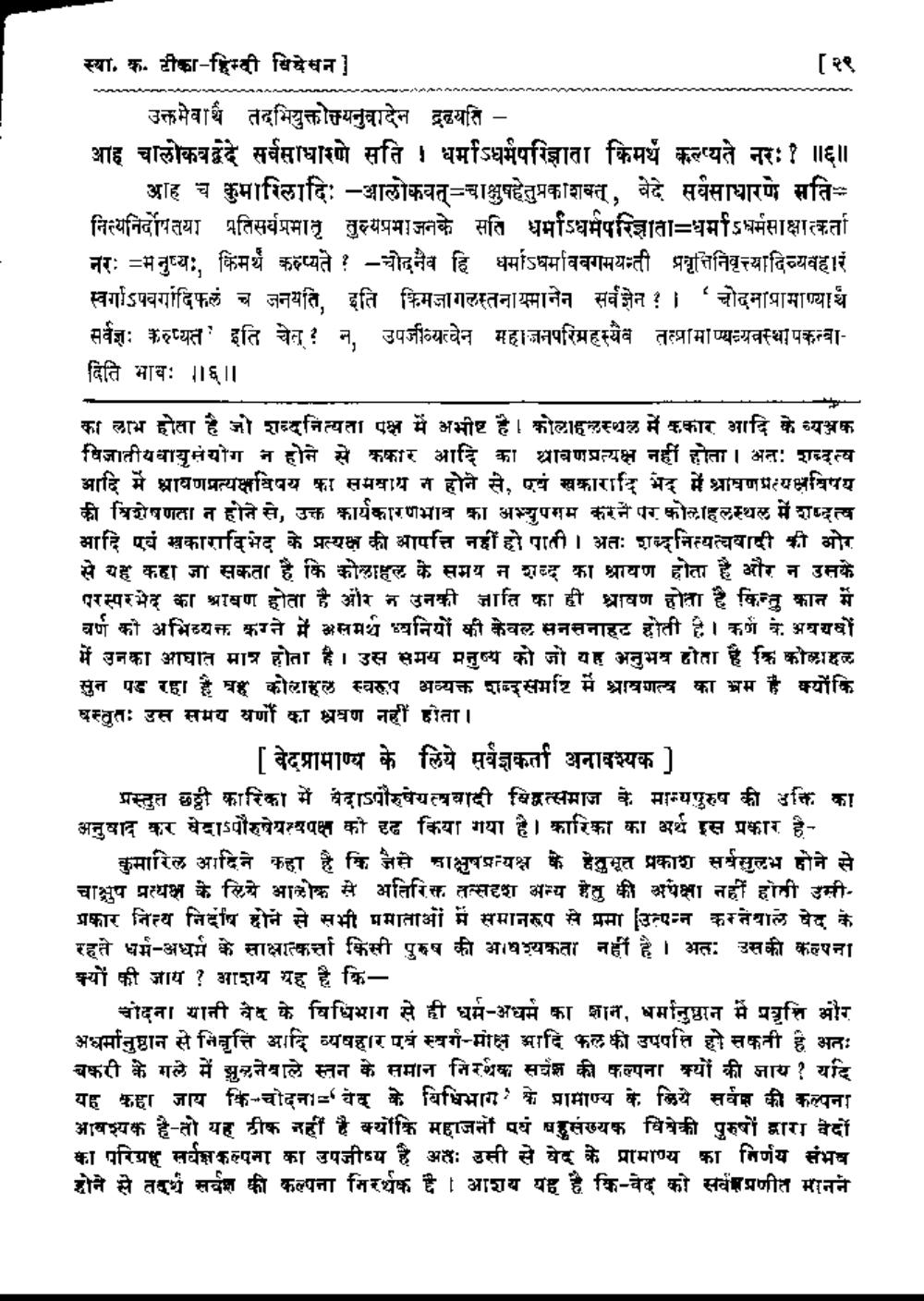________________
स्था. क. टीका-हिन्दी विवेचन]
उक्तमेवार्थ तदभियुक्तोक्त्यनुवादेन द्रढयति - आह चालोकवद्वदे सर्वसाधारणे सति । धर्माऽधर्मपरिज्ञाता किमर्थं कल्प्यते नरः ॥६॥
आह च कुमाग्लिादिः -आलोकवत्-चाक्षुषहेतुप्रकाशवत् , वेदे सर्वसाधारण मतिः नित्यनिर्दोषतया प्रतिसर्यप्रभातृ तुल्यप्रमाजनके सति धर्माऽधर्मपरिज्ञाता धर्माधर्मसाक्षात्कर्ता नरः =मनुष्यः, किमर्थं कल्प्यते ? –चोदनैव हि धर्माऽधर्माववगमयन्ती प्रवृत्तिनिवृत्त्यादिव्यवहार स्वर्गाऽपवर्गादिफलं च जनयति, इति किमजागलस्तनायमानेन सर्वज्ञेन ? । 'चोदनापामाण्यार्थ सर्वज्ञः करुयत' इति चेन ? न, उपजीव्यत्वेन महाजनपरिग्रहस्यैव तत्प्रामा प्यन्यवस्था पकन्वादिति भावः ॥६॥
का लाभ होता है जो शब्दनित्यता पक्ष में अभीष्ट है। कोलाहलस्थल में ककार आदि के व्यञ्जक विजातीयवायुमेयोग न होने से ककार आदि का श्रावणप्रत्यक्ष नहीं होता। अतः शब्दत्व आदि में श्रायणप्रत्यक्षविषय का समवाय न होने से, पवं खकारादि भेद में श्रावण प्रत्यक्षविषय की विशेषणता न होने से, उक्त कार्यकारणभाव का अभ्युपगम करने पर कोलाहलस्थल में शब्दत्व आदि पवं सकारादिभेद के प्रत्यक्ष की आपत्ति नहीं हो पाती। अतः शब्दनित्यत्ववादी की ओर से यह कहा जा सकता है कि कोलाहल के समय न शब्द का श्रावण होता है और न उसके परस्परभेद का श्रावण होता है और न उनकी जाति का ही श्रावण होता है किन्तु कान में वर्ण को अभिव्यक्त करने में असमर्थ ध्वनियों को केवल सनसनाहट होती है। कण के अवयवों में उनका आघात मात्र होता है। उस समय मनुष्य को जो यह अनुभव होता है कि कोलाहल सुन पड रहा है यह कोलाहल स्वरूप अव्यक्त शइसमष्टि में श्रावणत्व का भ्रम है क्योंकि घस्वतः उस समय बों का भ्रषण नहीं होता।
[ वेदप्रामाण्य के लिये सर्वज्ञकर्ता अनावश्यक ] प्रस्तुत छठी कारिका में बेदाऽपौरुषेयत्ववादी विद्वत्समाज के मान्यपुरुष की उक्ति का अनुवाद कर वेदापौरुषेयस्यपक्ष को हर किया गया है। कारिका का अर्थ इस प्रकार है
कुमारिल आदिने कहा है कि जैसे हानुषप्रत्यक्ष के हेतुभूत प्रकाश सर्वसुलभ होने से चाक्षुप प्रत्यक्ष के लिये आरोक से अतिरिक्त तत्सदृश अन्य हेतु की अपेक्षा नहीं होती उसी. प्रकार नित्य निर्दोष होने से सभी प्रमाताओं में समानरूप से प्रमा उत्पन्न करने वाले घेद के रहते धर्म-अधर्म के साक्षात्कर्ता किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं है। अतः उसकी कल्पना क्यों की जाय ? आशय यह है कि
चोदना थानी वैद के विधिभाग से ही धर्म-अधर्म का शान, धर्मानुष्ठान में प्रवृत्ति और अधर्मानुष्ठान से निवृत्ति आदि व्यवहार पर्व स्वर्ग-मोक्ष आदि फल की उपपत्ति हो सकती है अतः बकरी के गले में झुलनेवाले स्तन के समान निरर्थक सर्वेश की कल्पना क्यों की जाय? यदि यह कहा जाय कि-चोदना वेद के बिधिभाग के प्रामाण्य के लिये सर्वन की कल्पना आवश्यक है-तो यह ठीक नहीं है क्योंकि महाजनों पयं बहुसंख्यक विवेकी पुरुषों द्वारा वेदों का परिग्रह सर्वज्ञकल्पना का उपजीष्य है अतः उसी से वेद के प्रामाण्य का निर्णय संभव होने से तदर्थ सर्वश की कल्पना मिरर्थक है । आशय यह है कि-वेद को सर्वशप्रणीत मानने