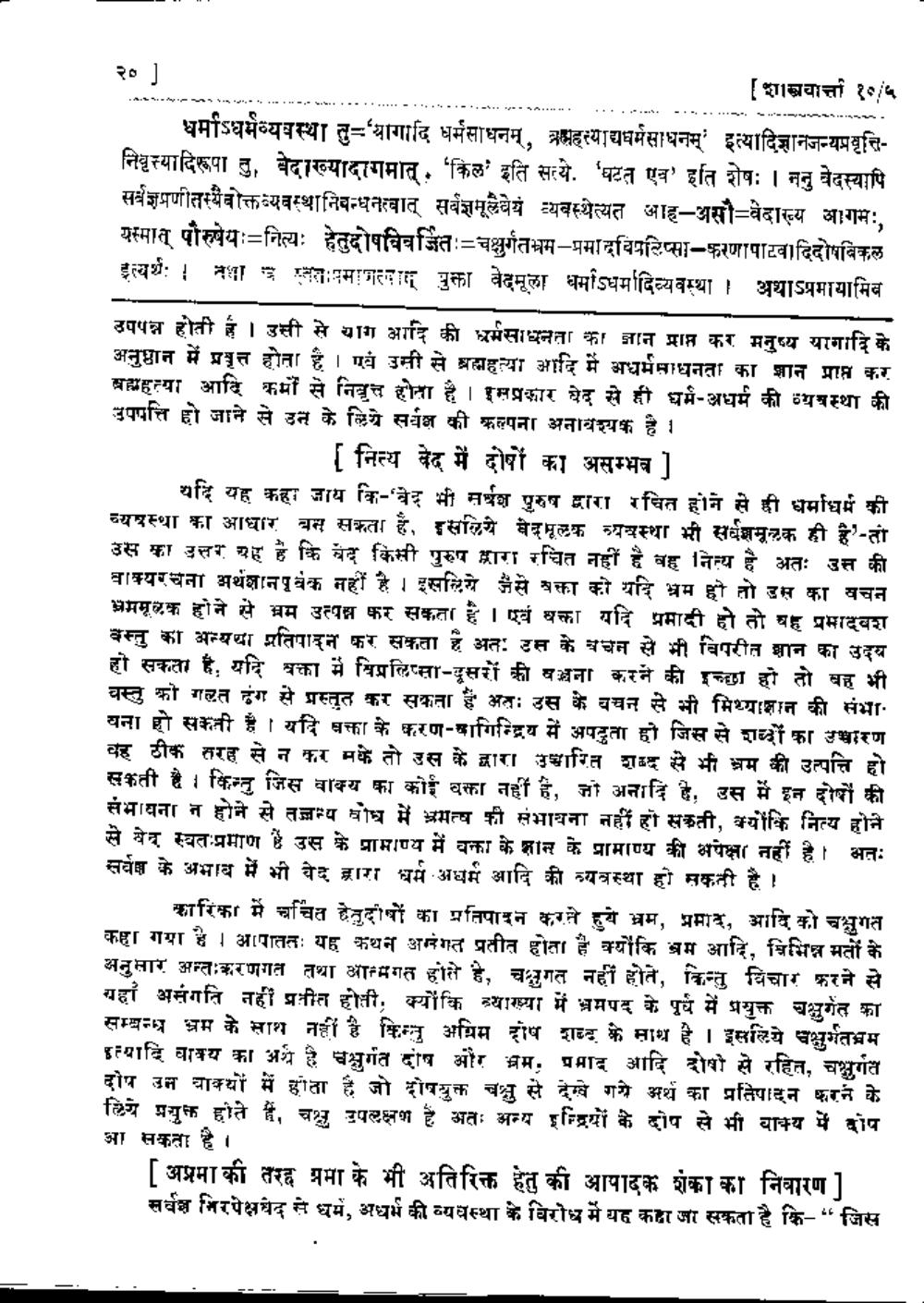________________
[शास्त्रवार्ता १०५ धर्माऽधर्मव्यवस्था तु='यागादि धर्मसाधनम् , अमहत्याद्यधर्मसाधनम्' इत्यादिज्ञानजन्यप्रवृत्तिनिवृत्यादिरूपा तु, वेदाख्यादागमात् . 'किल' इति सत्ये. 'घटत एव' इति शेषः । ननु वेदस्यापि सर्वज्ञप्रणीतस्यैवोक्त व्यवस्था निवन्धनत्वात् सर्वज्ञमूलवेयं व्यवस्थेत्यत आह-असौ वेदारख्य आगमः, यस्मात् पौरुषेयः नित्यः हेतुदोषविवर्जितः चक्षुर्गतभ्रम-प्रमादविपलिप्सा-फरणापाटवादिदोषविकल इत्यर्थः । नक्षा - लता मागत्माम् युक्ता वेदमूला धर्माऽधर्मादिव्यवस्था । अथाऽप्रमायामिव
उपपन्न होती है । उसी से याग आदि की धर्मसाधनता का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य यागादि के अनुष्ठान में प्रवृत्त होता है । एवं उमी से ब्रह्महत्या आदि में अधर्मसाधनता का ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्महत्या आदि कर्मों से निवृत्त होता है । इस प्रकार घेद से ही धर्म-अधर्म की व्यवस्था की उपपत्ति हो जाने से उन के लिये सर्वन की कल्पना अनावश्यक है।
[नित्य वेद में दोषों का असम्भव ] यदि यह कहा जाय कि-'वेद भी मर्धश पुरुष द्वारा रचित होने से ही धर्माधर्म की व्यवस्था का आधार बन सकता है, इसलिये वेदमूलक व्यवस्था भी सर्वशमूलक ही है'-ती उस का उत्तर यह है कि बंद किसी पुरुष द्वारा रचित नहीं है वह नित्य है अतः उस की वाक्यरचना अर्थशान पूर्वक नहीं है । इसलिये जैसे वक्ता को यदि भ्रम हो तो उस का वचन भ्रममूलक होने से भ्रम उत्पन्न कर सकता है । एवं धक्ता यदि प्रमादी हो तो यह प्रमादवश वस्तु का अन्यथा प्रतिपादन कर सकता है अतः उस के बचन से भी विपरीत शान का उदय हो सकता है, यदि वक्ता में विप्रलिप्सा-इसरों की वञ्चना करने की इच्छा हो तो वह भी वस्तु को गलत ढंग से प्रस्तुत कर सकता है. अतः उस के वचन से भी मिथ्याशान की संभा. यना हो सकती है। यदि वक्ता के करण-बागिन्द्रिय में अपटुता हो जिस से शब्दों का उच्चारण वह ठीक तरह से न कर मके तो उस के द्वारा उचारित शब्द से भी भ्रम की उत्पत्ति हो सकती है। किन्तु जिस वाक्य का कोई वक्ता नहीं है, जो अनादि है, उस में इन दोशै की संभावना न होने से तजन्य वोध में भ्रमत्य की संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि नित्य होने से वेद स्वतःप्रमाण हैं उस के प्रामाण्य में वका के ज्ञान के प्रामाण्य की अपेक्षा नहीं है। अतः सर्वश के अभाव में भी वेद द्वारा धर्म अधर्म आदि की व्यवस्था हो सकती है।
कारिका में चित हेतुदीषों का प्रतिपादन करते हुये भ्रम, प्रमाद, आदि को चक्षुगत कहा गया है । आपाततः यह कथन अग्गत प्रतीत होता है क्योंकि भ्रम आदि, विभिन्न मतों के अनुसार अन्तःकरणगत तथा आन्मगत होते है, चक्षुगत नहीं होते, किन्तु विचार करने से ग्रहां असंगति नहीं प्रतीत होती, क्योंकि व्याख्या में श्रमपद के पूर्व में प्रयुक्त चक्षुर्गत का सम्बन्ध भ्रम के साथ नहीं है किन्तु अग्रिम दोष शब्द के माथ है । इसलिये चक्षुर्मतभ्रम इत्यादि वाक्य का अर्थ है चक्षुर्गत दोष और भ्रम, प्रमाद आदि दोषो से रहित, चक्षुर्गत दोष उम याक्यों में होता है जो दोषयुक्त चक्षु से देग्वे गये अर्थ का प्रतिपादन करने के लिये प्रयुक्त होते हैं, चक्षु उपलक्षश है अतः अन्य इन्द्रियों के दोष से भी वाक्य में दोप आ सकता है।
[अप्रमा की तरह प्रमा के भी अतिरिक्त हेतु की आपादक शंका का निवारण] सर्व निरपेक्षधेद से धर्म, अधर्भ की व्यवस्था के विरोध में यह कहा जा सकता है कि- “ जिस