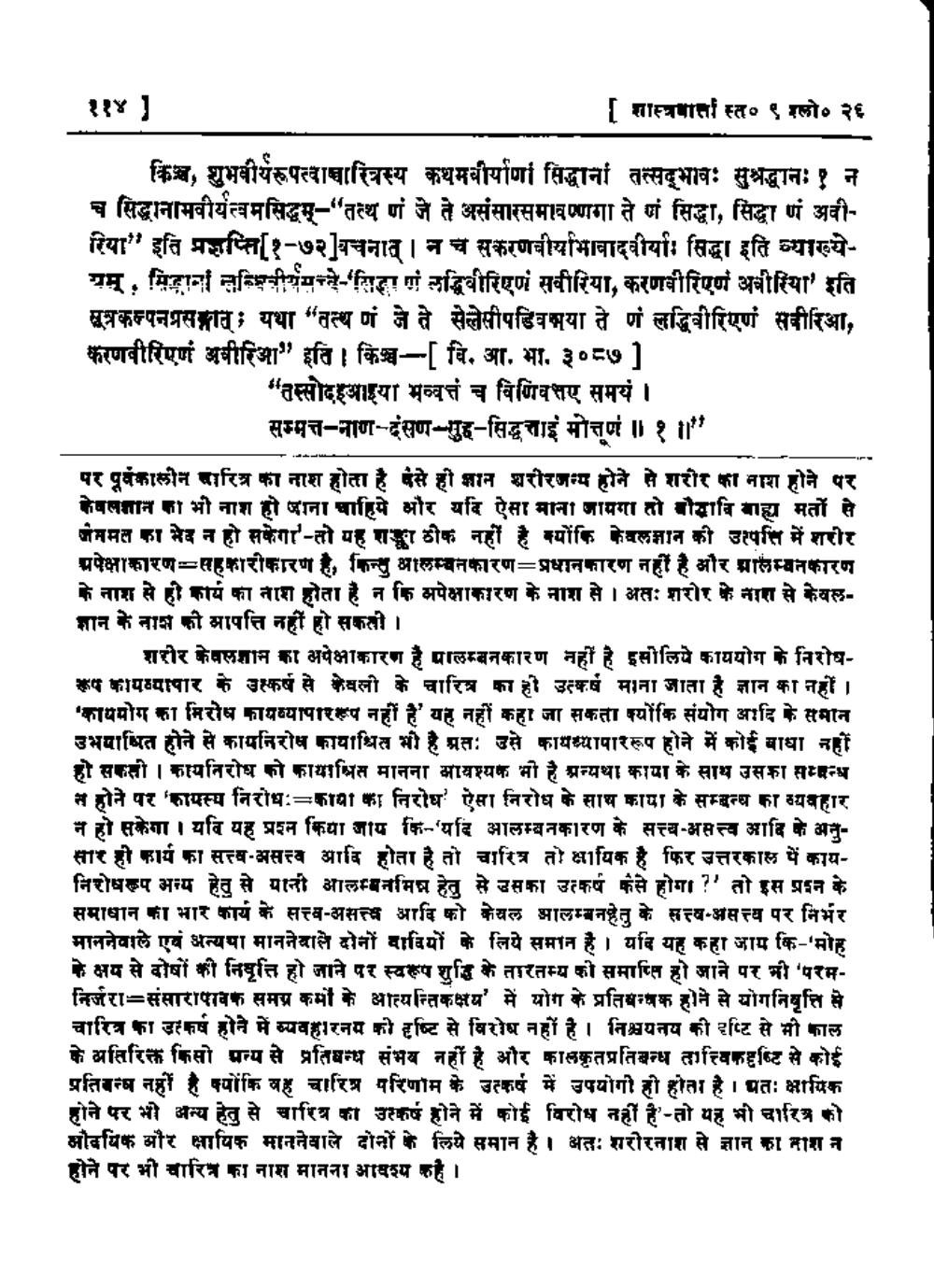________________
११४ ]
[ शास्त्रमा स्त० ९ श्लो० २६
किश्च शुभवरूपत्वाचारित्रस्य कथमवीर्यार्णा सिद्धानां तत्सद्भावः सुश्रद्धानः १ न च सिद्धानामवीर्यत्वमसिद्धम् - " तत्थ णं जे ते असंसारसमावण्णा ते णं सिद्धा, सिद्धा णं अवीरिया" इति प्रज्ञप्ति [१-७२ ] वचनात् । न च सुकरणचीर्याभावादवीर्याः सिद्धा इति व्याख्येयम् महान मन्त्रे- 'सिद्धा लद्भिवीरिएणं सवीरिया, करणवीरिएणं अवीरिया' इति सूत्रकम्पनप्रसङ्गात् यथा “तस्थ णं जे ते सेलेसीपडिवमया ते णं लद्विवीरिएणं सवीरिआ, करणवीरिएणं अभीरिआ" इति । किश्व - [ वि. आ. भा. ३०८७ ]
" तरसोद या मव्वत्तं च विविए समयं ।
सम्मत्त - नाण- दंसण-सुद्द - सिद्धताई मोत्तूणं ॥ १ ॥ "
पर पूर्वकालीन चारित्र का नाश होता है इसे ही ज्ञान शरीरजन्य होने से शरीर का नाश होने पर केवलज्ञान का भी नाश हो जाना चाहिये और यदि ऐसा माना जायगा तो बौद्धावि बाह्य मतों से जगमल का भेद न हो सकेगा तो यह शङ्का ठीक नहीं है क्योंकि केवलज्ञान की उत्पत्ति में शरीर अपेक्षाकारण सहकारीकारण है, किन्तु आलम्बनकारण प्रधान कारण नहीं है और प्रालम्बनकारण के नाश से ही कार्य का नाश होता है न कि अपेक्षाकारण के नाश से। अतः शरीर के नाश से केवलज्ञान के नाश की आपत्ति नहीं हो सकती ।
=
शरीर केवलज्ञान का अपेक्षाकारण है प्रालम्बनकारण नहीं है इसीलिये काययोग के निशेषरूप कायव्यापार के उत्कर्ष से केवली के चारित्र का ही उत्कर्ष माना जाता है ज्ञान का नहीं । 'काययोग का निरोष कायव्यापाररूप नहीं है' यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि संयोग अदि के समान उभाषित होने से कायनिरोध कायाधित भी है प्रतः उसे कायव्यापाररूप होने में कोई बाधा नहीं हो सकती । कायनिरोध को कायाश्रित मानना आवश्यक भी है अन्यथा काया के साथ उसका सम्बन्ध म होने पर 'कायस्य निरोधः काया का निरोध' ऐसा निरोध के साथ काया के सम्बन्ध का व्यवहार न हो सकेगा । यदि यह प्रश्न किया जाय कि यदि आलम्बनकारण के सत्य-असत्त्व आदि के अनुसार ही कार्य का सत्त्व असत्त्व आदि होता है तो चारित्र तो क्षायिक है फिर उत्तरकाल में कायनिशेषरूप अन्य हेतु से यानी आलम्बनमिन हेतु से उसका उत्कर्ष कैसे होगा ?' तो इस प्रश्न के समाधान का भार कार्य के सत्त्व असत्त्व आदि को केवल आलम्बनहेतु के सत्त्व असत्त्व पर निर्भर माननेवाले एवं अन्यथा माननेवाले दोनों वादियों के लिये समान है। यदि यह कहा जाय कि 'मोह के क्षय से दोषों की निवृत्ति हो जाने पर स्वरूप शुद्धि के तारतम्य की समाप्ति हो जाने पर की 'परमनिर्जरा=संसारापावक समग्र कर्मों के आत्यन्तिकक्षय' में योग के प्रतिबन्धक होने से योगनिवृत्ति से चारित्र का उत्कर्ष होने में व्यवहारनय को दृष्टि से विशेष नहीं है । निश्चयतय की दृष्टि से मी काल के अतिरिक्त किसो प्रत्य से प्रतिबन्ध संभव नहीं है और कालकृतप्रतिबन्ध तात्त्विकद्दष्टि से कोई प्रतिबन्ध नहीं है क्योंकि वह चारित्र परिणाम के उत्कर्ष में उपयोगी हो होता है। घतः क्षायिक होने पर भी अन्य हेतु से चारित्र का उत्कर्ष होने में कोई विरोध नहीं है तो यह भी चारित्र को औयिक और क्षायिक माननेवाले दोनों के लिये समान है । अतः शरीरनाश से ज्ञान का नाश न होने पर भी चारित्र का नाश मानना आवश्यकहै ।