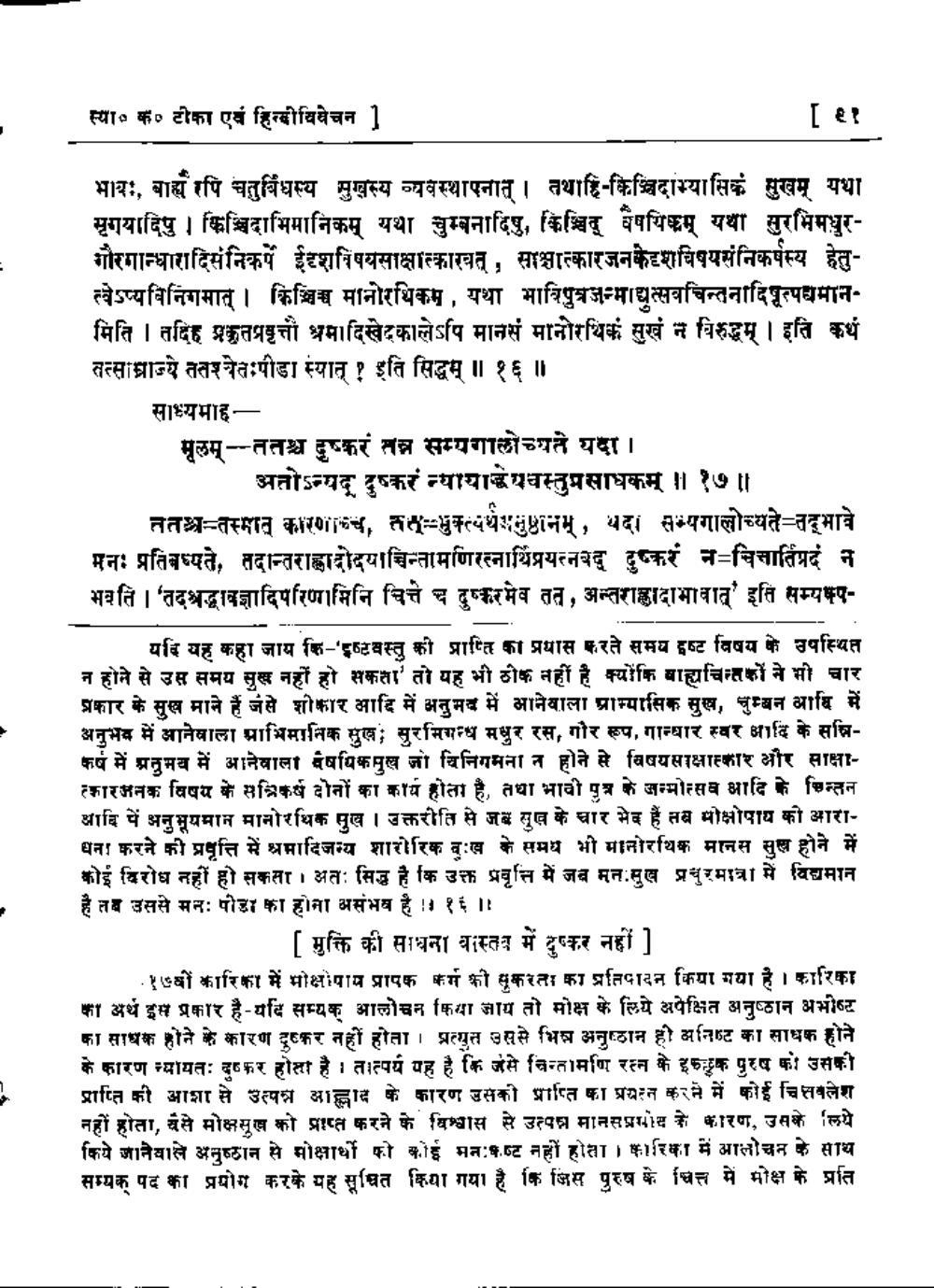________________
स्या का टीका एवं हिन्दीविवेचन ]
[
.
भाषः, बाह्य रपि चतुर्विधस्य मुखस्य व्यवस्थापनात् । तथाहि-किञ्चिदाभ्यासिकं सुखम् यथा मृगयादिषु । किश्चिदाभिमानिकम् यथा चुम्बनादिषु, किश्चित् वैषयिकम् यथा सुरभिमधुरगौरगान्धारादिसंनिक ईदृशविषयसाक्षात्कारबत , साक्षात्कारजनकेशविषयसंनिकर्षस्य हेतुत्वेऽप्यविनिगमात् । किश्चिञ्च मानोरथिकम , यथा भाविपुत्रजन्माधुत्सवचिन्तनादितत्पद्यमानमिति । तदिह प्रकृतप्रवृत्ती श्रमादिखेदकालेऽपि मानसं मानोरथिकं सुखं न विरुद्धम् । इति कथं तत्साम्राज्ये ततश्वेत पीडा स्यात् ? इति सिद्धम् ।। १६ ।।
साध्यमाहमूलम् --ततश्च दुष्करं सन्न सम्यगालोच्यते यदा।
___अतोऽन्यद दुष्करं न्यायावेयवस्तुप्रसाधकम् ॥ १७ ॥ ततश्च-तस्मात् कारणाच्च, तत्-भुक्त्यर्थमनुष्ठानम् , यदा सभ्यगालोच्यते तद्भावे मनः प्रतिवध्यते, सदान्तराहादोदयाचिन्तामणिरत्नार्थिप्रयत्नवद् दुष्करं न=चिसार्तिप्रदं न भवति । 'तदश्रद्धावज्ञादिपरिणामिनि चित्ते च दुष्करमेव तत , अन्तरालादाभावात्' इति सम्यक्प
यदि यह कहा जाय कि-'इष्टवस्तु की प्राप्ति का प्रयास करते समय इष्ट विषय के उपस्थित न होने से उस समय सुख नहीं हो सकता' तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि बाह्यचिन्तकों ने भी चार प्रकार के सुख माने हैं जैसे शीकार आदि में अनुभव में आनेवाला प्राम्यासिक सुख, चुम्बन आधि में अनुभव में आनेवाला माभिमानिक सुख; सुरमिगन्ध मधुर रस, गौर रूप, गान्धार स्वर आदि के सन्निकर्ष में प्रतुमय में आनेवाला वैषयिक मुख जो चिनिगमना न होने से विषयसाक्षात्कार और साक्षाकारजनक विषय के सत्रिकर्ष दोनों का कार्य होता है, तथा भावी पुत्र के जन्मोत्सव आदि के भिन्तन आदि में अनुभूयमान मानोरथिक सुख । उक्तरोति से जब सुख के चार भेव हैं सब मोक्षोपाय को आराधना करने की प्रवृत्ति में श्रमादिजन्य शारीरिक वुःख के समय भी मानोरथिक मानस सुख होने में कोई विरोध नहीं हो सकता। अतः सिद्ध है कि उक्त प्रवृत्ति में जब मनःसुख प्रचुरमात्रा में विद्यमान है तब उससे मनः पीडा का होना असंभव है ।। १६ ॥
[मुक्ति की साधना वास्तव में दुष्कर नहीं ] . १७वों कारिका में मोक्षोपाय प्रापक कर्म की सुकरता का प्रतिपादन किया गया है । कारिका का अर्थ इस प्रकार है-यदि सम्यक् आलोचन किया जाय तो मोक्ष के लिये अपेक्षित अनुष्ठान अभीष्ट का साधक होने के कारण दुष्कर नहीं होता। प्रत्युत्त उससे भिन्न अनुष्ठान ही अनिष्ट का साधक होने के कारण न्यायतः दुष्कर होता है । तात्पर्य यह है कि जैसे चिन्तामणि रत्न के इफक पुरुष को उसकी प्राप्ति की आशा से उत्पन्न आल्हाद के कारण उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करने में कोई चित्तक्लेश नहीं होता, वैसे मोक्षसुख को प्राप्त करने के विश्वास से उत्पन्न मानसप्रमोद के कारण, उसके लिये किये जानेवाले अनुष्ठान से मोक्षार्थी को कोई मनःपष्ट नहीं होता। कोरिका में आलोचन के साथ सम्यक् पद का प्रयोग करके यह सूचित किया गया है कि जिस पुरुष के चित्त में मोक्ष के प्रति