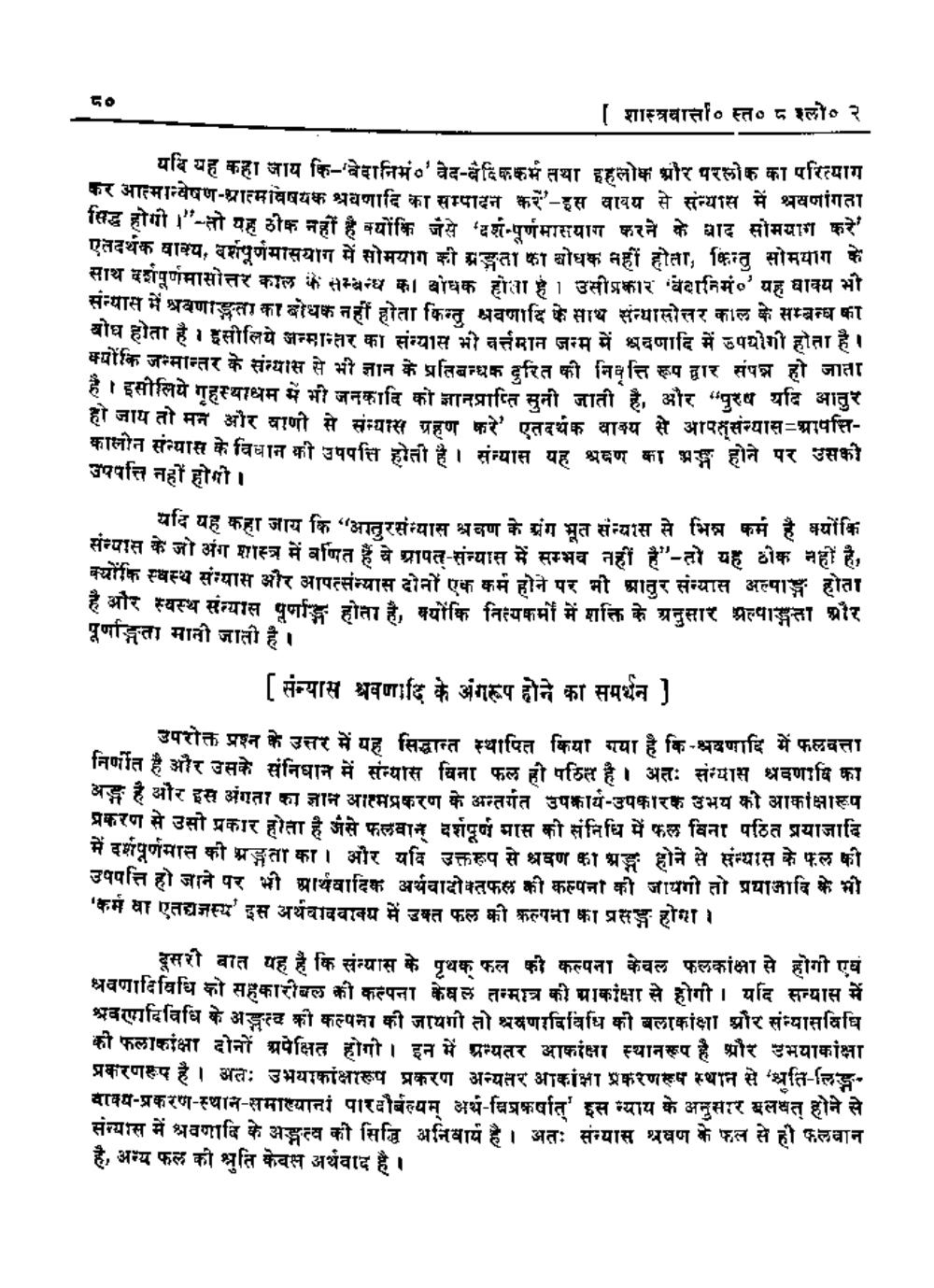________________
[ शास्त्रवा० स्त० ८ श्लो० २
यदि यह कहा जाय कि-'वेदानिमं०' वेद-वैदिककर्म तथा इहलोक और परलोक का परित्याग कर आत्मान्वेषण-प्रात्मविषयक श्रवणादिका सम्पादन करें-इस वावय से संन्यास में श्रवणांगता सिद्ध होगी।"-तो यह ठीक नहीं है क्योंकि जैसे 'दर्श-पूर्णमासयाग करने के बाद सोमयाग करे एतदर्थक वाक्य, वर्शपूर्णमासयाग में सोमयाग की अङ्गता का बोधक नहीं होता, किन्तु सोमयाग के साथ दशंपूर्णमासोत्तर काल के सम्बन्धका बाधक होता है। उसीप्रकार विनिमं०' यह बाक्य भी सन्यास में श्रवणाडता का बोधक नहीं होता किन्त श्रवणादि के साथ संन्यासोत्तर काल के सम्बन्ध का बोध होता है। इसीलिये जन्मान्तर का संन्यास भी वर्तमान जन्म में श्रवणादि में उपयोगी होता है। क्योकि जन्मान्तर के संन्यास से भी ज्ञान के प्रतिबन्धक दुरित की निवृत्ति रूप द्वार संपन्न हो जाता हैं । इसीलिये गृहस्थाश्रम में भी जनकादि को ज्ञानप्राप्ति सुनी जाती है, और "पुरष यदि आतुर हो जाय तो मन और वाणी से संन्यास ग्रहण करे एतदर्थक वाक्य से आपसंन्यास-आपत्तिकालीन संन्यास के विधान की उपपत्ति होती है। संन्यास यह श्रषण का असा होने पर उसको उपपत्ति नहीं होगी।
यदि यह कहा जाय कि "आतुरसंन्यास श्रवण के अंग भूत संन्यास से भिन्न फर्म है क्योंकि संन्यास के जो अंग शास्त्र में वर्णित हैं ये प्रापत-संन्यास में सम्भव नहीं है"-तो यह ठीक नहीं है। क्योंकि स्वस्थ संन्यास और आपत्संन्यास दोनों एक कर्म होने पर भी आतुर संन्यास अल्पाङ्ग होता है और स्वस्थ संन्यास पूर्णाङ्ग होता है, क्योंकि नित्यकर्मों में शक्ति के अनुसार अल्पाङ्गता और पूर्णाङ्गता मानी जाती है।
[संन्यास श्रवणादि के अंगरूप होने का समर्थन ] उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में यह सिद्धान्त स्थापित किया गया है कि-श्रवणादि में फलवत्ता निर्णीत है और उसके संनिधान में संन्यास विना फल हो पठित है। अतः संन्यास श्रवणादि का अङ्ग है और इस अंगता का ज्ञान आत्मप्रकरण के अन्तर्गत उपकार्य-उपकारक उभय को आकांक्षारूप प्रकरण से उसी प्रकार होता है जैसे फलवान दर्शपूर्ण मास की संनिधि में फल विना पठित प्रयाजादि में दर्शपूर्णमास की अङ्गता का। और यदि उक्तरुप से श्रवण का अङ्ग होने से संन्यास के फल की उपपत्ति हो जाने पर भी प्रार्थवादिक अर्थवादोक्तफल की कल्पना की जायगी तो प्रयाजादि के भी 'कर्म वा एतद्यजस्य' इस अर्थवाववाक्य में उक्त फल की कल्पना का प्रसङ्ग होगा।
दूसरी बात यह है कि संन्यास के पृथक् फल की कल्पना केवल फलकांक्षा से होगी एवं श्रवणादिविधि को सहकारीबल की कल्पना केवल तन्मात्र की प्राकांक्षा से होगी। यदि सन्यास में श्रवणादिविधि के अङ्गत्व की कल्पना की जायगी तो श्रवणादिविधि की बलाकांक्षा और संन्यासविधि की फलाकांक्षा दोनों अपेक्षित होगी। इन में अन्यतर आफांक्षा स्थानरूप है और उभयाकांक्षा प्रकरणरूप है। अत: उभयाकांक्षारूप प्रकरण अन्यतर आकांक्षा प्रकरणरूप स्थान से 'श्रुति-लिङ्गवाक्य-प्रकरण-स्थान-समाल्यानां पारदौर्बल्यम् अर्थ-चित्रकर्षात' इस न्याय के अनुसार बलथत् होने से संन्यास में श्रवणादि के अङ्गत्व की सिद्धि अनिवार्य है। अतः संन्यास श्रवण के फल से ही फलवान है, अन्य फल की श्रुति केवल अर्थवाद है।