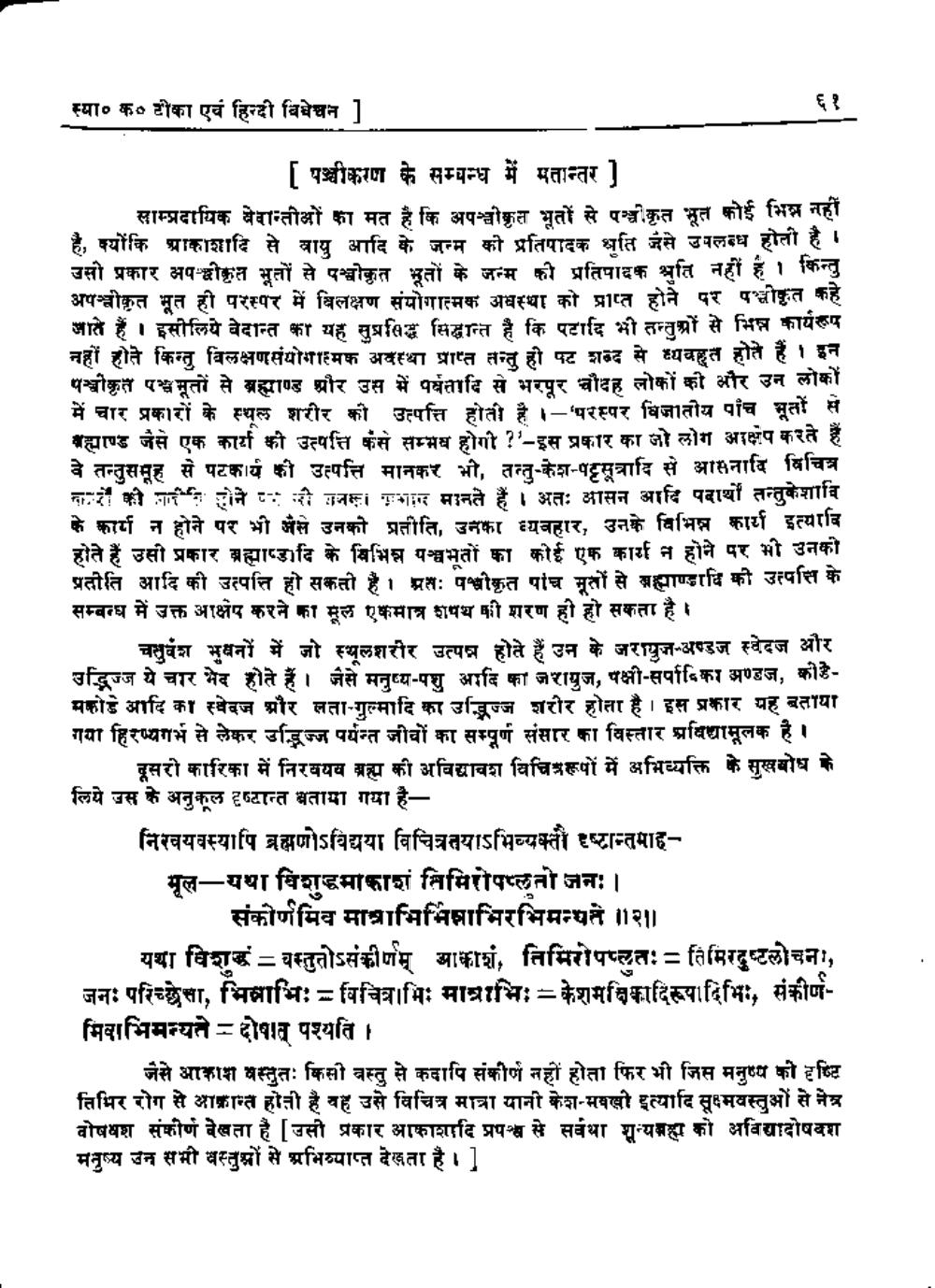________________
स्या० का टीका एवं हिन्दी विधेचन ]
पिनी
[पञ्चीकरण के सम्बन्ध में मतान्तर ] __ साम्प्रदायिक वेदान्तीओं का मत है कि अपञ्चीकृत भूतों से पञ्चीकृत भूत कोई भिन्न नहीं है, क्योंकि प्राकाशादि से वायु आदि के जन्म को प्रतिपादक श्रति जैसे उपलब्ध होती है । उसी प्रकार अप-धीकृत भूतों से पञ्चोकृत भूतों के जन्म की प्रतिपादक श्रुति नहीं है। किन्तु अपञ्चीकृत भूत ही परस्पर में विलक्षण संयोगात्मक अवस्था को प्राप्त होने पर पक्षीकृत कह आते हैं । इसीलिये वेदान्त का यह सुप्रसिद्ध सिद्धान्त है कि पटादि भी तन्तुओं से भिन्न कार्यरूप नहीं होते किन्तु विलक्षणसंयोगात्मक अवस्था प्राप्त तन्तु ही पट शब्द से ध्यवहत होते हैं । इन पश्चीकृत पश्च मूतों से ब्रह्माण्ड और उस में पर्वतादि से भरपूर चौदह लोकों की और उन लोकों में चार प्रकारों के स्थल शरीर की उत्पत्ति होती है।-'परस्पर विजातीय पांच भूतों से ब्रह्माण्ड जैसे एक कार्य की उत्पत्ति कसे सम्मव होगी ?'-इस प्रकार का जो लोग आक्षेप करते हैं वे तन्तुसमूह से पटकार्य की उत्पत्ति मानकर भी, तन्तु-केश-पट्टसूत्रादि से आसनावि विचित्र तारी की गई होने से उनका गभार मानते हैं । अतः आसन आदि पदार्थों तन्तुकेशावि के कार्ग न होने पर भी असे उनको प्रतीति, उनका व्यवहार, उनके विभिन्न कार्ग इत्यादि होते हैं उसी प्रकार ब्रह्माण्डादि के विभिन्न पश्वभतों का कोई एक कार्ग न होने पर भी उनको प्रतीति आदि की उत्पत्ति हो सकती है। प्रतः पश्चीकृत पांच मूतों से ब्रह्माण्डादि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उक्त आक्षेप करने का मूल एकमात्र शपथ की शरण ही हो सकता है।
चतुवंश भवनों में जो स्थूलशरीर उत्पन्न होते हैं उन के जरायुज-अण्डज स्वेदज और उद्धिज्ज ये चार भेद होते हैं। जैसे मनुष्य-पशु आदि का जरायुज, पक्षी-सादिका अण्डज, कोहमकोडे आदि का स्वेवज और लता-गुल्मादि का उबिज्ज शरीर होता है। इस प्रकार यह बताया गया हिरण्यगर्भ से लेकर उद्भिज्ज पर्यन्त जीवों का सम्पूर्ण संसार का विस्तार अविद्यामूलक है।
दूसरी कारिका में निरवयव ब्रह्म की अविद्यावश विचित्ररूपों में अभिव्यक्ति के सुखबोध के लिये उस के अनुकूल दृष्टान्त बताया गया है
निरवयवस्यापि ब्रह्मणोऽविद्यया विचित्रतयाऽभिव्यक्ती दृष्टान्तमाहमूल-यथा विशुद्धमाकाशं तिमिरोपालतो जनः ।
संकोणमिव मात्राभिभिन्नाभिरभिमन्यते ॥२॥ यथा विशुद्ध = वस्तुतोऽसंकीर्णम् आकाश, तिमिरोपप्लुतः = तिमिरदुष्टलोचना, जनः परिच्छेसा, भिन्नाभिः = विचित्राभिः मात्राभिः =केशमक्षिकादिरूयादिभिः, संकीर्णमिवाभिमन्यते- दोषात् पश्यति ।
जैसे आकाश वस्तुतः किसी वस्तु से कदापि संकीर्ण नहीं होता फिर भी जिस मनुष्य को दृष्टि तिभिर रोग से आक्रान्त होती है वह उसे विचित्र मात्रा यानी केश-मक्खी इत्यादि सूक्ष्मवस्तुओं से नेत्र वोषवश संकीर्ण वेखता है [उसी प्रकार आकाशादि प्रपश्व से सर्वथा शून्यबह्म को अविद्यादोषवश मनुष्य उन सभी वस्तुनों से अभिव्याप्त देखता है।]