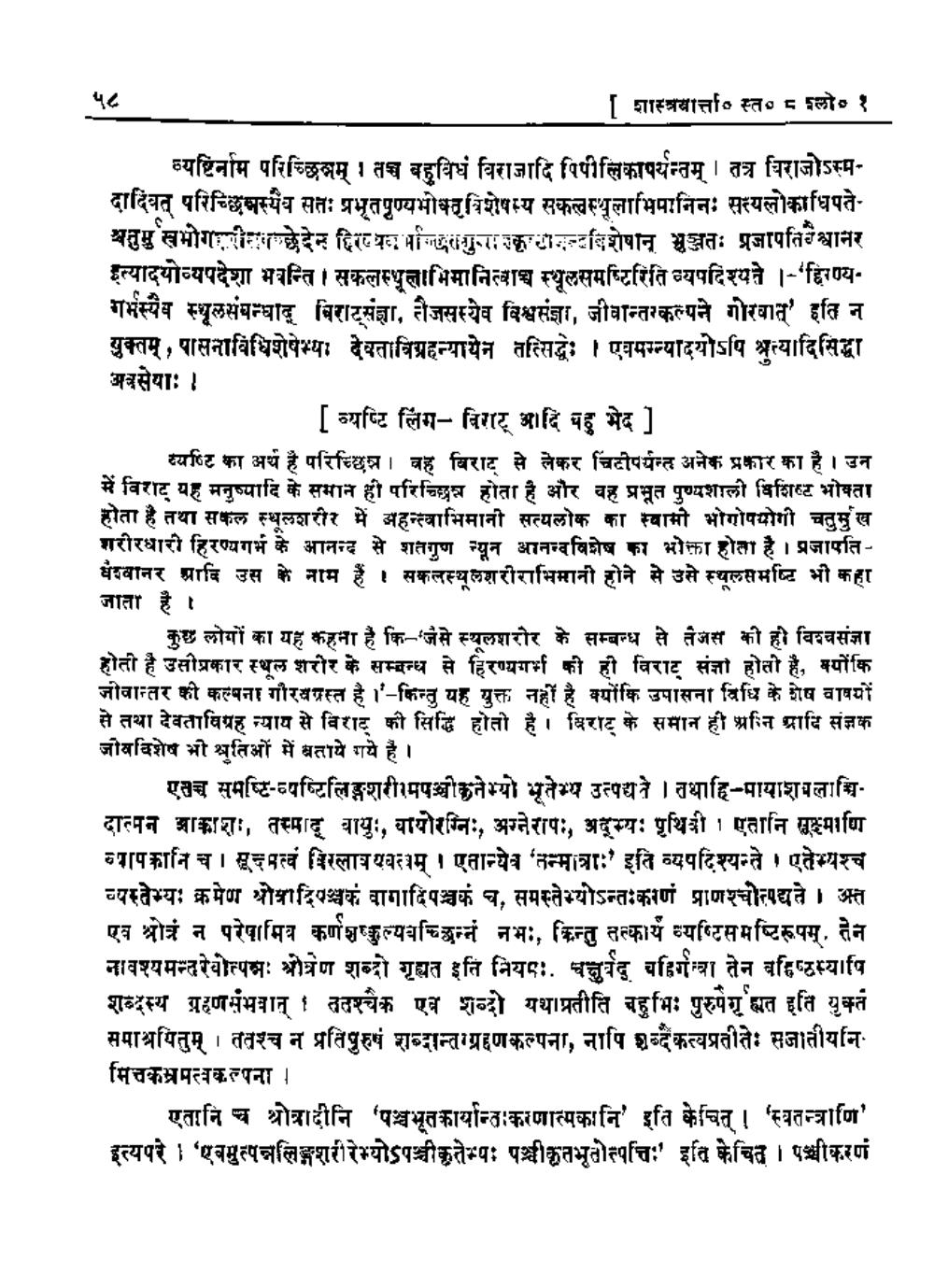________________
५८
[ शास्त्रया स्त० - लो०१
व्यष्टिर्नाम परिच्छिमम । तच्च बहुविधं विराजादि पिपीलिकापर्यन्तम् । तत्र विराजोऽस्मदादिवत् परिच्छिमस्यैव सतः प्रभृतपुण्यभोक्तविशेषम्य सकवस्थुलाभिमानिनः सत्यलोकाधिपते. चतुमुखभोगालीनाल्छेदेन दिल्या निवासस्कृतानन्दविशेषान भुञ्जतः प्रजापतिश्वानर इत्यादयोव्यपदेशा भवन्ति । सकलस्थुलाभिमानित्याच स्थलसमष्टिरिति व्यपदिश्यते ।-'हिरण्यगर्भस्यैव स्थूलसंपन्धाद् विरासंज्ञा, तैजसस्येव विश्वसंज्ञा, जीवान्तरकल्पने गोरवात्' इति न युक्तम् , पासनाविधिशेषेभ्या देवताविग्रहन्यायेन तत्सिद्धेः । एवमग्न्यादयोऽपि श्रुत्यादिसिद्धा अबसेयाः ।
[ व्यष्टि लिंग-विराट् आदि यह भेद ] व्यष्टि का अर्थ है परिच्छिन्न। वह विराट से लेकर चिटीपर्यन्त अनेक प्रकार का है । उन में विराट् यह मनुष्यादि के समान ही परिच्छिन्न होता है और वह प्रभूत पुण्यशाली विशिष्ट भोक्ता होता है तथा सकल स्थूलशरीर में अहन्त्वाभिमानी सत्यलोक का स्वामी भोगोपयोगी चतुर्मुख शरीरधारी हिरण्यगर्भ के आनन्द से शतगुण न्यून आनन्द विशेष का भोक्ता होता है । प्रजापतिधश्वानर प्रावि उस के नाम हैं । सकलस्थूलशरीराभिमानी होने से उसे स्थलसमष्टि भी कहा जाता है।
कुछ लोगों का यह कहना है कि-'जैसे स्थलशरोर के सम्बन्ध से तेजस की हो विश्वसंज्ञा होती है उसीप्रकार स्थूल शरीर के सम्बन्ध से हिरण्यगर्भ की ही विराट् संज्ञो होती है, क्योंकि जोवान्तर की कल्पना गौरवग्रस्त है। किन्तु यह युक्त नहीं है क्योंकि उपासना विधि के शेष वाषयों से तथा देवताविग्रह न्याय से विराट की सिद्धि होती है। विराट के समान ही अग्नि प्रादि संज्ञक जीवविशेष भी श्रुतिओं में बताये गये है।
एसच समष्टि-पष्टिलिङ्गशरीरमपश्चीकनेभ्यो भूतेभ्य उत्पद्यते । तथाहि-मायाशबलाश्चिदात्मन आकाशः, तस्माद् वायुः, यायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी । एतानि सूक्ष्माणि यापकानि च । सूक्ष्मत्वं पिरलाव यवत्वम् । एतान्येव तन्मात्राः' इति व्यपदिश्यन्ते । एतेभ्यश्च व्यस्तेभ्यः क्रमेण श्रोत्रादिपञ्चकं वागादिपञ्चकं च, समस्तेभ्योऽन्तःकरणं प्राणश्चोत्पद्यते । अत एव श्रोत्रं न परेषामित्र कर्णशष्कुल्यवच्छिन्नं नमः, किन्तु तत्कार्य व्यष्टिसमष्टिरूपम् , तेन नावश्यमन्तरेयोत्पन्नः श्रोत्रेण शब्दो गृह्यत इति नियमः चक्षुर्वद् हिर्गत्रा तेन बहिष्ठम्यापि शब्दस्य ग्रहणसंभवात् । ततश्चैक एवं शब्दो यथाप्रतीति बहुभिः पुरुपेगृह्यत इति युक्त समाश्रयितुम् । ततश्च न प्रतिपुरुषं शब्दान्त ग्रहणकल्पना, नापि शब्दै कत्यप्रतीते सजातीयनिमिचकनमत्वकल्पना ।
। एतानि च श्रोत्रादीनि 'पञ्चभृतकार्यान्तःकरणात्मकानि' इति केचित् । 'स्वतन्त्राणि' इत्यपरे । एवमुत्पन्नलिङ्गशरीरेभ्योऽपञ्चीकृतेभ्यः पञ्चीकृतभृतोत्पचिः' इति केचित । पश्चीकरणं