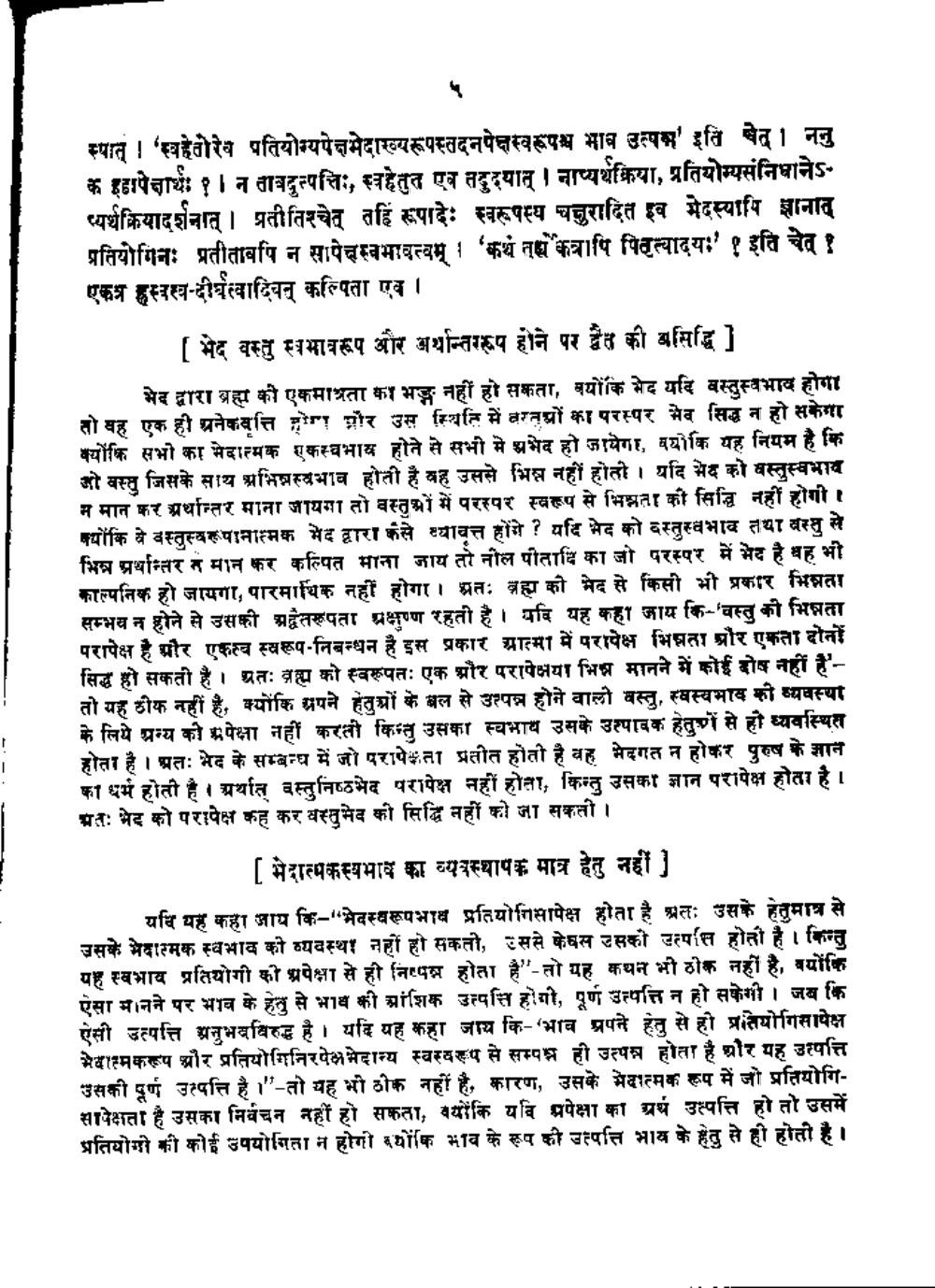________________
1
I
स्पात् | 'स्वहेतोरेव प्रतियोग्यपेक्ष मेदाख्यरूपस्तदनपेक्ष स्वरूपश्च भाव उत्पन्न' इति वेद । ननु कापेतार्थः ९ । न तावदुत्पत्तिः स्वहेतुत एव तदुदयात् । नाप्यर्थक्रिया, प्रतियोग्यसंनिधानेऽव्यर्थक्रियादर्शनात् । प्रतीतिश्चेत् तहिं रूपादेः स्वरूपस्य चक्षुरादित इव मेदस्यापि ज्ञानाद प्रतियोगिनः प्रतीतावपि न सापेक्ष स्वभावत्वम् । 'कथं त कत्रापि पितृत्वादयः' १ इति चेत् १ ear ह्रस्व-दीर्घत्वादिवत् कल्पिता एव ।
[ भेद वस्तु स्वभावरूप और अर्थान्तररूप होने पर द्वैत की सिद्धि ]
भेद द्वारा ब्रह्म की एकमात्रता का भङ्ग नहीं हो सकता, क्योंकि भेद यदि वस्तुस्वभाव होगा तो वह एक ही अनेकवृत्ति हो और उस स्थिति में वस्तुओं का परस्पर मेव सिद्ध न हो सकेगा क्योंकि सभी का मेदात्मक एकस्वभाव होते से सभी में अभेद हो जायेगा, क्योंकि यह नियम है कि ओ वस्तु जिसके साथ अभिन्नस्वभाव होती है वह उससे भिन्न नहीं होती । यदि भेद को वस्तुस्वभाव म मान कर अर्थान्तर माना जायगा तो वस्तुनों में परस्पर स्वरूप से भिन्नता की सिद्धि नहीं होगी । क्योंकि वे वस्तुस्वरूपानात्मक भेद द्वारा कैले व्यावृत्त होंगे ? यदि भेद को वस्तुस्वभाव तथा वस्तु से भी fe अर्थान्तर में मान कर कल्पित माना जाय तो नील पीतादि का जो परस्पर में भेद है वह काल्पनिक हो जायगा, पारमार्थिक नहीं होगा । अतः ब्रह्म को भेद से किसी भी प्रकार भिन्नता सम्भव न होने से उसकी अद्वैतरूपता प्रक्षुण्ण रहती है। यदि यह कहा जाय कि 'वस्तु की भिन्नता परापेक्ष है और एकरच स्वरूप-निबन्धन है इस प्रकार आत्मा में परापेक्ष भिन्नता और एकता दोनों सिद्ध हो सकती है। ग्रतः व्रह्म को स्वरूपतः एक और परापेक्षया भिन्न मानने में कोई दोष नहीं है'तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि अपने हेतुत्रों के बल से उत्पन्न होने वाली स्वस्वभाव की व्यवस्था वस्तु, के लिये अन्य की अपेक्षा नहीं करती किन्तु उसका स्वभाव उसके उत्पादक हेतुकों से हो व्यवस्थित होता है। अतः भेद के सम्बन्ध में जो परापेक्षता प्रतीत होती है वह मेदगत न होकर पुरुष के ज्ञान का धर्म होती है । अर्थात् वस्तुनिष्ठभेद परापेक्ष नहीं होता, किन्तु उसका ज्ञान परापेक्ष होता है । अतः भेद को परापेक्ष कह कर वस्तुभेद की सिद्धि नहीं की जा सकती ।
[ भेदात्मकभाव का व्यवस्थापक मात्र हेतु नहीं ]
afar यह कहा जाय कि- "मेवस्वरूपभाव प्रतियोगिसापेक्ष होता है अतः उसके हेतुमात्र से उसके भेदात्मक स्वभाव की व्यवस्था नहीं हो सकती, उससे केवल उसको उत्पति होती है । किन्तु यह स्वभाव प्रतियोगी की अपेक्षा से ही निष्पन्न होता है" तो यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर भाव के हेतु से भाव की प्रांशिक उत्पत्ति होगी, पूर्ण उत्पत्ति न हो सकेगी। जब कि ऐसी उत्पत्ति अनुभवविरुद्ध है। यदि यह कहा जाय कि 'भाव प्रपने हेतु से ही प्रतियोगिसापेक्ष
arre और प्रतियोगिनिरपेक्ष मेदान्य स्वस्वरूप से सम्पन्न ही उत्पन्न होता है और यह उत्पत्ति उसकी पूर्ण उत्पत्ति है ।" तो यह भी ठीक नहीं है, कारण, उसके मेदात्मक रूप में जो प्रतियोगिसापेक्षता है उसका निर्वाचन नहीं हो सकता, क्योंकि यदि अपेक्षा का अर्थ उत्पत्ति हो तो उसमें प्रतियोगी की कोई उपयोगिता न होगी क्योंकि भाव के रूप की उत्पत्ति भाव के हेतु से ही होती है।