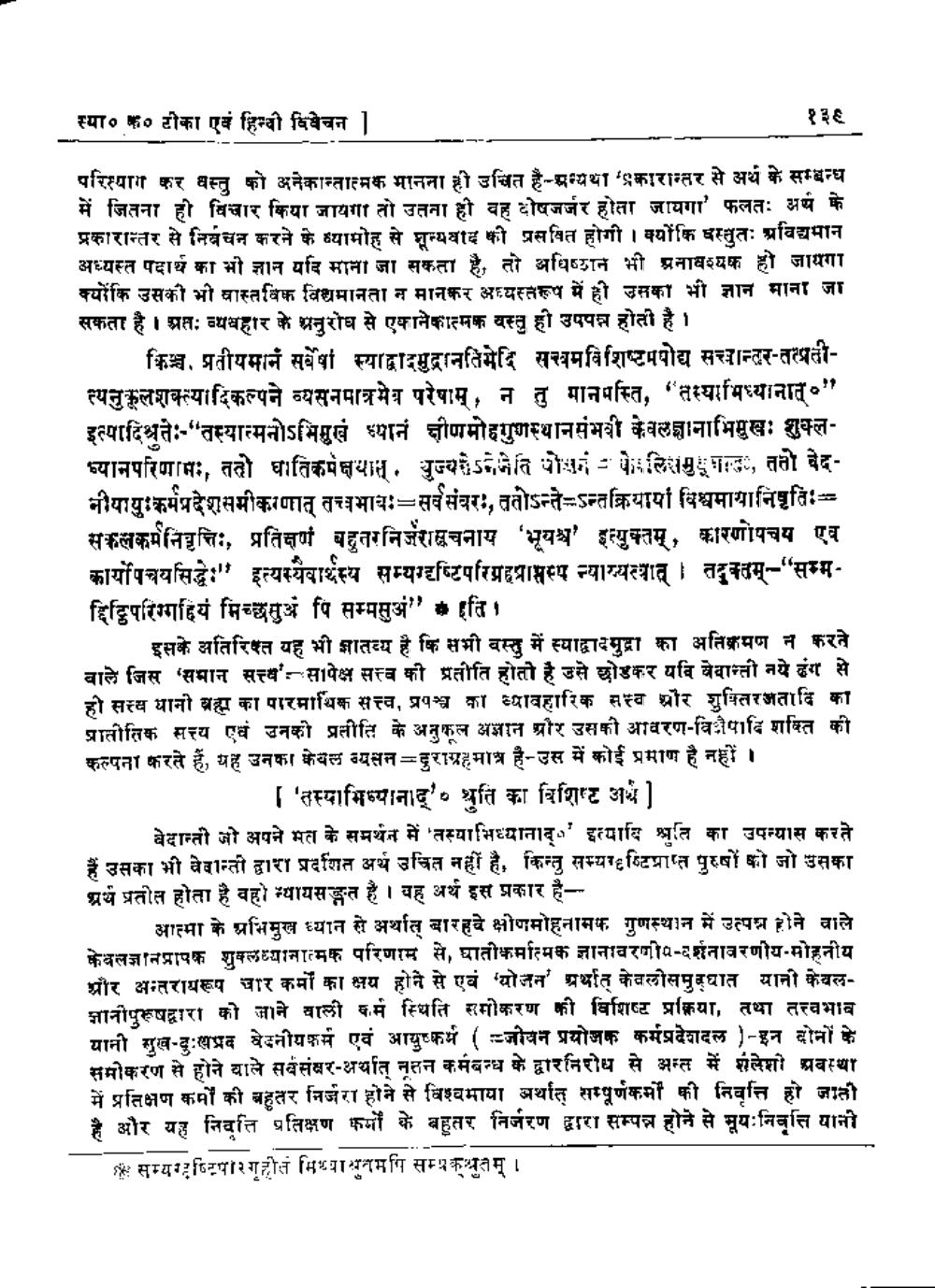________________
१३६
स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन |
परित्याग कर वस्तु को अनेकान्तात्मक मानना ही उचित है अन्यथा प्रकारान्तर से अर्थ के सम्बन्ध में जितना ही विचार किया जायगा तो उतना ही वह दोषजर्जर होता जायेगा' फलतः अर्थ के प्रकारान्तर से निर्वाचन करने के व्यामोह से शून्यवाद की प्रसवित होगी। क्योंकि वस्तुतः श्रविद्यमान अध्यस्त पदार्थ का भी ज्ञान यदि माना जा सकता है, तो अधिष्ठान भी अनावश्यक हो जायगा क्योंकि उसकी भी वास्तविक विद्यमानता न मानकर अध्यस्तरूप में ही उसका भी ज्ञान माना जा सकता है । अतः व्यवहार के अनुरोध से एकानेकात्मक वस्तु ही उपपन्न होती है ।
किश्च प्रतीयमानं सर्वेषां स्याद्वादमुद्रानतिमेदि सत्रम विशिष्टमपोद्य सच्चान्दर-तत्प्रतीत्यनुकूलशक्त्यादिकल्पने व्यसनमात्रमेव परेषाम्, न तु मानवस्ति, "तस्याभिध्यानात् ०" इत्यादिश्रुते:-"तस्यात्मनोऽभिमुखं ध्यानं क्षीणमोहगुणस्थान संभवी केवलज्ञानाभिमुखः शुक्लध्यानपरिणामः ततो घातिकपेक्षयात्. युज्यतेऽनेनेति पो फेलिमु ततो वेदनायुःकर्मप्रदेशसमीकरणात् तच्चभावः = सर्व संवरः, ततोऽन्ते ऽन्तक्रियायां विश्वमायानिषृतिः = सकलकर्म निवृत्तिः, प्रतिक्षणं बहुतरनिर्जरासुचनाय 'भूयश्र' इत्युक्तम्, कारणोपचय एव कार्योपचयसिद्धेः” इत्यस्यैवार्थस्य सम्यग्दृष्टिपरिग्रहप्राशस्य न्याय्यत्यात् । तदुक्तम्- "सम्म - दिपरिगहियं मिच्छतु पि सम्मसुअं" इति ।
इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि सभी वस्तु में स्याद्वादमुद्रा का अतिक्रमण न करते वाले जिस 'समान सत्त्व' सापेक्ष सत्त्व की प्रतीति होती है उसे छोडकर यदि वेदान्ती नये ढंग से ही सत्य यानी ब्रह्म का पारमार्थिक सत्त्व, प्रपश्व का व्यावहारिक सत्व और शुक्तिरजतादि का प्रातीतिक सत्य एवं उनकी प्रतीति के अनुकूल अज्ञान श्रौर उसकी आवरण-विक्षेपादि शक्ति की कल्पना करते हैं, यह उनका केवल व्यसन दुराग्रहमात्र है उस में कोई प्रमाण है नहीं ।
[ 'तस्याभिध्यानाद्' श्रुति का विशिष्ट अर्थ ]
०
वेदान्ती जो अपने मत के समर्थन में 'तस्याभिध्यानाद्' इत्यादि श्रुति का उपन्यास करते हैं उसका भी वेदान्ती द्वारा प्रदर्शित अर्थ उचित नहीं है, किन्तु सम्यग्दष्टिप्राप्त पुरुषों को जो उसका श्रर्थ प्रतीत होता है वही न्यायसङ्गत है । यह अर्थ इस प्रकार है
―w
आत्मा के श्रभिमुख ध्यान से अर्थात् बारहवे क्षीणमोहनामक गुणस्थान में उत्पन्न होने वाले केवलज्ञानप्रापक शुक्लध्यानात्मक परिणाम से, घातीकर्मात्मक ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय सोहनीय और अन्तरायरूप चार कर्मों का क्षय होने से एवं 'योजन' प्रर्थात् केवलसमुद्घात यानी केवलज्ञानीपुरुषद्वारा की जाने वाली कर्म स्थिति समीकरण की विशिष्ट प्रक्रिया, तथा तत्त्वभाव यानी सुख-दुःखप्रद वेदनीयकर्स एवं आयुष्कर्म ( =जीवन प्रयोजक कर्मप्रवेशदल )- इन दोनों के समीकरण से होने वाले सर्वसंबर अर्थात् नूतन कर्मबन्ध के द्वारनिरोध से अन्त में शंशी अवस्था
प्रतिक्षण कर्मों की बहुतर निर्जरा होने से विश्वमाया अर्थात् सम्पूर्णकर्मों की निवृत्ति हो जाती है और यह निवृत्ति प्रतिक्षण फर्मों के बहुतर निर्जरण द्वारा सम्पन्न होने से मूयः निवृत्ति यानी
सम्यगृष्टिपरगृहीतं मिथ्यामपि सम्प्रश्रुतम् ।