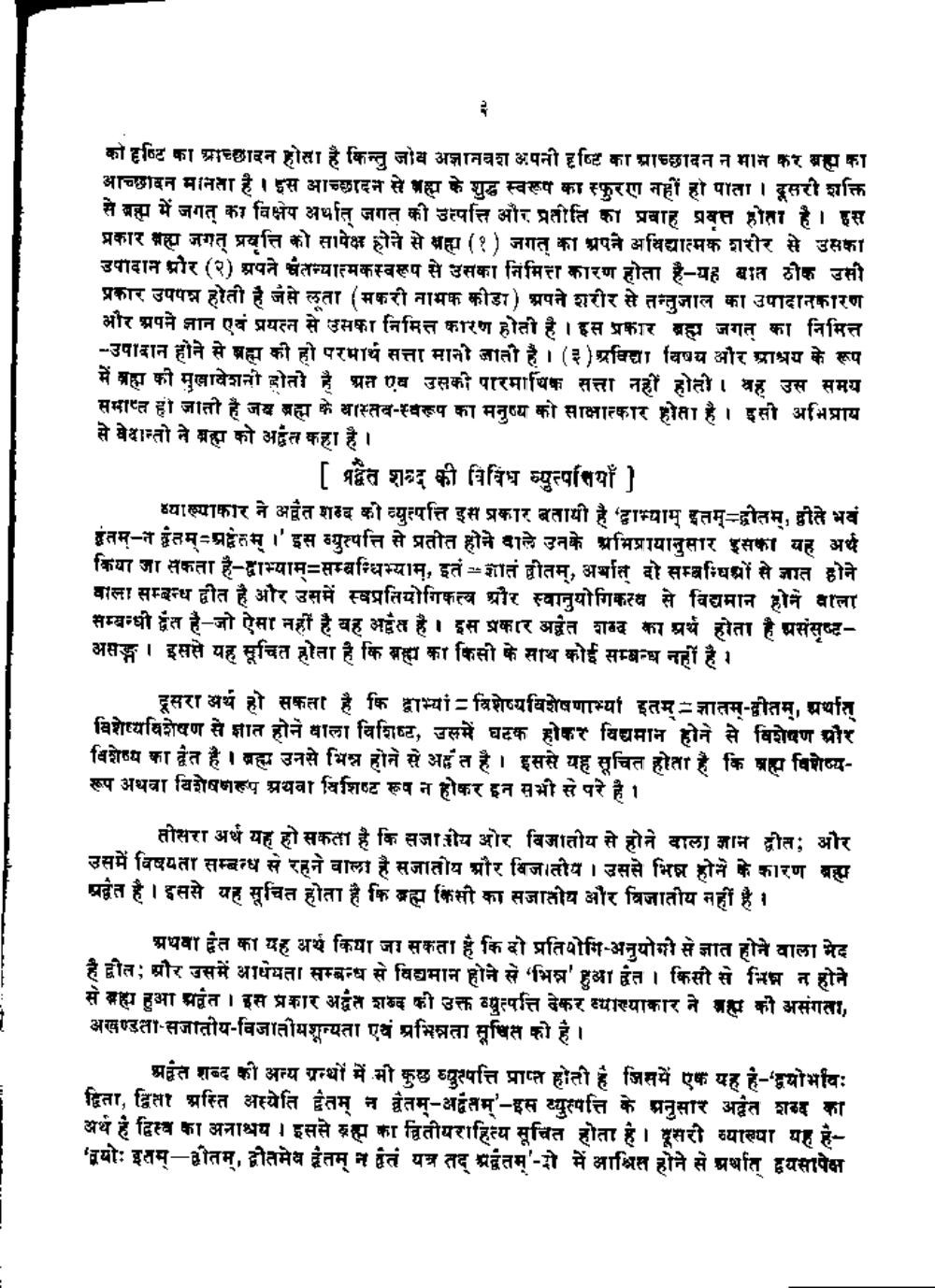________________
को दृष्टि का प्राच्छादन होता है किन्तु जोव अज्ञानवश अपनी दृष्टि का प्राच्छादन न मान कर ब्रह्म का आच्छावन मानता है। इस आच्छादन से ब्रह्म के शद्ध स्वरूप का स्फरण नहीं हो पाता। दूसरी शक्ति से ब्रह्म में जगत् का विक्षेप अर्थात् जगत की उत्पत्ति और प्रतीति का प्रवाह प्रवृत्त होता है। इस प्रकार ब्रह्म जगत् प्रवृत्ति को सापेक्ष होने से ब्रह्म (१) जगत् का अपने अविद्यात्मक शरीर से उसका उपादान और (२) अपने चतन्यात्मकस्वरूप से उसका निमित्त कारण होता है-यह बात ठीक उसी प्रकार उपपन्न होती है जैसे लता (मकरी नामक कीड़ा) अपने शरीर से तन्तुजाल का उपादानकारण
और अपने ज्ञान एवं प्रयत्न से उसका निमित्त कारण होती है । इस प्रकार ब्रह्म जगत का निमित्त -उपादान होने से ब्रह्म की हो परमार्थ सत्ता मानी जाती है। (३) अविद्या विषय और प्राश्रय के रूप में ब्रह्म की मुखावेशनी होतो है अत एव उसकी पारमाथिक सत्ता नहीं होती। वह उस समय समाप्त हो जाता है जब ब्रह्म के वास्तव-स्वरूप का मनुष्य को साक्षात्कार होता है। इसी अभिप्राय से वेदान्तो ने ब्रह्म को अद्वैत कहा है।
[ प्रद्वैत शब्द की विविध व्युत्पत्तियाँ ) ध्याख्याकार ने अवैत शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार बतायी है 'द्वाभ्याम् इतम्-द्वीतम्, द्वीते भवं हुँतम्-न तम्-प्रतम् ।' इस व्युत्पत्ति से प्रतीत होने वाले उनके अभिप्रायानुसार इसका यह अर्थ किया जा सकता है-द्वाभ्याम् सम्बन्धिभ्याम, इतं जातं द्वीतम्, अर्थात दो सम्बन्धिनों से ज्ञात होने वाला सम्बन्ध द्वीत है और उसमें स्वप्रतियोगिफत्व और स्वानुयोगिकरव से विद्यमान होने वाला सम्बन्धी द्वैत है-जो ऐसा नहीं है वह अद्वैत है। इस प्रकार अन्वत शब्द का अर्थ होता है प्रसंसृष्टअसङ्ग । इससे यह सूचित होता है कि ब्रह्म का किसी के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।
दूसरा अर्थ हो सकता है कि द्वाभ्यां - विशेष्यविशेषणाभ्यां इतम-ज्ञातम्-द्वीतम्, अर्थात् विशेष्यविशेषण से ज्ञात होने वाला विशिष्ट, उसमें घटक होकर विद्यमान होने से विशेषण और विशेष्य का द्वैत है । ब्रह्म उनसे भिन्न होने से अहं त है। इससे यह सूचित होता है कि ब्रह्म विशेष्यरूप अथवा विशेषणल्प अथवा विशिष्ट रूप न होकर इन सभी से परे है।
तीसरा अर्थ यह हो सकता है कि सजातीय ओर विजातीय से होने वाला ज्ञान द्वीत; और उसमें विषयता सम्बन्ध से रहने वाला है सजातीय और विजातीय । उससे भिन्न होने के कारण ब्रह्म प्रवत है । इससे यह सूचित होता है कि ब्रह्म किसी का सजातीय और विजातीय नहीं है।
अथवा देत का यह अर्थ किया जा सकता है कि दो प्रतियोगि-अनुयोगो से ज्ञात होने वाला भेद है द्वील; और उसमें आधेयता सम्बन्ध से विद्यमान होने से 'भिन्न' हुआ वैत । किसी से भिन्न न होने से ब्रह्म हुआ प्रत । इस प्रकार अद्वत शब्द की उक्त व्युत्पत्ति देकर व्याख्याकार ने ब्रह्मा की असंगता, अखण्डता-सजातीय-विजातीयशून्यता एवं प्रभिन्नता सूधित को है।
अद्वत शब्द की अन्य ग्रन्थों में भी कुछ व्युत्पत्ति प्राप्त होती है जिसमें एक यह है-'योर्भावः द्विता, द्विता अस्ति अस्येति द्वैतम् न चैतम्-अद्वतम्'-इस व्युत्पत्ति के अनुसार अद्वैत शब्द का अर्थ है द्विस्व का अनाथय । इससे ब्रह्म का द्वितीयराहित्य सूचित होता है। दूसरी व्याख्या यह है'तयोः इसम्-वीतम्, द्वौतमेव द्वैतम् न तं यत्र तद् अद्वैतम्'-दो में आश्रित होने से अर्थात् द्वयसापेक्ष