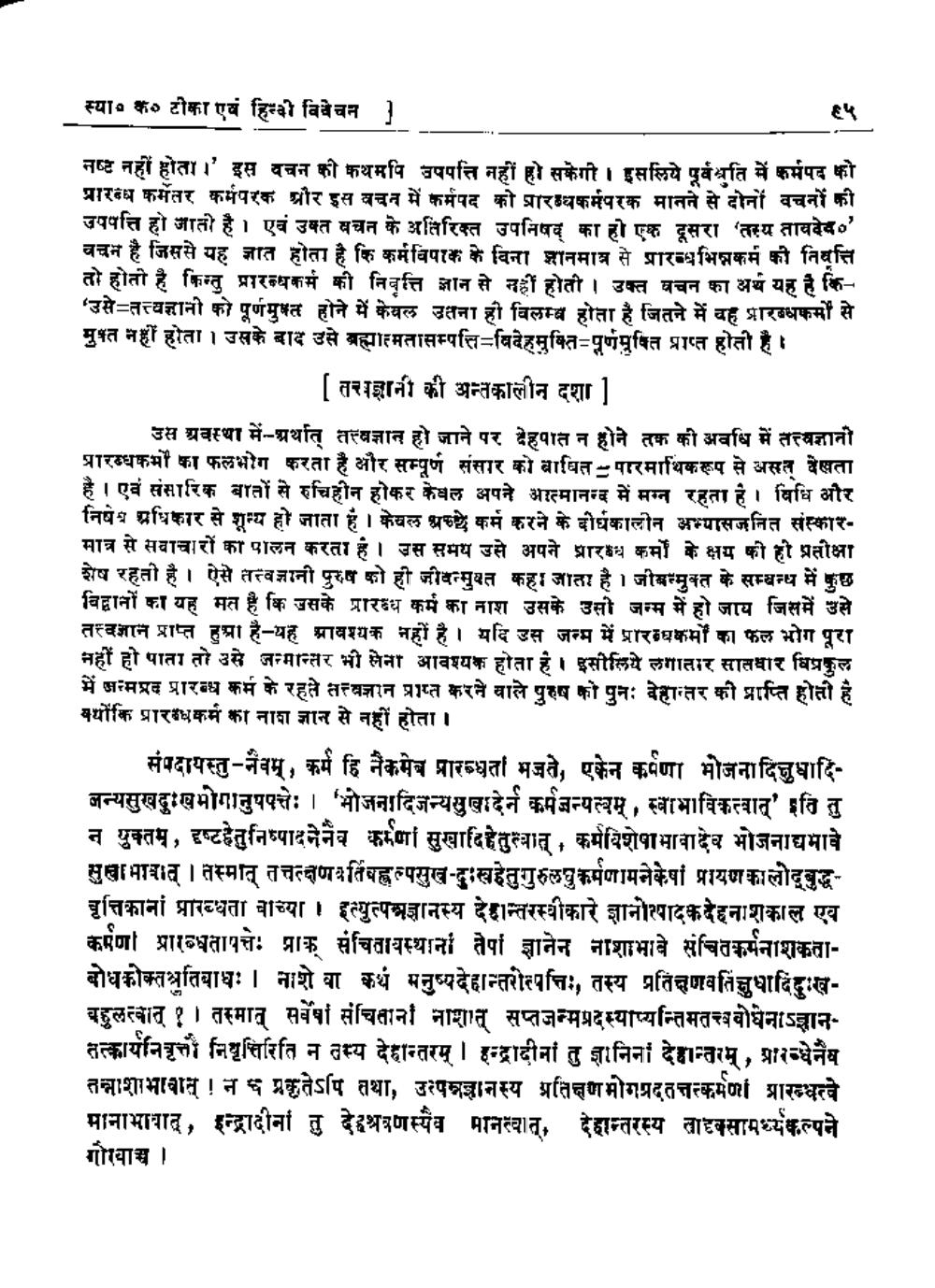________________
स्या का टीका एवं हिन्दी विवेचन ।
नष्ट नहीं होता।' इस वचन की कथमपि उपपत्ति नहीं हो सकेगी। इसलिये पूर्वश्रुति में कर्मपद को प्रारब्ध कमतर कर्मपरक और इस वचन में कर्मपद को प्रारब्धकर्मपरक मानने से दोनों वचनों की उपपत्ति हो जाती है। एवं उक्त वचन के अतिरिक्त उपनिषद का हो एक दूसरा 'तस्य तावदेव०' वचन है जिससे यह ज्ञात होता है कि कर्मविपाक के बिना ज्ञानमात्र से प्रारधभिन्नकर्म की निवृत्ति तो होती है किन्तु प्रारब्धकर्म की निवृत्ति ज्ञान से नहीं होती। उक्त बचन का अर्थ यह है कि'उसे तत्त्वज्ञानी को पूर्णमुक्त होने में केवल उतना ही विलम्ब होता है जितने में वह प्रारब्धफर्मों से मुक्त नहीं होता। उसके बाद उसे ब्रह्मात्मतासम्पत्ति-विदेहमुक्ति-पूर्णमुक्ति प्राप्त होती है।
[ तसज्ञानी की अन्तकालीन दशा ] उस अवस्था में-अर्थात् तत्त्वज्ञान हो जाने पर देहपात न होने तक की अवधि में तत्त्वज्ञानी प्रारब्धको का फलभोग करता है और सम्पूर्ण संसार को बाधित - पारमार्थिकरूप से असत् देखता है । एवं संसारिक बातों से रुचिहीन होकर केवल अपने आत्मानन्द में मग्न रहता है। विधि और निषेध अधिकार से शून्य हो जाता है । केवल अच्छे कर्म करने के दीर्घकालीन अभ्यासजनित संस्कारमात्र से सवाचारों का पालन करता है। उस समय उसे अपने प्रारब्ध कर्मों के क्षय की ही प्रतीक्षा शेष रहती है। ऐसे तत्त्वज्ञानी पुरुष को ही जीवन्मुक्त कहा जाता है । जीवन्मुक्त के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का यह मत है कि उसके प्रारब्ध कर्म का नाश उसके उसी जन्म में हो जाय जिसमें उसे तत्त्वज्ञान प्राप्त हुआ है-यह प्रावश्यक नहीं है। यदि उस जन्म में प्रारम्घकर्मों का फल भोग पूरा नहीं हो पाता तो उसे जन्मान्तर भी लेना आवश्यक होता है। इसीलिये लगातार सातवार विप्रकुल में जन्मप्रद प्रारब्ध कर्म के रहते तत्त्वज्ञान प्राप्त करने वाले पुरुष को पुनः वेहान्तर की प्राप्ति होती है क्योंकि प्रारब्धकर्म का नाश ज्ञान से नहीं होता।
संपदायस्तु-नैवम् , कर्म हि नैकमेव प्रारब्धता भजते, एकेन कर्षणा भोजनादिक्षुधादिजन्यसुखदुःखमोगानुपपत्तेः । 'भोजनादिजन्यसुखादेने कर्मजन्यत्वम् , स्वाभाविकत्वात्' इति तु न युक्तम , दृष्टहेतुनिष्पादनेनैव कर्मणां सुखादिहेतुत्वात् , कर्मविशेषाभावादेव भोजनाद्यमावे सुखाभावात् । तस्मात् तचक्षणवर्तिबह्वल्पसुख-दुःखहेतुगुरुलघुकर्मणामनेकेषां प्रायणकालोबुद्धवृत्तिकानां प्रारब्धता वाच्या । इत्युत्पत्रज्ञानस्य देहान्तरस्वीकारे ज्ञानोत्पादक देहनाशकाल एव करणा प्रारब्धतापत्तेः प्राक् संचितावस्थानां तेषा ज्ञानेन नाशाभावे संचितकर्मनाशकताबोधकोक्तश्रुतियाधः | नाशे वा कथं मनुष्यदेहान्तरोत्पत्तिः, तस्य प्रतिक्षणवतिक्षुधादिंदुःखबहुलत्वात् ? । तस्मात् सर्वेषां संचितानां नाशात् सप्तजन्मपदस्याप्यन्तिमतत्त्ववोधेनाऽज्ञानतत्कानिवृत्ती निवृत्तिरिति न तस्य देहान्तरम् । इन्द्रादीनां तु ज्ञानिनां देहान्तरम् , पारधेनैव तन्नाशाभावात् ! न १ प्रकृतेऽपि तथा, उत्पन्नवानस्य प्रतिक्षणभोगप्रदतत्तत्कर्मणां प्रारब्धत्वे मानाभावात् , इन्द्रादीनां तु देहश्रवणस्यैव मानत्वात्, देहान्तरस्य ताइक्सामध्यकल्पने गोवाच ।