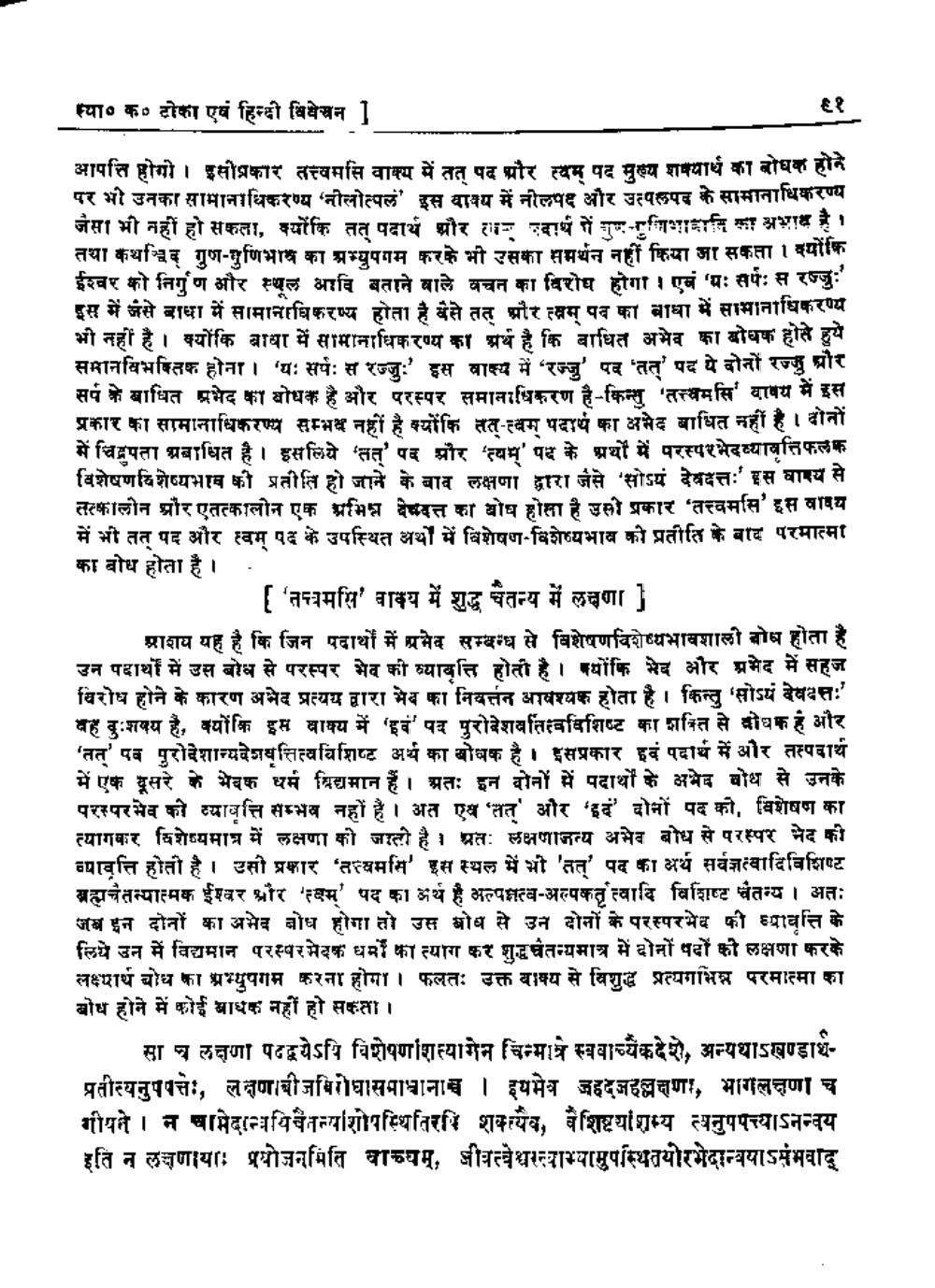________________
प्या० क० टोका एवं हिन्दी विवेचन ]
आपत्ति होगी। इसीप्रकार तत्त्वमसि वाक्य में तत् पद और स्वम् पद मुख्य शक्या का बोधक होने पर भी उनका सामानाधिकरण्य 'नीलोत्पलं' इस वाक्य में नीलपद और उत्पलपर के सामानाधिकरण्य जैसा भी नहीं हो सकला, क्योंकि तत् पदार्थ और ला जदार्थ में गुणगुलिभानानि का अभाव है। तथा कश्चिद् गुण-पुणिभाव का अभ्युपगम करके भी उसका समर्थन नहीं किया जा सकता । क्योंकि ईश्वर को निर्गुण और स्थल आदि बताने वाले वचन का विरोध होगा । एवं 'यः सर्पः स रज्जुः इस में जैसे बाधा में सामानाधिकरण्य होता है वैसे तत और त्वम् पब का बाधा में सामानाधिकरण्य भी नहीं है। क्योंकि बावा में सामानाधिकरण्य का अर्थ है कि बाधित अभेव का बोधक होते हुये समानविभक्तिक होना। 'यः सर्पः स रज्जुः' इस वाक्य में ‘रज्जु' पद 'तत्' पद ये दोनों रज्जु पोर
प्रभेद का बोधक है और परस्पर समानाधिकरण है-किन्त 'तत्त्वमसि' याषय में इस प्रकार का सामानाधिकरण्य सम्भव नहीं है क्योंकि तत-त्वम पदार्थ का अभेद बाधित नहीं है । दोनों में चिदुपता अबाधित है। इसलिये तत' पद और 'त्यम्' पद के अर्थों में परस्परभेदच्यावृत्तिफलक विशेषणविशेष्यभाव की प्रतीति हो जाने के बाद लक्षणा द्वारा जैसे 'सोऽयं देवदत्तः' इस वाश्य से तत्कालीन और एतत्कालीन एक अभिन्न देवदत्त का बोध होता है उसी प्रकार 'तत्त्वमसि' इस वाक्य में भी तत् पद और स्वम् पद के उपस्थित अर्थों में विशेषण-विशेष्यभाव को प्रतीति के बाद परमात्मा का बोध होता है। .
['तत्वमसि' वाक्य में शुद्ध चैतन्य में लक्षणा ] प्राशय यह है कि जिन पदार्थों में प्रभेद सम्बन्ध से विशेषणविशेष्यभावशाली बोष होता है उन पदार्थों में उस बोध से परस्पर भेव की व्यावृत्ति होती है। क्योंकि भेद और प्रभेद में सहज विरोध होने के कारण अभेद प्रत्यय द्वारा भेव का निवर्तन आवश्यक होता है। किन्तु 'सोऽयं देवदत्तः'
य है, क्योंकि इस वाक्य में 'पद परोदेशतित्वविशिष्ट का शक्ति से बोधक है और 'तत्' पव पुरोदेशान्यदेभवृत्तित्वविशिष्ट अर्थ का बोधक है। इसप्रकार इवं पदार्थ में और तत्पदार्थ में एक दूसरे के भेवक धर्म विद्यमान हैं। अतः इन दोनों में पदार्थों के अभेद बोथ से उनके परस्पर भेव को व्यावृत्ति सम्भव नहीं है। अत एव तत्' और 'इदं' दोनों पद को, विशेषण का त्यागकर विशेष्यमात्र में लक्षणा को जाती है। प्रतः लक्षणाजन्य अभेव बोध से परस्पर भेद की व्यावृत्ति होती है। उसी प्रकार 'तत्वमसि' इस स्थल में भी 'तत्' पद का अर्थ सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट ब्रह्मचैतन्यात्मक ईश्वर और 'स्वम्' पद का अर्थ है अल्पमत्व-अल्पकर्तृत्वादि विशिष्ट चैतन्य । अतः जब इन दोनों का अभेद बोध होगा तो उस ओष से उन दोनों के परस्परभेद की ध्यावृत्ति के लिये उन में विद्यमान परस्पर मेदक धर्मों का त्याग कर शुद्धतन्यमात्र में दोनों पदों को लक्षणा करके लक्ष्यार्थ बोध का अभ्युपगम करना होगा। फलतः उक्त वाक्य से विशुद्ध प्रत्यगभिन्न परमात्मा का बोध होने में कोई बाधक नहीं हो सकता।
सा च लक्षणा पदद्वयेऽपि विशेषणांशत्यागेन चिन्मात्रे स्ववाच्यैकदेशे, अन्यथाऽखण्डार्थप्रतीत्यनुपपत्तेः, लक्षणाची जविरोधासमाधानाच । इयमेव जहदजहल्लक्षणा, भागलक्षणा च गीयने । न चामेदान्वयिचैतन्यांशोपस्थितिरवि शक्त्यैव, वैशिष्टयां शम्य त्यनुपपत्त्याऽनन्वय इति न लक्षणायाः प्रयोजनमिति वाच्यम्, जीवत्वेश्वरन्याभ्यामुपस्थितयोरभेदान्वयाऽसंभवाद्