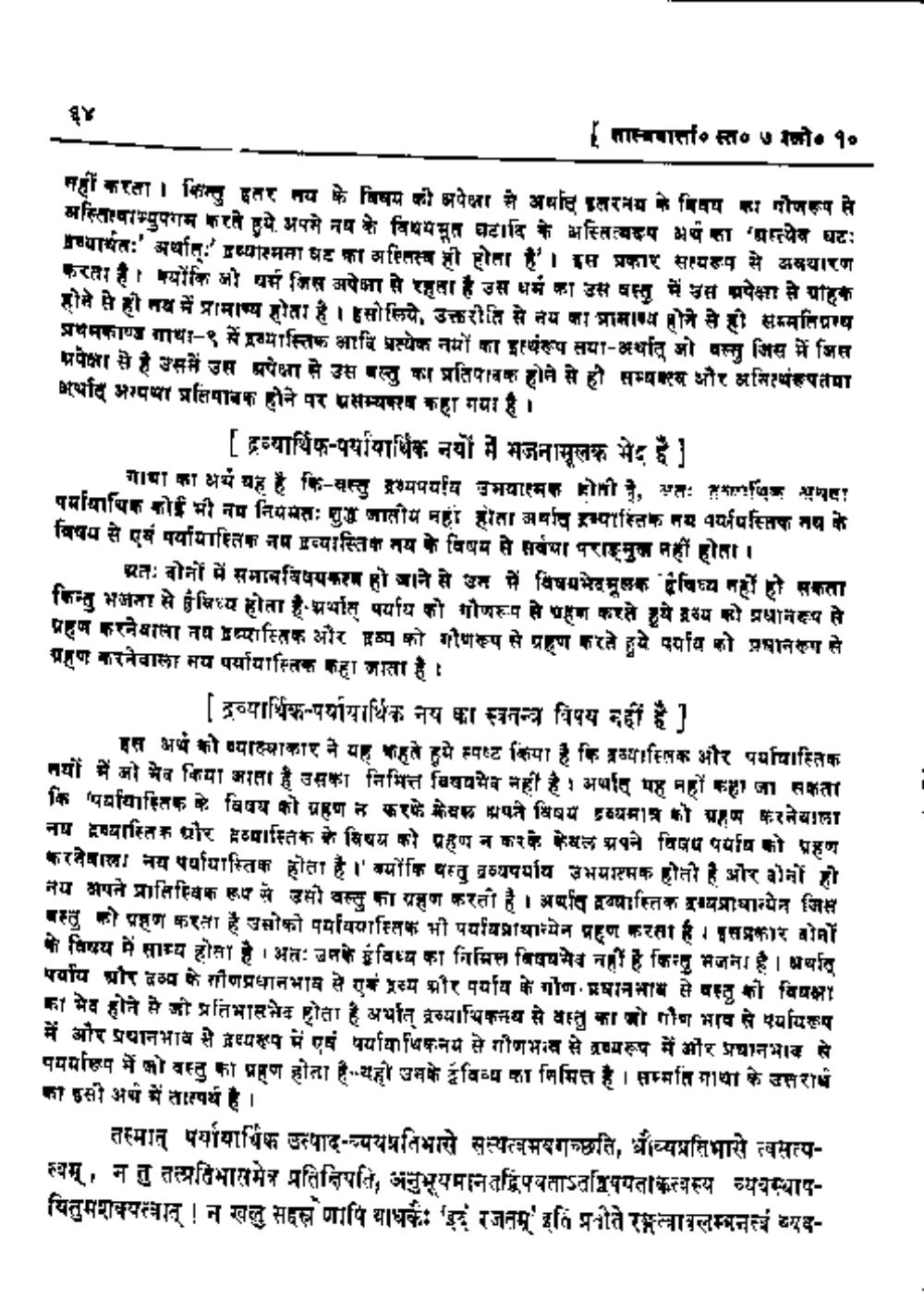________________
मावास्त०७ पलो. १०
नहीं करता। किन्तु इतर नय के विषय की अपेक्षा से अपद इतरनय के विषय का पोजरूप से मस्तिस्पाभ्युपगम करते हुये. अपमे नब के विषय मूत घटादि के अस्तित्वाप असा प्रस्त्येव घट: ध्यार्थतः' अर्थात यास्ममा घट का अस्तित्व ही होता है। इस प्रकार सत्यरूप से अयथारण करता है। क्योंकि जो धर्म जिस अपेक्षा से रहता है उस धर्म का उस वस्तु में उस अपेक्षा से ग्राहक होमे से होनब में प्रामाण्य होता है। सोलिये, उक्तरीति से नय का प्रामाण्य होने से ही सम्मतिनाथ प्रषमकाण्ड गाथा-९ में पूग्यास्तिक भावि प्रत्येक नमों का इस्थरूप सया-अर्थात ओ पल्स जिस में जिस अपेक्षा से है उसमें उस अपेक्षा से उस वस्तु का प्रतिपावक होने से हो सम्बारव और असिस्थापतमा अर्थाद अग्पया प्रसिपावक होने पर प्रसम्यश्व कहा गया है।
[ द्रव्यार्थिफ-पर्यायार्थिक नयों में भजनामूलक भेद है। गाथा का अर्थ यह है कि-वास्तु द्रश्यपर्याय उभयात्मक होती है, अतः कि अगला पर्यायाधिक कोई भी नए नियमतः शुद्ध जातीम महा होता अर्थात हम्पास्तिक नर पर्नपस्तिक नप के विषय से एवं पर्यायास्तिक नम प्रत्यास्तिक नय के विषय से सर्वमा पराङ्मुज नहीं होता।
प्रतः दोनों में समानविषयकरम हो जाने से उन में विषयमेवमूलक विध्य नहीं हो सकता किन्तु भजना से निध्य होता है-मर्थात् पर्याय को गौणरूप से पहण करते हुये द्रश्य को प्रधानरूप से प्रहण करनेवाला नयध्यास्तिक और तव्य को गौणरूप से प्रहण करते हुये पर्याय को प्रधान रूप से ग्रहण करनेवाला मय पर्यायास्तिक कहा जाता है।
[ द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक नय का स्वतन्त्र विषय नहीं है ] इस अर्थ को प्याल्याकार ने यह कहते हुमे स्पष्ट किया है कि व्यास्मिक और पर्यावास्तिक नयों में मो भेव किया जाता है उसका निमित्त विषयमेव नहीं है। अर्थात पह नहीं कहा जा सकता कि 'पर्यायास्तिक के विषय को ग्रहण न करके केवल अपने विषय हुण्यमात्र को ग्रहण करने याला नष दयास्तिक और पास्तिक के विषय को प्रहण न करके केवल अपने विषय पर्याय को प्रहण करनेवाला नय पर्यायास्तिक होता है। क्योंकि बस्तु तव्यपर्याय उभमश्रामक होती है और दोनों ही नय अपने प्रातिस्विक रूप से उसी वस्तु का ग्रहण करती है। अवि पास्तिक म्यप्राधान्यन जिस बस्तु को ग्रहण करता है उसोको पर्यायास्तिक भी पर्यायप्राधान्येन ग्रहण करता है । इसप्रकार बोगों के विषय में साम्य होता है । अतः उनके विध्य का निमिस विषयमेव नहीं है किन्तु मजना है । अर्थात पर्वाय और द्रव्य के गौणप्रधानभाव से एवं त्रस्य और पर्याय के गौण प्रधानाब से वस्तु को विषक्षा का मेव होने से जो प्रतिभासद होता है अर्थात् ग्याथिकलय से धातु का जो गौण भाव से पर्यायरूप में और प्रधानभाव से ध्यप में एवं पर्यायाथिकान से गौणभनय से द्रष्यरूप में और प्रधानभाव से पयहिप में को वस्तु का प्राण होता है यही उनके वैविध्य का निमित्त है। सम्मति गाथा के उसरा का इसी अर्थ में तात्पर्य है।
___ तस्मान् पर्यायार्षिक उत्पाद-व्ययप्रतिभासे सत्पत्नमयगच्छति, पांच्यप्रसिभासे त्वसत्यस्वम् । न तु तत्प्रतिभासमेत्र प्रतिक्षिपति, अनुभूयमानदिपवताऽधिपयताकत्यस्य व्यवस्थापयितुमशक्यत्वात् ! न खलु सहस्र णापि बाधकः इ रजतम्' इति प्रोते रस्त्रावलम्पनत्वं यद