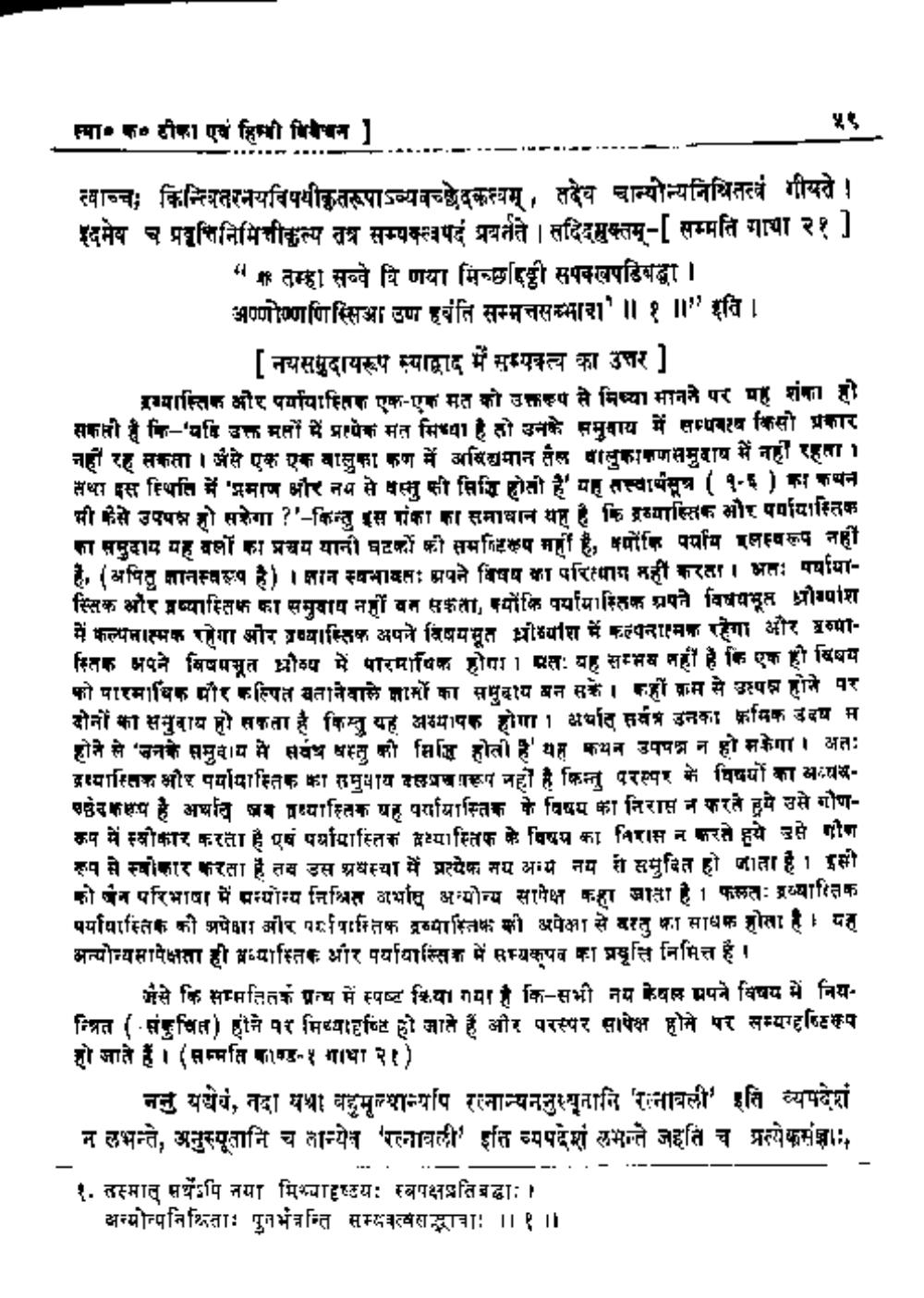________________
५५
स्मा० क० टीका एवं हिन्वी विवेचन ]
स्वाच्च किन्त्रितनयविपयीकृतरूपाऽव्यवच्छेदकस्यम्, तदेव चान्योन्यनिश्रितत्वं गीयते । इदमेव च प्रवृत्तिनिमित्तीकल्प तत्र सम्यक्वपदं प्रवर्तते । तदिदमुक्तम् - [ सम्मति गाथा २१] 41 * तुम्हा सव्वेणिया मच्छडी सपक्खपडिबद्धा । अण्णोष्णणि रिस उण हवंति सम्मतसम्भारा' ॥ १ ॥” इति ।
[ नयसमुदायरूप स्याद्वाद में सम्यक्त्व का उत्तर ]
स्तिक और पर्यायास्तिक एक-एक मत को उक्तरूप से मिथ्या मानने पर यह शंका हो सकती है कि यदि उक्त मतों में प्रत्येक मत मिथ्या है तो उनके समुदाय में सम्uश्व किसी प्रकार नहीं रह सकता। जैसे एक एक वालुका कण में अविद्यमान तेल वालुका कणसमुदाय में नहीं रहता Her इस स्थिति में 'प्रमाण और नम से वस्तु की सिद्धि होती है' यह तत्त्वार्थसूत्र ( १-६ ) का कपन मी कैसे उपपन हो सकेगा ?' किन्तु इस शंका का समाधान यह है कि द्रव्यास्तिक और पर्यायास्तिक का समुदाय यह वलों का प्रथम यानी घटकों को समय नहीं है, क्योंकि पर्याय इलस्वरूप नहीं है (अपितु ज्ञानस्वरूप है) । ज्ञान स्वभावतः अपने विषय का परित्याग नहीं करता। अतः पर्यायाfers और fere का समुदाय नहीं बन सकता, क्योंकि पर्यायास्तिक अपने विषयभूत प्रश मैं कल्पनात्मक रहेगा और प्रति अपने विषयसूत धोश्यांश में कल्पनात्मक रहेगा और fare अपने frauya tou में पारमाविक होगा | यह सम्भव नहीं है कि एक ही विषय को पार्थिक र कल्पित बताने वाले शामों का समुदाय बन सके। कहीं क्रम से उत्पन्न होने पर दोनों का समुदाय हो सकता है किन्तु यह अध्यापक होगा। अर्थात सर्वत्र उनका क्रमिक उदय म होने से 'उनके समुदाय में सर्वत्र वस्तु को सिद्धि होती है यह कथन उपपन्न न हो सकेगा। अतः प्रध्यास्तिक और पर्यायास्तिक का समुदाय रूप नहीं है किन्तु परस्पर के विषयों का अ
है अर्थात् जब प्रध्यास्तिक यह पर्यायास्तिक के विषय का निरास न करते हुये उसे गौणरूप में स्वीकार करता है एवं पर्यायास्तिक वास्तिक के विषय का वास न करते हुये उसे रूप से स्वीकार करता है तब उस श्रवस्या में प्रत्येक नय अन्य नय से समुदित हो जाता है। इसी को जैन परिभाषा में योग्य निश्रित अर्थात् अन्योन्य सापेक्ष कहा जाता है। फलतः प्रव्याक्तिक पास्तिक की अपेक्षा और पाक्तिक द्रव्यास्तिक की अपेक्षा से वस्तु का साधक होता है। यह अन्योन्यसापेक्षता ही अव्यास्तिक और पर्यायास्तिक में सम्यकूपन का प्रवृत्ति निमित्त है ।
जैसे कि सम्मलित प्रत्य में स्पष्ट किया गया है कि सभी नय केवल पने विषय में निय न्त्रित (संकुचित) होने पर हिट हो जाते हैं और परस्पर सापेक्ष होने पर सम्यग्दृष्टिरूप हो जाते हैं। सम्मति-गाथा २१)
ननु यथेयं तदा या मृत्यान्यपि रत्नान्यननुस्मृतानि 'रत्नावली' इति व्यपदेशं न लभन्ते, अनुस्यूतानि च तान्येव 'रत्नावली' इति व्यपदेशं लभन्ते जहति च प्रत्येक संज्ञ
१. तस्मात् सर्वेऽपि नया मिध्यादृष्टयः स्वपक्षप्रतिबद्धाः । अन्योन्यनिश्रिताः पुनर्भवन्ति सम्यक्त्वाचा! ।। १ ।।