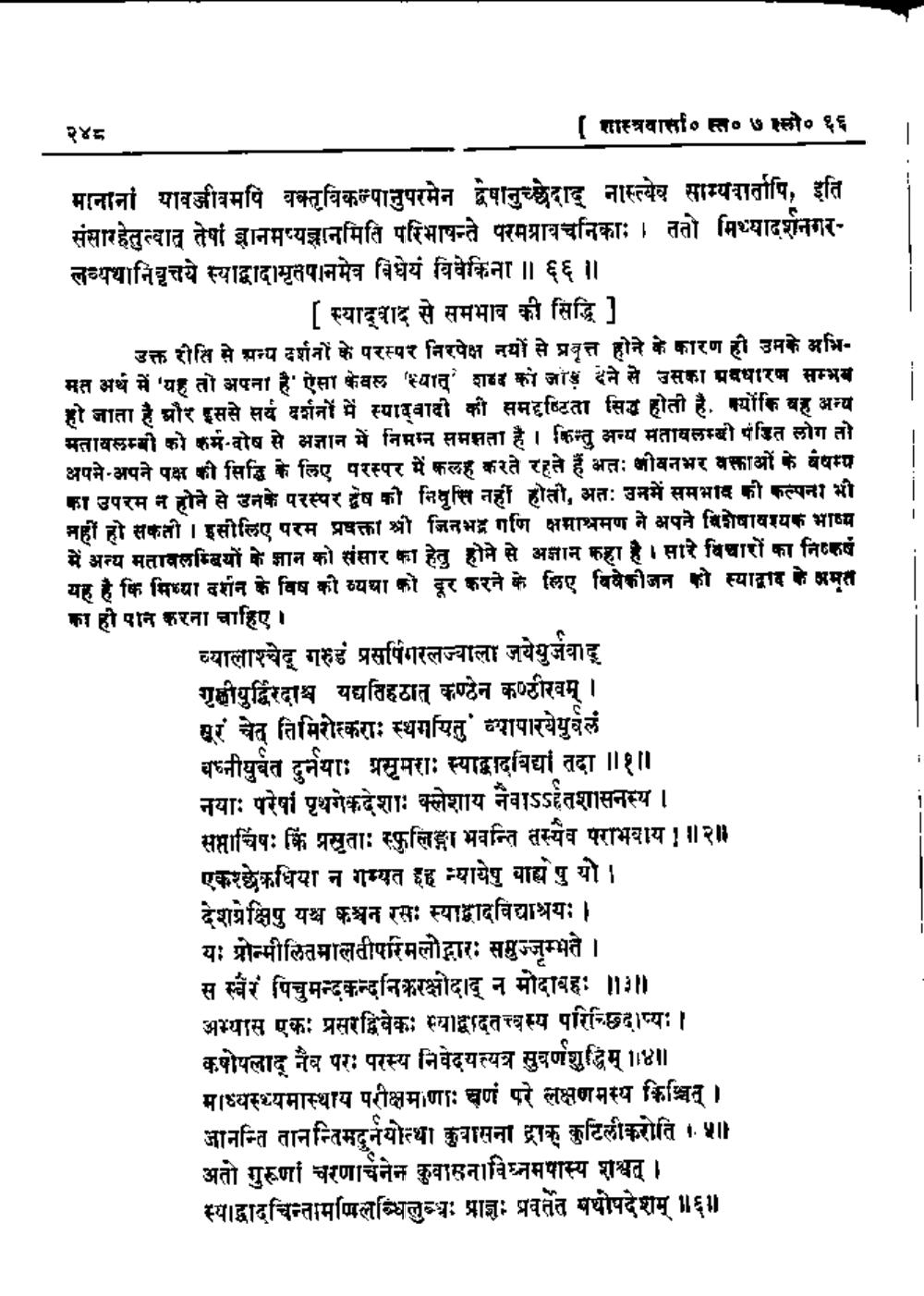________________
२४६
[ शास्त्रवा० ० ७ सो०६६
।
मानानां यावजीवमपि वक्तृविकल्पानुपरमेन द्वेषानुच्छेदाद् नास्त्येव साम्यवार्तापि, इति संसारहेतुत्वात तेषां ज्ञानमयज्ञानमिति परिभाषन्ते परमप्रावनिकाः । ततो मिथ्यादर्शनगरलव्यथानिवृत्तये स्याद्वादामृतपानमेव विधेयं विवेकिना ॥६६॥
[स्याद्वाद से समभाव की सिद्धि ] उक्त रीति से अन्य दर्शनों के परस्पर निरपेक्ष नयों से प्रवृत्त होने के कारण ही उनके अभिमत अर्थ में 'यह तो अपना है ऐसा केवल स्यात्' शब्द को जार देने से उसका प्रवधारण सम्भव हो जाता है और इससे सर्य दर्शनों में स्यादवादी की समदृष्टिता सिद्ध होती है, क्योंकि वह अन्य मतावलम्बी को कर्म-वोष से अज्ञान में निमग्न समानता है। किन्तु अन्य मतावलम्बी पंडित लोग तो अपने-अपने पक्ष की सिद्धि के लिए परस्पर में कलह करते रहते हैं अतः जीवनभर वक्ताओं के बैषम्य का उपरम न होने से उनके परस्पर द्वेष की निवृति नहीं होती, अत: उनमें समभाव की कल्पना भी नहीं हो सकती । इसीलिए परम प्रवक्ता श्री जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण ने अपने विशेषावश्यक भाष्य में अन्य मतावलम्बियों के ज्ञान को संसार का हेतु होने से अज्ञान कहा है। सारे विचारों का निष्कर्ष यह है कि मिथ्या दर्शन के विष को व्यथा को दूर करने के लिए विवेकीजन को स्याद्वाद के अमस का ही पान करना चाहिए।
च्यालाश्चेद् गरुड प्रसर्पिगरलज्याला जयेयुजवाद् गृहीयुद्धिरदाश्च यद्यतिहठात कण्ठेन कण्ठीरवम् । घरं चेत् तिमिरोस्कराः स्थयितु व्यापारयेयुर्वलं चनीयुबेत दुर्नया: प्रसृमराः स्याद्वादविद्यां तदा ॥१॥ नयाः परेषां पृथगेकदेशाः क्लेशाय नैवाऽऽहेतशासनस्य । सप्तार्चिषः किं प्रसृताः स्फुलिङ्गा भवन्ति तस्यैव पराभवाय ॥२॥ एकरछेकधिया न गम्यत इह न्यायेषु याह्य पु यो। देशप्रक्षिपु यश्च कश्चन रसः स्याद्वादविद्याश्रयः। या प्रोन्मीलितमालतीपरिमलोद्वारः समुज्जृम्भते । स स्वैरं पिचुमन्दकन्दनिकरक्षोदाद् न मोदावहः ॥३॥ अभ्यास एकः प्रसरद्विवेकः स्याद्वादतत्त्वस्य परिच्छिदाप्यः । कपोपलाद् नैव परः परस्य निवेदयत्यत्र सुवर्णशुद्धिम् ॥४॥ माध्यस्थ्यमास्थाय परीक्षमाणाः चणं परे लक्षणमस्य किश्चिन् । जानन्ति तानन्तिमदुनयोत्था कुवासना द्राक् कुटिलीकरोति । ५॥ अतो गुरूणां चरणानेन कुवासनाविघ्नमपास्य शश्वत् । स्याद्वादचिन्तामणिलब्धिलुब्धः प्राज्ञः प्रवर्तेत यथोपदेशम् ॥६॥