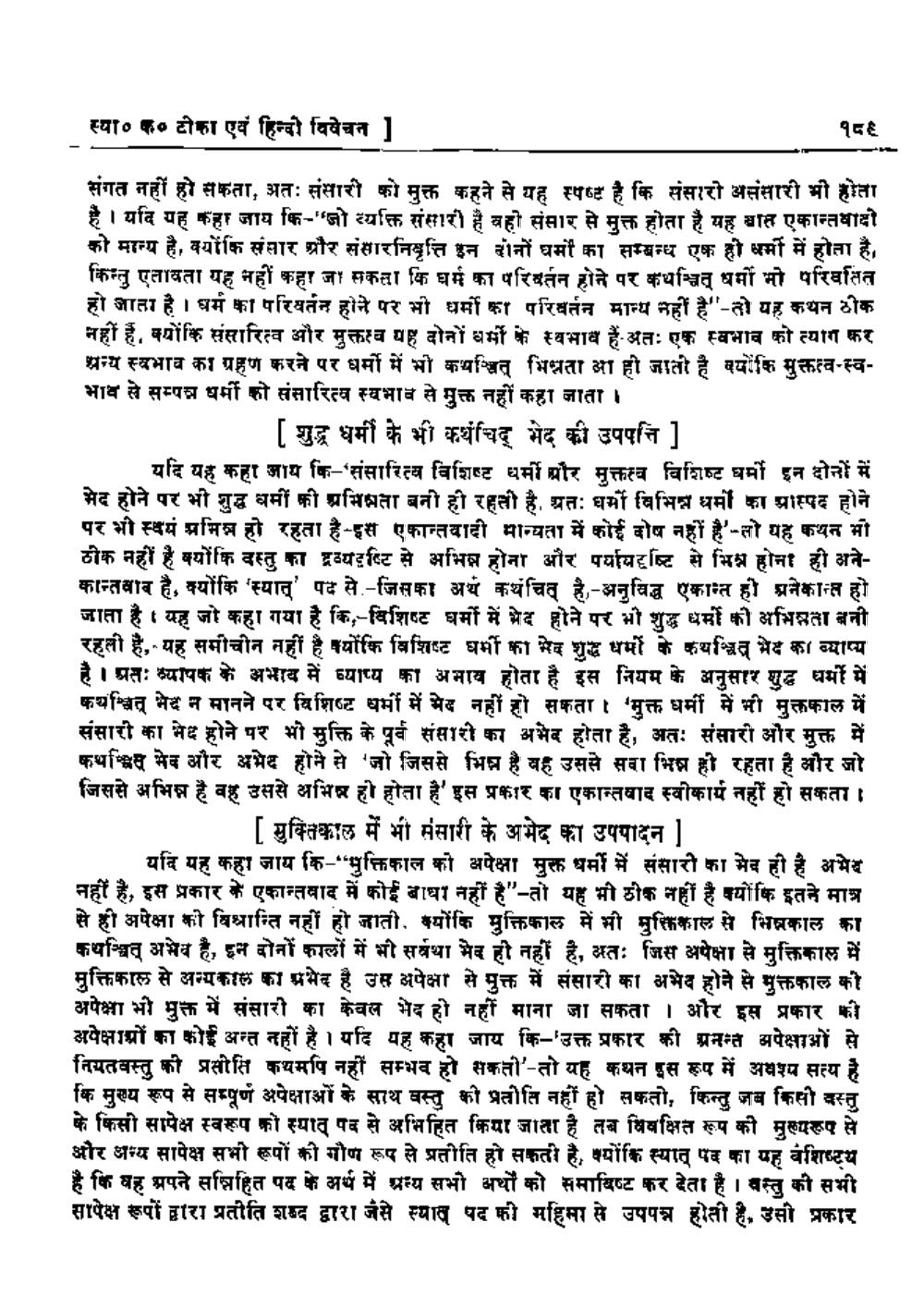________________
स्था० क. टोका एवं हिन्दी विवेचन ]
१८९
संगत नहीं हो सकता, अतः संसारी को मुक्त कहने से यह स्पष्ट है कि संसारो असंसारी भी होता है । यदि यह कहा जाय कि-"जो व्यक्ति संसारी है वहो संसार से मुक्त होता है यह बात एकान्तवादी को मान्य है, क्योंकि संसार और संसारनिवृत्ति इन दोनों धर्मों का सम्बन्ध एक ही धर्मों में होता है, किन्तु एतावता यह नहीं कहा जा सकता कि धर्म का परिवर्तन होने पर कश्चित् धर्मो मो परिवर्तित हो जाता है। धर्म का परिवर्तन होने पर भी धर्मों का परिवर्तन मान्य नहीं है"-तो यह कथन ठीक नहीं है. क्योंकि संसारित्व और मुक्तस्व यह दोनों धर्मों के स्वभाव हैं अतः एक स्वभाव को त्याग कर अन्य स्वभाव का ग्रहण करने पर धर्मों में भी कश्चित् भिन्नता आ ही जाती है क्योंकि मुक्तत्व-स्वभाव से सम्पन्न धर्मी को संसारित्व स्वभाव से मुक्त नहीं कहा जाता।
[ शुद्ध धर्मी के भी कथंचिद् भेद की उपपत्ति ] यदि यह कहा जाय कि-'संसारित्व विशिष्ट धर्मी पौर मुक्तत्व विशिष्ट धर्मो इन दोनों में भेद होने पर भी शुद्ध धमी की प्रभिन्नता बनी ही रहती है, अत: धर्मों विभिन्न धर्मों का प्रास्पद होने पर भी स्वयं अभिन्न हो रहता है-इस एकान्तवादी मान्यता में कोई दोष नहीं है'-तो यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि वस्तु का द्रव्यदृष्टि से अभिन्न होना और पर्यायष्टि से भिन्न होना ही अनेकान्तवाव है, क्योंकि 'स्यात्' पद से.-जिसका अर्थ कथंचित है,-अनुविद्ध एकान्त हो अनेकान्त हो जाता है । यह जो कहा गया है कि,-विशिष्ट धर्मों में भेद होने पर भी शुद्ध धर्मों को अभिन्नता बनी रहती है, यह समीचीन नहीं है क्योंकि विशिष्ट धर्मी का मेव शुद्ध धमों के कश्चित् भेद का व्याप्य है। प्रतः व्यापक के अभाव में ध्याय का अभाव होता है इस नियम के अनुसार शुद्ध धर्मों में कश्चित् भेद न मानने पर विशिष्ट धर्मी में भेद नहीं हो सकता। 'मुक्त धर्मी में भी मुक्तकाल में संसारी का भेद होने पर भी मुक्ति के पूर्व संसारी का अभेद होता है, अतः संसारी और मुक्त में कश्चित भेव और अभेद होने से 'जो जिससे भिन्न है वह उससे सवा भिन्न ही रहता है और जो जिससे अभिन्न है वह उससे अभिन्न हो होता है। इस प्रकार का एकान्तवाद स्वीकार्य नहीं हो सकता।
[ मुक्तिकाल में भी संसारी के अभेद का उपपादन ] यदि यह कहा जाय कि-"मुक्तिकाल को अपेक्षा मुक्त धर्मी में संसारी का मेव ही है अमेव नहीं है, इस प्रकार के एकान्तवाद में कोई बाधा नहीं है"-तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि इतने मात्र से ही अपेक्षा की विश्रान्ति नहीं हो जाती, क्योंकि मुक्तिकाल में भी मुक्तिकाल से भिन्नकाल का कश्चित् अमेव है, इन दोनों कालों में भी सर्वथा भेव ही नहीं है, अतः जिस अपेक्षा से मुक्तिकाल में मुक्तिकाल से अन्यकाल का प्रभेद है उस अपेक्षा से मुक्त में संसारी का अभेव होने से मुक्तकाल की अपेक्षा भी मुक्त में संसारी का केवल भेद हो नहीं माना जा सकता । और इस प्रकार की अपेक्षानों का कोई अन्त नहीं है । यदि यह कहा जाय कि-'उक्त प्रकार की अनन्त अपेक्षाओं से नियतवस्तु की प्रसीति कथमपि नहीं सम्भव हो सकती'-तो यह कथन इस रूप में अवश्य सत्य है कि मुख्य रूप से सम्पूर्ण अपेक्षाओं के साथ वस्तु की प्रतीति नहीं हो सकतो, किन्तु जब किसी वस्तु के किसी सापेक्ष स्वरूप को स्यात् पब से अभिहित किया जाता है तब विवक्षित रूप की मुख्यरूप से और अन्य सापेक्ष सभी रूपों की गौण रूप से प्रतीति हो सकती है, क्योंकि स्यात् पद का यह वैशिष्ट्य है कि वह अपने सन्निहित पद के अर्थ में अन्य सभी अर्थों को समाविष्ट कर देता है । वस्तु की सभी सापेक्ष रूपों द्वारा प्रतीति शब्द द्वारा जैसे स्याव पद की महिमा से उपपन्न होती है, उसी प्रकार