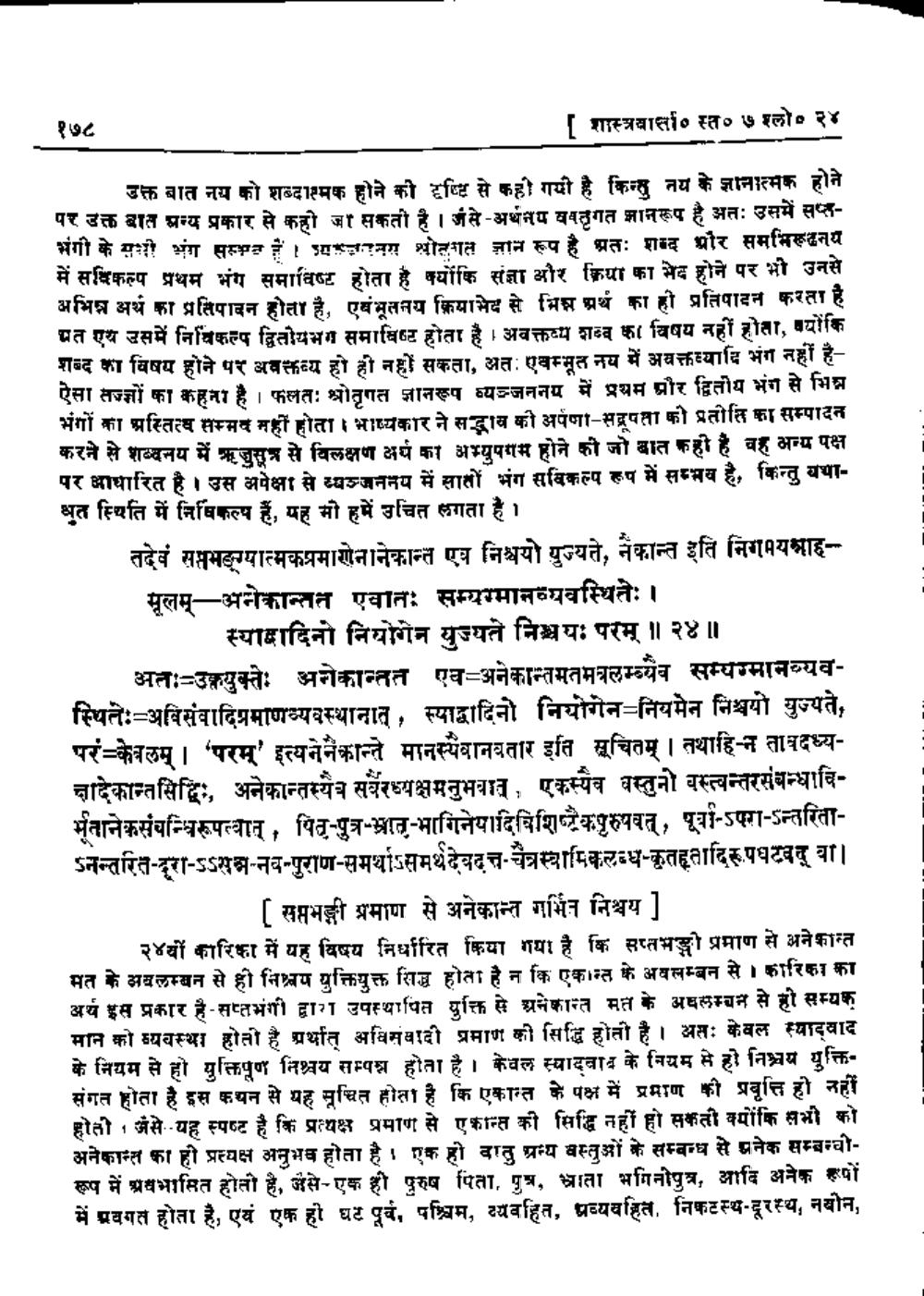________________
१७८
[ शास्त्रवास० स्त० ७ श्लो० २४
उक्त बात नय को शब्दाश्मक होने की दृष्टि से कही गयी है किन्तु नय के ज्ञानात्मक होने पर उक्त बात अन्य प्रकार से कही जा सकती है। अंसे अर्थनय वक्तृगत ज्ञानरूप है अतः उसमें सप्तभंगी के सभी अंग जान रूप है श्रतः शब्द और समभिरूढनय उनसे में सविकल्प प्रथम भंग समाविष्ट होता है क्योंकि संज्ञा और क्रिया का भेद होने पर अभिन्न अर्थ का प्रतिपादन होता है, एवंभूतनय क्रियाभेद से भिन्न अर्थ का ही प्रतिपादन करता है तए उसमें निर्विकल्प द्वितीयभग समाविष्ट होता है। अवक्तव्य शब्द का विषय नहीं होता, क्योंकि शब्द का विषय होने पर अवक्तव्य हो ही नहीं सकता, अतः एवम्भूत नय में अवक्तव्यादि भंग नहीं हैऐसा तज्ज्ञों का कहना है । फलतः श्रोतृगत ज्ञानरूप व्यञ्जननय में प्रथम और द्वितीय भंग से भिन्न अंगों का अस्तित्व समय नहीं होता। भाष्यकार ने सद्भाव की अर्पणा - सद्रूपता की प्रतीति का सम्पादन करने से शब्दमय में ऋजुसूत्र से विलक्षण अर्थ का अभ्युपगम होने की जो बात कही है वह अन्य पक्ष पर आधारित है । उस अपेक्षा से व्यञ्जननय में सातों भंग सविकल्प रूप में सम्भव है, किन्तु यथाभुत स्थिति में निधिकल्प हैं, यह मो हमें उचित लगता है।
तदेवं सप्तभङ्ग्यात्मकप्रमाणेनानेकान्त एव निश्वयो युज्यते, नैकान्त इति निगमयश्नाहमूलम् — अनेकान्तत एवातः सम्यग्मानव्यवस्थितेः । स्याद्वादिनो नियोगेन युज्यते निश्चयः परम् ॥ २४ ॥
अतः उक्तयुक्तेः अनेकान्तत एव अनेकान्तमतमत्रलम्ब्यैव सम्यग्मानव्यवस्थितेः=अविसंवादिप्रमाणव्यवस्थानात् स्याद्वादिनो नियोगेन नियमेन निश्चयो युज्यते, परं=केवलम् | ‘परम्' इत्यनेनैकान्ते मानस्यैवानवतार इति सूचितम् । तथाहि न तावदध्यचादेकान्तसिद्धिः, अनेकान्तस्यैव सर्वैरध्यक्षमनुभवात् एकस्यैव वस्तुनो वस्त्वन्तरसंबन्धाविभूतानेकसंवन्धिरूपत्वात् पितु पुत्र-आत्-भागिनेयादिविशिष्यैकपुरुषवत् पूर्वा ऽपराऽन्तरिताऽनन्तरित दूरा -ऽऽसन- नव-पुराण-समर्थाऽसमर्थ देवदत्त चैत्रस्वामिकलब्ध-कृतहृतादिरूपघटवद् वा ।
.
↑
,
[ सप्तभङ्गी प्रमाण से अनेकान्त गर्भित निश्चय ]
२४ कारिका में यह विषय निर्धारित किया गया है कि सप्तभङ्गी प्रमाण से अनेकान्त मत के अवलम्बन से ही निश्चय युक्तियुक्त सिद्ध होता है न कि एकान्त के अवलम्बन से । कारिका का अर्थ इस प्रकार है - सप्तभंगी द्वारा उपस्थापित युक्ति से अनेकान्त मत के अवलम्बन से ही सम्यक मान को व्यवस्था होती है प्रर्थात् अविसंवादी प्रमाण की सिद्धि होती है। अतः केवल स्थादवाद के नियम से हो युक्तिपूर्ण निश्चय सम्पन्न होता है। केवल स्यादवाद के नियम से ही निश्चय युक्तिसंगत होता है इस कथन से यह सूचित होता है कि एकान्त के पक्ष में प्रमाण की प्रवृत्ति ही नहीं होती जैसे यह स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से एकान्त की सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि सभी को अनेकान्त का ही प्रत्यक्ष अनुभव होता है। एक ही वातु ग्रन्य वस्तुओं के सम्बन्ध से अनेक सम्बन्धीरूप में प्रभासित होती है, जैसे- एक ही पुरुष पिता, पुत्र, भ्राता भगिनोपुत्र, आदि अनेक रूपों में प्रवगत होता है, एवं एक ही घट पूर्व, पश्चिम, व्यवहित, धव्यवहित निकटस्थ दूरस्थ, नवीन,
1