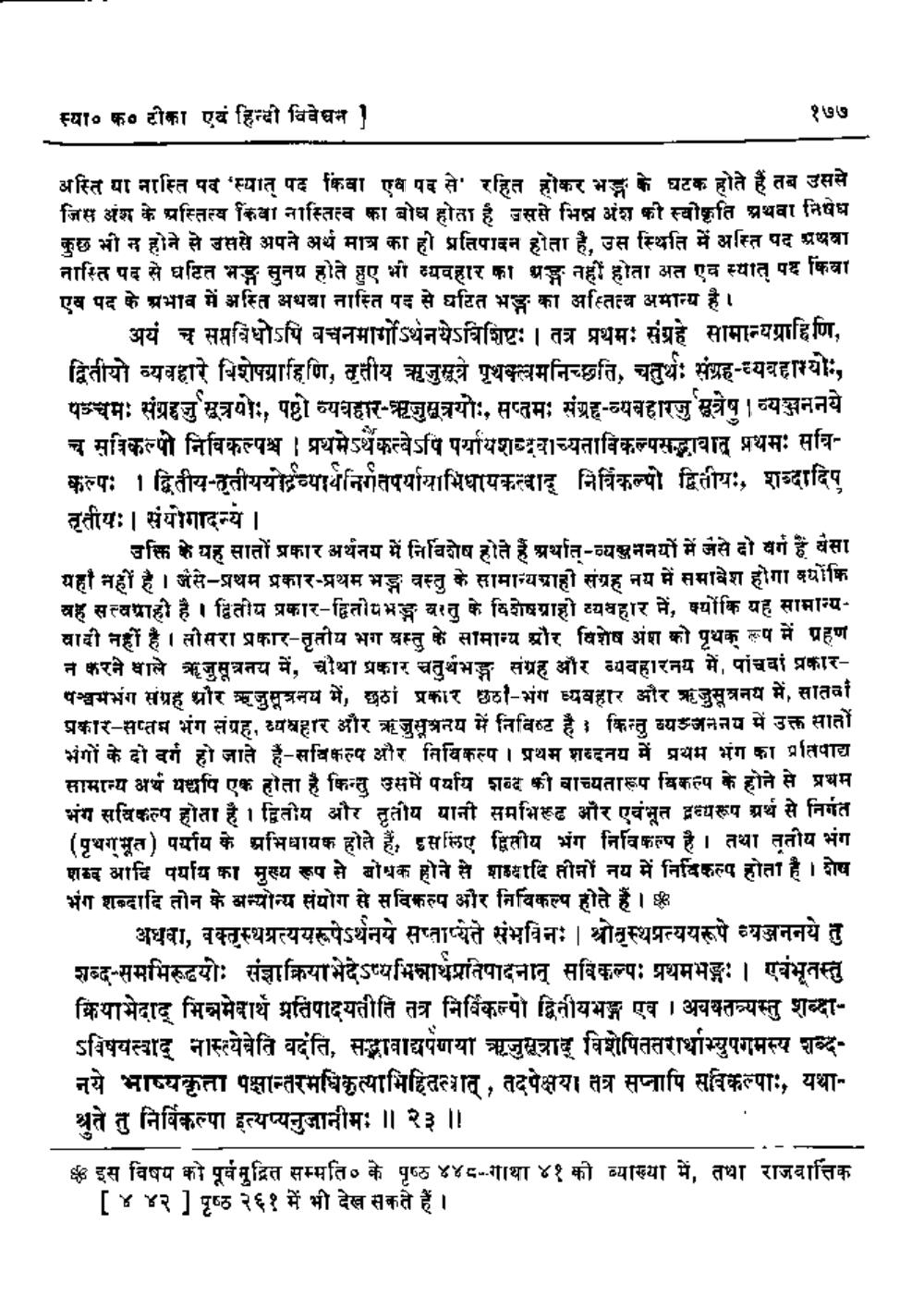________________
स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन ]
अस्ति या नास्ति पर्व 'स्यात् पद किंवा एव पद से रहित होकर भङ्ग के घटक होते हैं तब उससे जिस अंश के प्रस्तित्व किंवा नास्तित्व का बोध होता है उससे भिन्न अंश की स्वीकृति प्रथवा निषेध कुछ भी न होने से उससे अपने अर्थ मात्र का ही प्रतिपादन होता है, उस स्थिति में अस्ति पद अथवा नास्ति पद से घटित भङ्ग सुनय होते हुए भी व्यवहार का भङ्ग नहीं होता अत एव स्यात् पद किंवा एव पद के प्रभाव में अस्ति अथवा नास्ति पद से घटित भङ्ग का अस्तित्व अमान्य है ।
अयं च सप्तविधोऽपि वचनमार्गोऽथेनयेऽविशिष्टः । तत्र प्रथमः संग्रहे सामान्य ग्राहिणि, द्वितीयो व्यवहारे विशेषग्राहिणि, तृतीय ऋजुसूत्रे पृथक्त्वमनिच्छति, चतुर्थः संग्रह व्यवहारयोः, पञ्चमः संग्रहजु सूत्रयोः, पट्टो व्यवहार ऋजुसूत्रयोः, सप्तमः संग्रह - व्यवहारजु सूत्रेषु । व्यञ्जननये
विकल्पो निर्विकल्पश्च । प्रथमेऽथकत्वेऽपि पर्यायशब्दवाच्यताविकल्पसद्भावात् प्रथमः सवि कल्पः । द्वितीय तृतीययोर्द्रव्यार्थ निर्गतपर्यायाभिधायकत्वाद् निर्विकल्पो द्वितीयः शब्दादिपु तृतीयः । संयोगादन्यं |
उक्ति के यह सातों प्रकार अर्थनय में निर्विशेष होते हैं अर्थात् व्यञ्जननयों में जैसे दो वर्ग हैं वैसा यहाँ नहीं है। जैसे- प्रथम प्रकार प्रथम भङ्ग वस्तु के सामान्यग्राही संग्रह नय में समावेश होगा क्योंकि वह सत्वग्राही है । द्वितीय प्रकार- द्वितीयभङ्ग वस्तु के विशेषग्राही व्यवहार में, क्योंकि यह सामान्यवादी नहीं है । तीसरा प्रकार - तृतीय भग वस्तु के सामान्य और विशेष अंश को पृथक् रूप में ग्रहण न करने वाले ऋजुसूत्रनय में, चौथा प्रकार चतुर्थभङ्ग संग्रह और व्यवहारनय में पांचवां प्रकारपञ्श्वमभंग संग्रह और ऋजुसूत्रमय में छठां प्रकार छठी-भंग व्यवहार और ऋजुसूत्रनय में, सातक प्रकार - सप्तम भंग संग्रह व्यवहार और ऋजुसूत्रत्य में निविष्ट है किन्तु व्यञ्जननय में उक्त सातों भंगों के दो वर्ग हो जाते हैं- सविकल्प और निविकल्प | प्रथम शब्दनय में प्रथम भंग का प्रतिपाद्य सामान्य अर्थ यद्यपि एक होता है किन्तु उसमें पर्याय शब्द की वाच्यतारूप विकल्प के होने से प्रथम भंग सविकल्प होता है । द्वितीय और तृतीय यानी समभिरूट और एवंभूत द्रव्यरूप अर्थ से निर्गत ( पृथग्भूत) पर्याय के अभिधायक होते हैं, इसलिए द्वितीय भंग निर्विकल्प है। तथा तृतीय भंग शब्द आदि पर्याय का मुख्य रूप से बोधक होने से शब्दादि तीनों नय में निर्विकल्प होता है। शेष भंग शब्दादि तोन के अन्योन्य संयोग से सविकल्प और निर्विकल्प होते हैं।
अथवा, वक्तृस्थप्रत्ययरूपेऽर्थनये सप्ताप्येते संभविनः । श्रोतस्थप्रत्ययरूपे व्यञ्जननये तु शब्द- समभिरुद्वयोः संज्ञाक्रिया भेदेऽप्यभिन्नार्थप्रतिपादनात् सविकल्पः प्रथमभङ्गः । एवंभूतस्तु क्रियाभेदाद् भिन्नमेवार्थे प्रतिपादयतीति तत्र निर्विकल्पो द्वितीयभङ्ग एव । अवक्तव्यस्तु शब्दाSविषयत्वाद् नास्त्येवेति वदति, सद्भावाद्यर्पणया ऋजुसूत्राद् विशेषिततरार्थाभ्युपगमस्य शब्दनये भाष्यकृता पक्षान्तरमधिकृत्याभिहितत्वात् तदपेक्षया तत्र सप्नापि सविकल्पाः, यथा - श्रुते तु निर्विकल्पा इत्यप्यनुजानीमः || २३ ||
7
१७७
* इस विषय को पूर्व मुद्रित सम्मति के पृष्ठ ४४८ - गाथा ४१ की व्याख्या में, तथा राजवार्तिक [ ४ ४२ ] पृष्ठ २६१ में भी देख सकते हैं ।