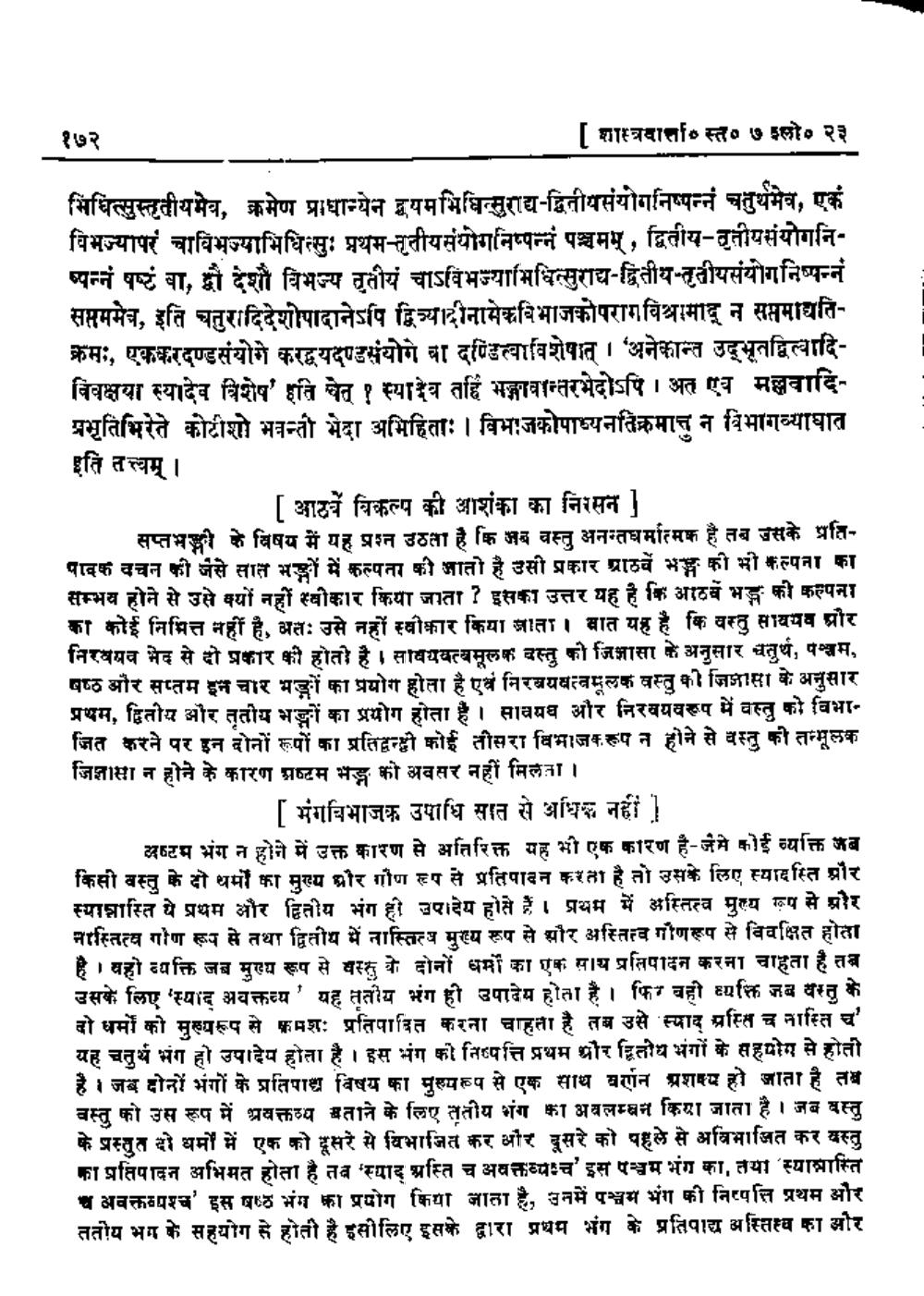________________
१७२
[ शास्त्रवान स्त०७लो. २३
भिधित्सुस्तृतीयमेव, क्रमेण प्राधान्येन द्वयमभिधिसुराद्य-द्वितीयसंयोगनिष्पन्नं चतुर्थमेव, एक विभज्यापरं चाविभज्याभिधित्सुः प्रथम-तृतीयसंयोगनिष्पन्न पञ्चमम् , द्वितीय-तृतीयसंयोगनिप्पन्नं षष्टं वा, द्वौ देशौ विभज्य तृतीयं चाऽविभज्याभिधित्सुराद्य-द्वितीय-तृतीयसंयोगनिष्पन्न सप्तममेव, इति चतुरादिदेशीपादानेऽपि द्विव्यादीनामेकविभाजकोपरागविश्रामाद् न सप्तमाघतिक्रमः, एककरदण्डसंयोगे करद्वयदण्डसंयोगे वा दण्डित्वाविशेषात् । 'अनेकान्त उद्धृतद्वित्वादिविवक्षया स्यादेव विशेष' इति चेत् ? स्यादेव तहि भङ्गावान्तरभेदोऽपि । अत एव मल्लवादिप्रभृतिभिरेते कोटीशो भवन्ती भेदा अभिहिताः । विभाजकोपाध्यनतिक्रमात न विभागव्याघात इति तत्त्वम् ।
[आठवें विकल्प की आशंका का निरसन ] सप्तमी के विषय में यह प्रश्न उठता है कि जब वस्तु अनन्तधर्मात्मक है तब उसके प्रतिपावक वचन की जैसे सात भङ्गों में कल्पना की जाती है उसी प्रकार प्राठवें मन की भी कल्पना का सम्भव होने से उसे क्यों नहीं स्वीकार किया जाता ? इसका उत्तर यह है कि आठवें भङ्ग की कल्पना का कोई निमित्त नहीं है, अतः उसे नहीं स्वीकार किया जाता। बात यह है कि वस्तु सावयव और निरवयव भेद से दो प्रकार की होती है। सावयवत्वमूलक वस्तु को जिज्ञासा के अनुसार चतुर्थ, पश्चम, षष्ठ और सप्तम इन चार भडों का प्रयोग होता है एवं निरजयवत्वमूलक वस्तु की जिज्ञासा के अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय भङ्गों का प्रयोग होता है। सावयव और निरवयवरूप में वस्तु को विभाजित करने पर इन दोनों रूपों का प्रतिद्वन्द्वी कोई तीसरा विभाजकरूप न होने से वस्तु की तन्मूलक जिज्ञासा न होने के कारण अष्टम भङ्ग को अवसर नहीं मिलता।
[ मंगविभाजक उपाधि सात से अधिक नहीं ] अष्टम भंग न होने में उक्त कारण से अतिरिक्त यह भी एक कारण है-जैसे कोई व्यक्ति जब किसी वस्तु के दो थमों का मुख्य प्रऔर गौण रूप से प्रतिपादन करता है तो उसके लिए स्यादस्ति और स्यानास्ति ये प्रथम और द्वितीय भंग ही उपादेय होते हैं। प्रथम में अस्तित्व मुख्य रूप से और नास्तित्व गौण रूप से तथा द्वितीय में नास्तित्व मुख्य रूप से और अस्तित्व गौणरूप से विवक्षित होता है। वहो व्यक्ति जब मुख्य रूप से वस्तु के दोनों धर्मों का एक साय प्रतिपादन करना चाहता है तब उसके लिए 'स्याद अवक्तव्य' यह ततीय भंग ही उपादेय होता है। फिर वही व्यक्ति जब वस्तु के दो धर्मों को मुख्यरूप से क्रमशः प्रतिपारित करना चाहता है तब उसे स्याद् अस्ति च नास्ति च' यह चतुर्थ भंग हो उपादेय होता है । इस भंग को निष्पत्ति प्रथम और द्वितीय भंगों के सहयोग से होती है । जब दोनों भंगों के प्रतिपाद्य विषय का मुख्यरूप से एक साथ वर्णन अशक्य हो जाता है तब वस्तु को उस रूप में प्रवक्तव्य बताने के लिए ततीय भंग का अवलम्बन किया जाता है । जब वस्तु के प्रस्तुत दो धर्मों में एक को दूसरे से विभाजित कर और दूसरे को पहले से अविभाजित कर वस्तु का प्रतिपादन अभिमत होता है तब 'स्याद् अस्ति च अवक्तव्याच' इस पञ्चम भंग का, तया स्यान्नास्ति च अवक्तम्पश्च' इस षष्ठ भंग का प्रयोग किया जाता है, उनमें पञ्चम भंग की निष्पत्ति प्रथम और ततीय भा के सहयोग से होती है इसीलिए इसके द्वारा प्रथम भंग के प्रतिपाद्य अस्तित्व का और