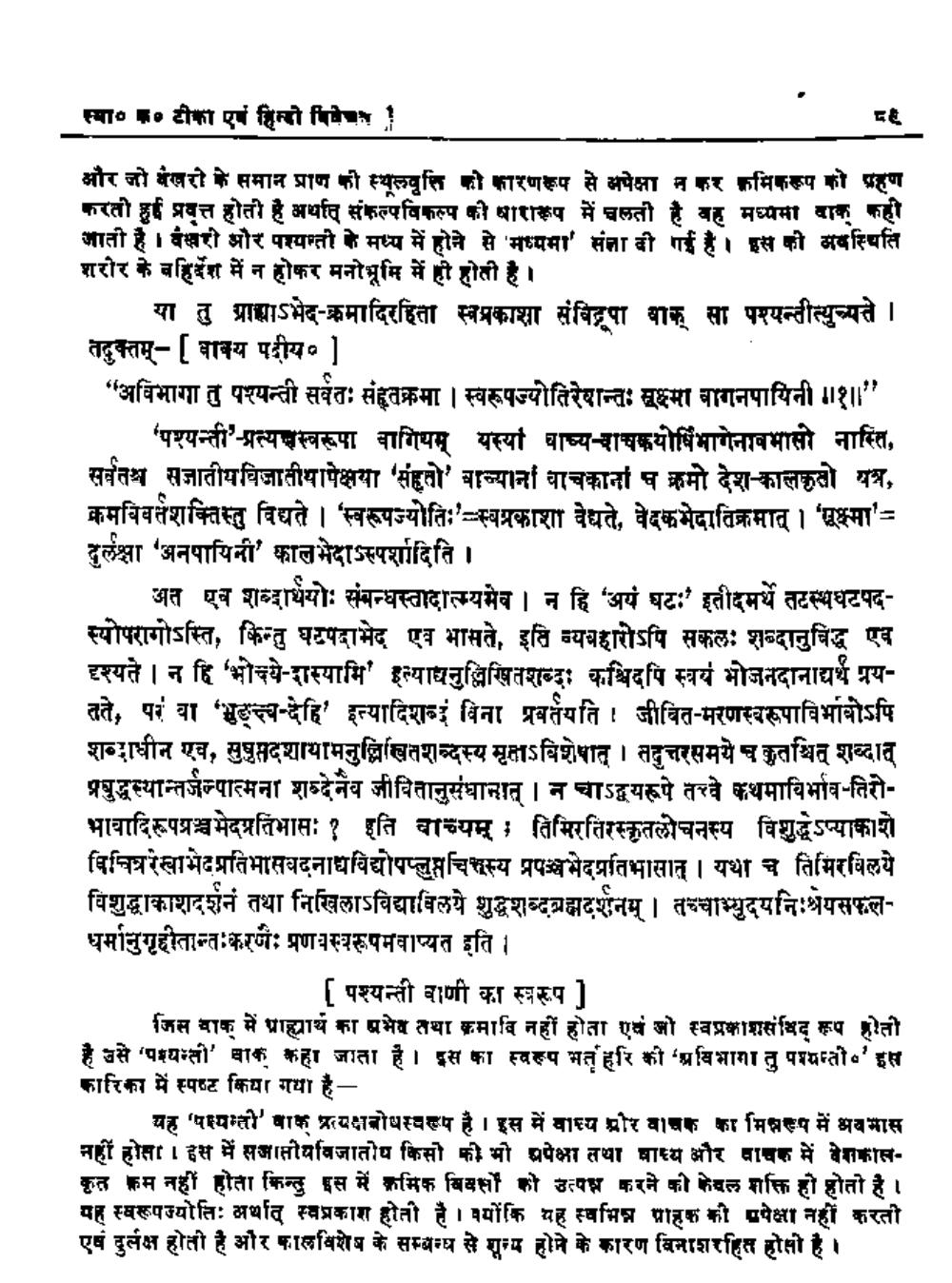________________
स्मा० क० टीका एवं हिन्दी विवे
और जो वैखरो समान प्राण की स्थूलवृति को कारणरूप से अपेक्षा न कर क्रमिकरूप को ग्रहण करती हुई प्रवृत्त होती है अर्थात् संकल्पविकल्प की धारारूप में चलती है वह मध्यमा वाक् कही जाती है। वैखरी और पश्यन्ती के मध्य में होने से 'मध्यमा' संज्ञा दी गई है। इस की अवस्थिति शरीर के बहिर्देश में न होकर मनोभूमि में ही होती है।
६६
या तु ग्राह्याऽभेद क्रमादिरहिता स्वप्रकाशा संविद्रूपा वाक् सा पश्यन्तीत्युच्यते । तदुक्तम् - [ वाक्यपदीय० ]
“अविभागा तु पश्यन्ती सर्वतः संहृवक्रमा । स्वरूपज्योतिरेषान्तः सूक्ष्मा वागनपायिनी ॥|१||”
'पश्यन्ती' प्रत्यक्षस्वरूपा बागियम् यस्य वाच्य वाचक योषिभागेनावभासो नास्ति, सर्वतश्च सजातीयविजातीयापेक्षया 'संहतो' वान्यानां वाचकानां च क्रमो देश-कालकृतो यत्र, क्रमविवर्तशक्तिस्तु विद्यते । 'स्वरूपज्योतिः 'स्वप्रकाशा वैधते, वेदकभेदातिक्रमात् । 'सूक्ष्मा'= दुर्लक्षा 'अनपायिनी' कालभेदाऽस्पर्शादिति ।
अत एव शब्दार्थयोः संबन्धस्तादात्म्यमेव । न हि 'अयं घटः' इतीदमर्थे तटस्थघटपदस्योपरागोऽस्ति, किन्तु घटपदाभेद एव भासते इति व्यवहारोऽपि सकलः शब्दानुविद्ध एव दृश्यते । न हि 'भोचये दास्यामि' इत्याद्यनुल्लिखितशब्दः कश्चिदपि स्वयं भोजनदानाद्यर्थं प्रयतते, परं वा 'य- देहि' इत्यादिशब्दं विना प्रवर्तयति । जीवित मरणस्वरूपाविर्भावोऽपि शब्दाधीन एव, सुषुप्तदशायामनुल्लिखित शब्दस्य मृताऽविशेषात् । तदुत्तरसमये च कृतश्चित् शब्दात् प्रबुद्धस्यान्तर्जल्पात्मना शब्देनैव जीवितानुसंधानात् । न चाऽद्वयरूपे तत्वे कथमाविर्भाव-तिरोभावादिरूपप्रञ्च भेदप्रतिभासः ? इति वाच्यम् तिमिरतिरस्कृतलोचनस्य विशुद्धेऽप्याकाशे विचित्ररेखाभेदप्रतिभासवदनाद्यविद्योपप्लुप्तचिश्वस्य प्रपञ्चभेदप्रतिभासात् । यथा च तिमिरविलये विशुद्धाकाशदर्शनं तथा निखिला विद्याविलये शुद्धशब्दब्रह्मदर्शनम् । तच्चाभ्युदयनिःश्रेयसफलधर्मानुगृहीतान्तःकरणैः प्रणवस्त्ररूपमवाप्यत इति ।
[ पश्यन्ती वाणी का स्त्ररूप ]
जिस वाक में प्राह्मार्थ का प्रभेव तथा क्रमावि नहीं होता एवं जो स्वप्रकाशसंविद् रूप होती है उसे 'पश्यन्ती' वाक् कहा जाता है। इस का स्वरूप भर्तृहरि की 'श्रविभागा तु पश्यन्ती० ' इस कारिका में स्पष्ट किया गया है
यह 'पश्यन्ती' वाक् प्रत्यक्षबोधस्वरूप है। इस में वाध्य श्रीर वाचक का मित्ररूप में अवभास नहीं होता । इस में सजातीयविजातीय किसी की भी अपेक्षा तथा वाध्य और वाचक में देशकालकृत कम नहीं होता किन्तु इस में क्रमिक बिवसों को उत्पन्न करने की केवल शक्ति हो होती है । यह स्वरूपज्योति अर्थात् स्वप्रकाश होती है। क्योंकि यह स्वभिन्न ग्राहक की पपेक्षा नहीं करती एवं दुर्लक्ष होती है और कालविशेष के सम्बन्ध से शून्य होने के कारण विनाशरहित होती है ।