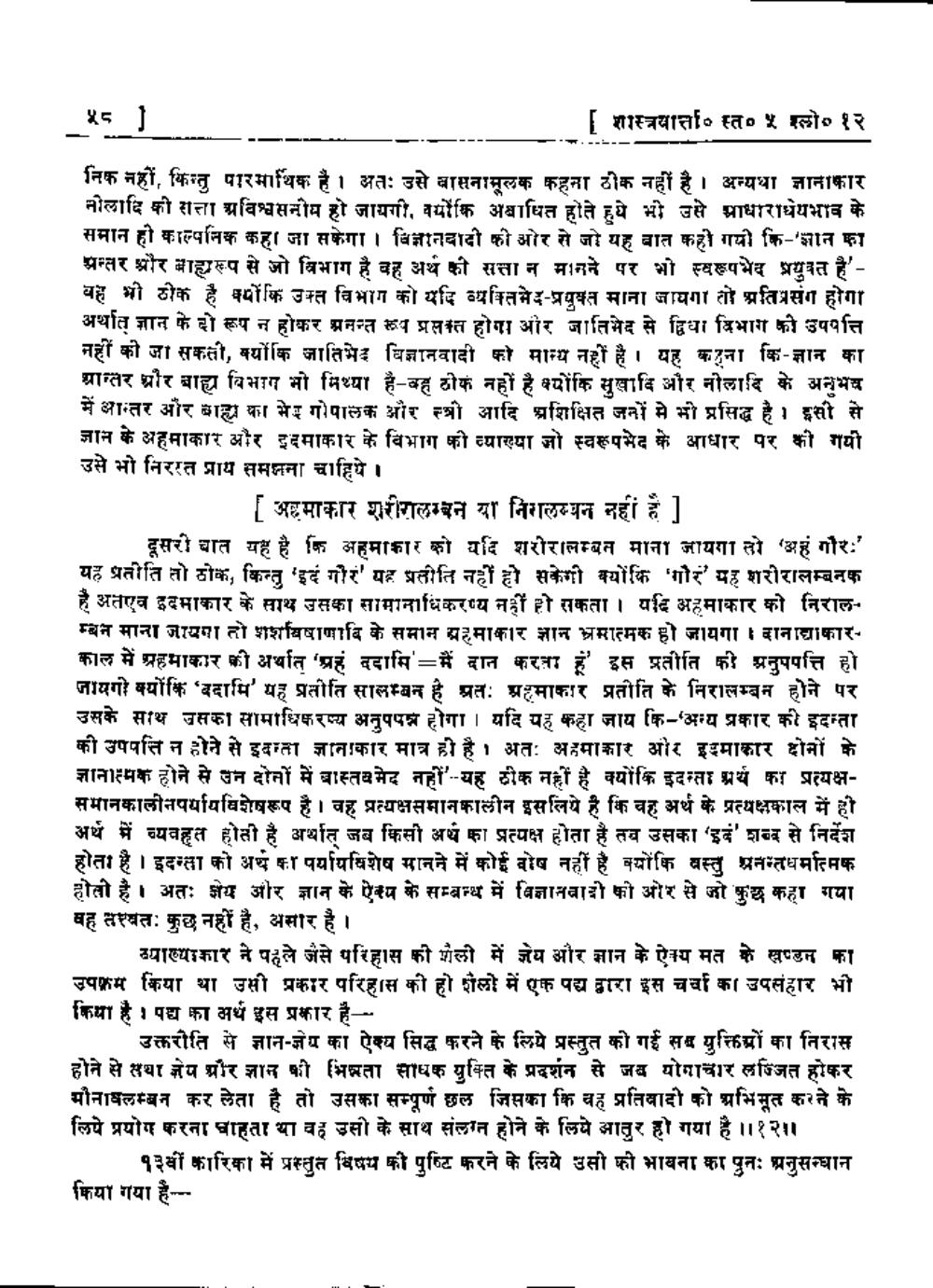________________
५८ ]
[ शास्त्रयाता० स्त०५ श्लो०१२
निक नहीं, किन्तु पारमार्थिक है। अतः उसे वासनामूलक कहना ठीक नहीं है। अन्यथा जानाकार मौलादि की सत्ता अविश्वसनीय हो जायगी, क्योंकि अबाधित होते हुये भी उसे प्राधाराधेयभाव के समान हो काल्पनिक कहा जा सकेगा। विज्ञानवादी की ओर से जो यह बात कही गयो कि-'ज्ञान का अन्तर और बाह्यरूप से जो विभाग है वह अर्थ को सत्ता न मानने पर भी स्वरूपभेद प्रयुक्त हैवह भी ठीक है क्योंकि उक्त विभाग को यदि व्यक्तिमेद-प्रयुक्त माना जायगा तो अतिप्रसंग होगा अर्थात जान के दो रूप न होकर अनन्त रूप प्रलक्त होगा और जातिभेद से द्विधा विभाग को उपपत्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि जातिभेद विज्ञानवादी को मान्य नहीं है। यह कहना कि-ज्ञान का प्रान्तर और बाह्य विभाग भो मिथ्या है-वह ठीक नहीं है क्योंकि सुखादि और नीलादि के अनुभव में आन्तर और बाहर का भेष गोपालक और स्त्री आदि प्रशिक्षित जनों में भी प्रसिद्ध है। इसी से ज्ञान के अहमाकार और इदमाकार के विभाग की व्याख्या जो स्वरूपभेद के आधार पर की गयी उसे भो निरस्त प्राय समझना चाहिये।
[ अहमाकार शरीरालम्बन या निगलम्बन नहीं है ] दूसरी चात यह है कि अहमाकार को यदि शरीरालम्बन माना जायगा तो 'अहं गौरः' यह प्रतीति तो ठोक, किन्तु 'इदं गौर' यह प्रतीति नहीं हो सकेगी क्योंकि 'गौरं' यह शरीरालम्बनक है अतएव इदमाकार के साथ उसका सामानाधिकरण्यन हो सकता। यदि अहमाकार को । म्बन माना जायमा तो शविषाणादि के समान ग्रहमाकार ज्ञान भ्रमात्मक हो जायगा । दानाद्याकारकाल में ग्रहमाकार की अर्थात 'प्रहं ददामि'=मैं दान करता हूँ' इस प्रतीति की अनुपपत्ति हो जायगी क्योंकि वदामि' यह प्रतीति सालम्बन है प्रतः प्रहमाकार प्रतीति के निरालम्बन होने पर उसके साथ उसका सामाधिकरप्य अनुपपन्न होगा। यदि यह कहा जाय कि-'अन्य प्रकार की इदन्ता की उपपत्ति न होने से इदाता ज्ञानाकार मात्र ही है। अतः अहमाकार और इदमाकार दोनों के ज्ञानात्मक होने से उन दोनों में वास्तव मेद नहीं-यह ठीक नहीं है क्योंकि इदन्ता प्रर्य का प्रत्यक्षसमानकालीनपर्यायधिशेषरूप है। वह प्रत्यक्षसमानकालीन इसलिये है कि वह अर्थ के प्रत्यक्षकाल में ही अर्थ में व्यवहृत होती है अर्थात् जब किसी अर्थ का प्रत्यक्ष होता है तब उसका 'इ' शब्द से निर्देश होता है । इदन्ता को अर्थ का पर्यायविशेष मानने में कोई दोष नहीं है क्योंकि वस्तु अनन्तधर्मात्मक होती है। अतः ज्ञेय और ज्ञान के ऐक्य के सम्बन्ध में विज्ञानवादी की ओर से जो कुछ कहा गया यह तस्वतः कुछ नहीं है, असार है।
व्याख्याकार ने पहले जैसे परिहास की शैली में ज्ञेय और ज्ञान के ऐलय मत के वण्डन का उपक्रम किया था उसी प्रकार परिहास की हो शैली में एक पद्य द्वारा इस चर्चा का उपसंहार भी किया है। पद्य का अर्थ इस प्रकार है---
उक्तरोति से ज्ञान-ज्ञेय का ऐक्य सिद्ध करने के लिये प्रस्तुत की गई सब युक्तियों का निरास होने से तथा जेय और ज्ञान की भिन्नता साधक युक्ति के प्रदर्शन से जब योगाचार लज्जित होकर मौनावलम्बन कर लेता है तो उसका सम्पूर्ण छल जिसका कि वह प्रतिवादी को अभिमूत करने के लिये प्रयोग करना चाहता था वह उसी के साथ संलग्न होने के लिये आतुर हो गया है ।।१२॥
१३वीं कारिका में प्रस्तुत विषय की पुष्टि करने के लिये उसी की भावना का पुनः अनुसन्धान किया गया है--