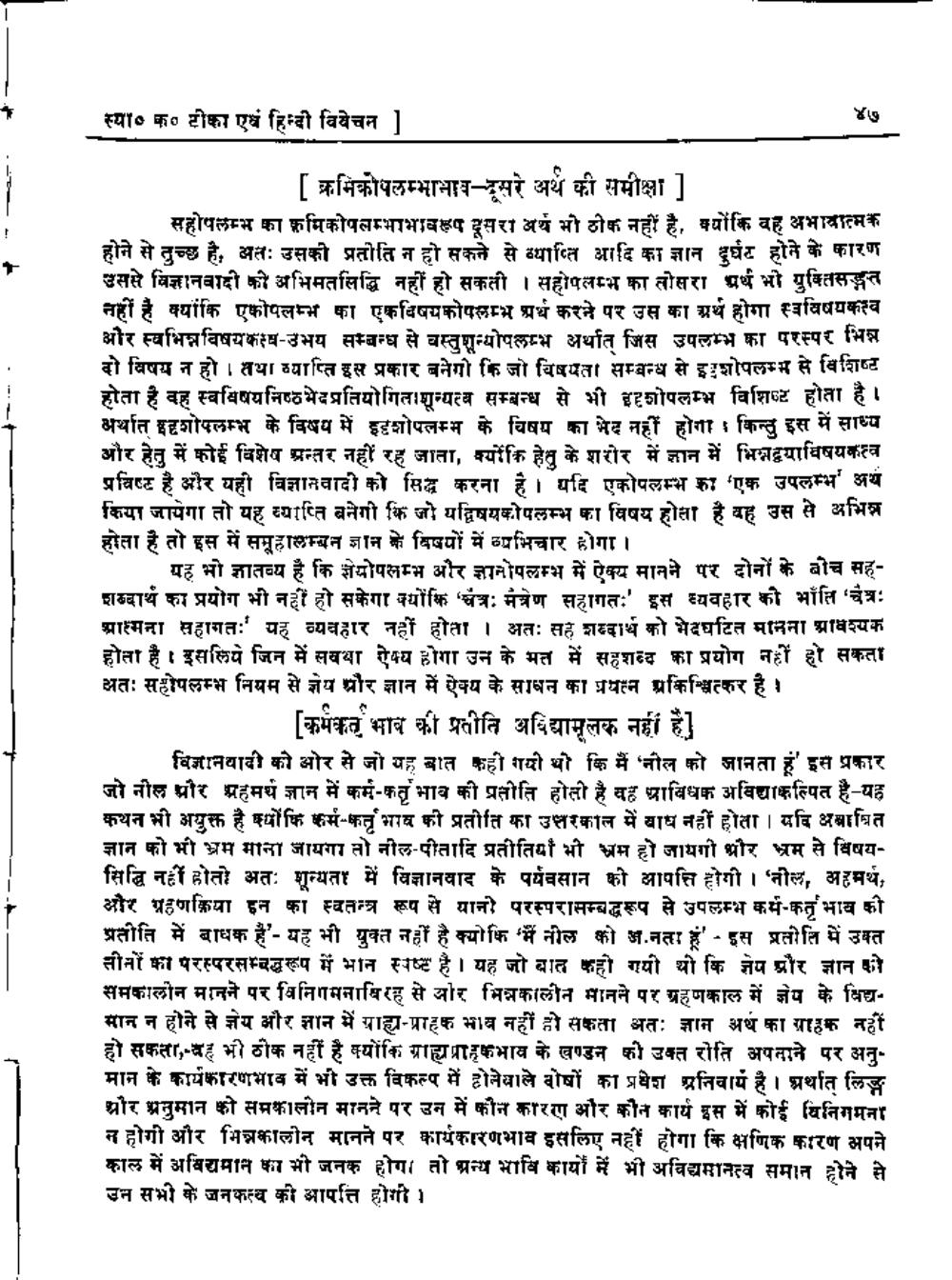________________
स्या० का टीका एवं हिन्दी विवेचन ]
[ क्रमिकोपलम्भाभाव-दूसरे अर्थ की समीक्षा ] सहोपलम्भ का क्रमिकोपलम्भाभावरूप दूसरा अर्थ भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह अभावात्मक होने से तुच्छ है, अतः उसकी प्रतीति न हो सकने से व्याप्ति आदि का ज्ञान दुर्घट होने के कारण उससे विज्ञानवादी को अभिमतसिद्धि नहीं हो सकती । सहोपलम्भ का तीसरा अर्थ भी युक्तिसङ्गत नहीं है क्योंकि एकोपलम्भ का एकविषयकोपलम्भ अर्थ करने पर उस का अर्थ होगा स्वविषयकत्व और स्वभिन्न विषयकाम-उभय सम्बन्ध से वस्तुशून्योपलम्भ अर्थात जिस उपलम्भ का परस्पर भिन्न दो विषय न हो । तथा व्याप्ति इस प्रकार बनेगी कि जो विषयता सम्बन्ध से इशोपलम्म से विशिष्ट होता है वह स्वविषयनिष्ठभेदप्रतियोगिताशून्यत्व सम्बन्ध से भी इशोपलम्भ विशिष्ट होता है। अर्थात इशोफ्लम्भ के विषय में इडशोपलम्म के विषय का भेद नहीं होगा किन्तु इस में साध्य और हेतु में कोई विशेष अन्तर नहीं रह जाता, क्योंकि हेतु के शरीर में ज्ञान में भिन्नद्वयाविषयकत्व प्रविष्ट है और यही विज्ञानवादी को सिद्ध करना है। यदि एकोपलम्भ का 'एक उपलम्भ' अथ किया जायेगा तो यह व्याप्ति बनेगी कि जो यद्विषयकोपलम्भ का विषय होता है वह उस से अभिन्न होता है तो इस में समूहालम्बन ज्ञान के विषयों में व्यभिचार होगा।
यह भी ज्ञातव्य है कि ज्ञेयोपलम्भ और ज्ञानोपलम्भ में ऐक्य मानने पर दोनों के बीच सहशब्दार्थ का प्रयोग भी नहीं हो सकेगा क्योंकि 'चत्रः मत्रेण सहागतः' इस ध्यवहार की भाँति 'चैत्र: प्रात्मना सहागतः' यह व्यवहार नहीं होता । अतः सह शब्दार्थ को भेदघटित मानना आवश्यक होता है । इसलिये जिन में लवथा ऐक्य होगा उन के भत में सहशब्द का प्रयोग नहीं हो सकता अतः सहोपलम्भ नियम से ज्ञेय और ज्ञान में ऐक्य के साधन का प्रयत्न प्रकिश्चित्कर है।
[कमकत भाव की प्रतीति अविद्यामूलक नहीं है] विज्ञानयादी को ओर से जो यह बात कही गयी थी कि मैं 'नील को जानता हूं' इस प्रकार जो नील और महमर्थ ज्ञान में कर्म-कर्तृ भाव की प्रतीति होली है वह प्राविधक अविद्याकल्पित है-यह कथन भी अयुक्त है क्योंकि कर्म-कर्तृ भाव की प्रतीति का उत्तरकाल में बाघ नहीं होता । यदि अबाधित ज्ञान को भी भ्रम माना जायगा तो नील-पीतादि प्रतीतियाँ भी भ्रम हो जायगी और भ्रम से विषयसिद्धि नहीं होतो अत: शून्यता में विज्ञानवाद के पर्यवसान को आपत्ति होगी। 'नील, अहमर्थ,
और ग्रहण किया इनका स्वतन्त्र रुप से यानी परस्परासम्बदरूप से उपलम्भ कर्म-क प्रतीति में बाधक है - यह भी युक्त नहीं है क्योकि 'मैं नील को अ.नता हूँ' - इस प्रतीति में उक्त तीनों का परस्परसम्बद्ध रूप में भान स्पष्ट है। यह जो बात कही गयी थी कि ज्ञेय और ज्ञान को समकालीन मानने पर विनिगमनाधिरह से और भिन्नकालीन मानने पर ग्रहणकाल में ज्ञेय के विद्यमान न होने से ज्ञेय और ज्ञान में ग्राह्य-प्राहक भाव नहीं हो सकता अतः ज्ञान अर्थ का ग्राहक नहीं हो सकता,वह भी ठीक नहीं है क्योंकि ग्राह्यप्राहकभाव के खण्डन को उक्त रोति अपनाने पर अनुमान के कार्यकारणभाव में भी उक्त विकल्प में होनेवाले दोषों का प्रवेश अनिवार्य है। अर्थात् लिङ्ग और अनुमान को समकालीन मानने पर उन में कौन कारण और कौन कार्य इस में कोई विनिगमना न होगी और भिन्नकालीन मानने पर कार्यकारणभाव इसलिए नहीं होगा कि क्षणिक कारण अपने काल में अविद्यमान का भी जनक होगा तो अन्य भावि कार्यों में भी अविद्यमानत्व समान होने से उन सभी के जनकत्व की आपत्ति होगी।