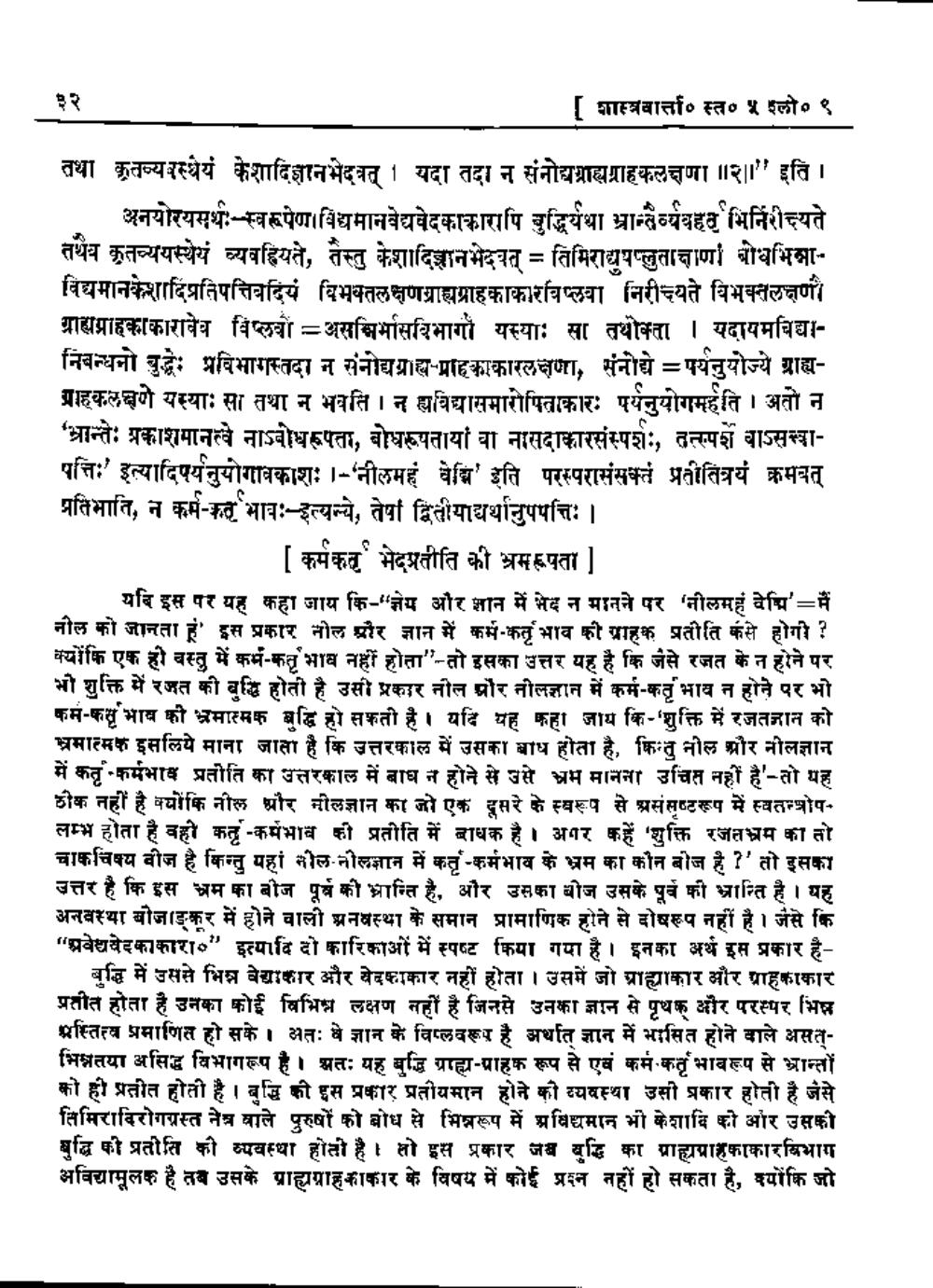________________
[ शास्त्रवार्ता० स्त० ५ इलो० ९
तथा कृतव्यवस्थेयं केशादिज्ञानभेदवत् । यदा तदा न संनोद्यग्राह्यग्राहकलक्षणा ||२||" इति ।
अनयोरयमर्थः-स्वरूपेणाविद्यमानवेद्यवेदकाकारापि बुद्धिर्यथा भ्रान्तैर्व्यवहत् भिर्निरीक्ष्यते तथैव कृतव्ययस्थेयं व्यवह्रियते, तैस्तु केशादिज्ञानभेदवत् = तिमिराद्युपप्लुताचाणां बोधभिन्नाविद्यमान केशादिप्रतिपत्तिवदियं विभक्तलक्षणग्राह्मग्राहकाकारविप्लवा निरीक्ष्यते विभक्तलक्षण ग्रास ग्राहकाकारावेव विप्लवों = असनिर्भासविभागों यस्याः सा तथोक्ता । यदायमचिद्यानिबन्धनो युद्धेः प्रविभागस्तदा न संनोद्यग्राह्य ग्राहकाकारलक्षणा, संनोद्ये = पर्यनुयोज्ये ग्राह्यग्राहकलक्षणे यस्याः सा तथा न भवति । न ह्यविद्यासमारोपिताकार: पर्यनुयोगमर्हति । अतो न 'आन्तेः प्रकाशमानत्वे नाऽवोधरूपता, बोधरूपतायां वा नासदाकारसंस्पर्शः, तत्स्पर्श वाऽसच्चापत्तिः' इत्यादिपर्यनुयोगावकाशः । - ' नीलमहं वेद्मि' इति परस्परासंसक्तं प्रतीतित्रयं क्रमवत् प्रतिभाति, न कर्म-कट भावः - इत्यन्ये, तेषां द्वितीयाद्यर्थानुपपत्तिः ।
३२
[ कर्मकर्तृ भेदप्रतीति की भ्रमरूपता ]
इस पर यह कहा जाय कि - "ज्ञेय और ज्ञान में भेद न मानने पर 'नीलमहं वेति' = मैं नील को जानता हूं इस प्रकार नील और ज्ञान में कर्म-कर्तृ भाव की ग्राहक प्रतीति कंसे होगी ? क्योंकि एक ही वस्तु में कर्म-कर्तृ भाव नहीं होता" तो इसका उत्तर यह है कि जैसे रजत के न होने पर भी शुक्ति में रजत की बुद्धि होती है उसी प्रकार नील और नीलज्ञान में कर्म-कर्तृ भाव न होने पर भी कर्म-कर्तृ भाव की भ्रमात्मक बुद्धि हो सकती है। यदि यह कहा जाय कि 'शुक्ति में रजतज्ञान को भ्रमात्मक इसलिये माना जाता है कि उत्तरकाल में उसका बाघ होता है, किन्तु नील और नीलज्ञान में कर्तृकर्मभाव प्रतीति का उत्तरकाल में बाघ न होने से उसे भ्रम मानना उचित नहीं है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि नील और नीलज्ञान का जो एक दूसरे के स्वरूप से प्रसंसृष्टरूप में स्वतन्त्रोपलम्भ होता है वही कर्तृकर्मभाव की प्रतीति में बाधक है। अगर कहें 'शुक्ति रजतभ्रम का तो चाकचिषय वीज है किन्तु यहां नील नीलज्ञान में कर्तृ - कर्मभाव के भ्रम का कौन बीज है ?' तो इसका उत्तर है कि इस भ्रम का बीज पूर्व की भ्रान्ति है, और उसका बीज उसके पूर्व की भ्रान्ति है । यह अनवस्था बोजाङ्कर में होने वाली अनवस्था के समान प्रामाणिक होने से दोषरूप नहीं है । जैसे कि "प्रवेश वेद का कारा" इत्यादि दो कारिकाओं में स्पष्ट किया गया है। इनका अर्थ इस प्रकार है
बुद्धि में उससे भिन्न वेद्याकार और वेदकाकार नहीं होता। उसमें जो ग्राह्याकार और ग्राहकाकार प्रतीत होता है उनका कोई विभिन्न लक्षण नहीं है जिनसे उनका ज्ञान से पृथक् और परस्पर भिन अस्तित्व प्रमाणित हो सके। अतः वे ज्ञान के विप्लवरूप है अर्थात् ज्ञान में भासित होने वाले असत्भिन्नतया असिद्ध विभागरूप है । अतः यह बुद्धि ग्राह्यग्राहक रूप से एवं कर्म कर्तृ भावरूप से भ्रान्तों को ही प्रतीत होती है । बुद्धि की इस प्रकार प्रतीयमान होने की व्यवस्था उसी प्रकार होती है जैसे तिमिराविरोगग्रस्त नेत्र वाले पुरुषों को बोध से भिन्नरूप में अविद्यमान भी केशादि को ओर उसकी बुद्धि की प्रतीति की व्यवस्था होती है । तो इस प्रकार जब बुद्धि का ग्राह्यग्राहकाकार विभाग raaree है तब उसके ग्राह्यग्राहकाकार के विषय में कोई प्रश्न नहीं हो सकता है, क्योंकि जो