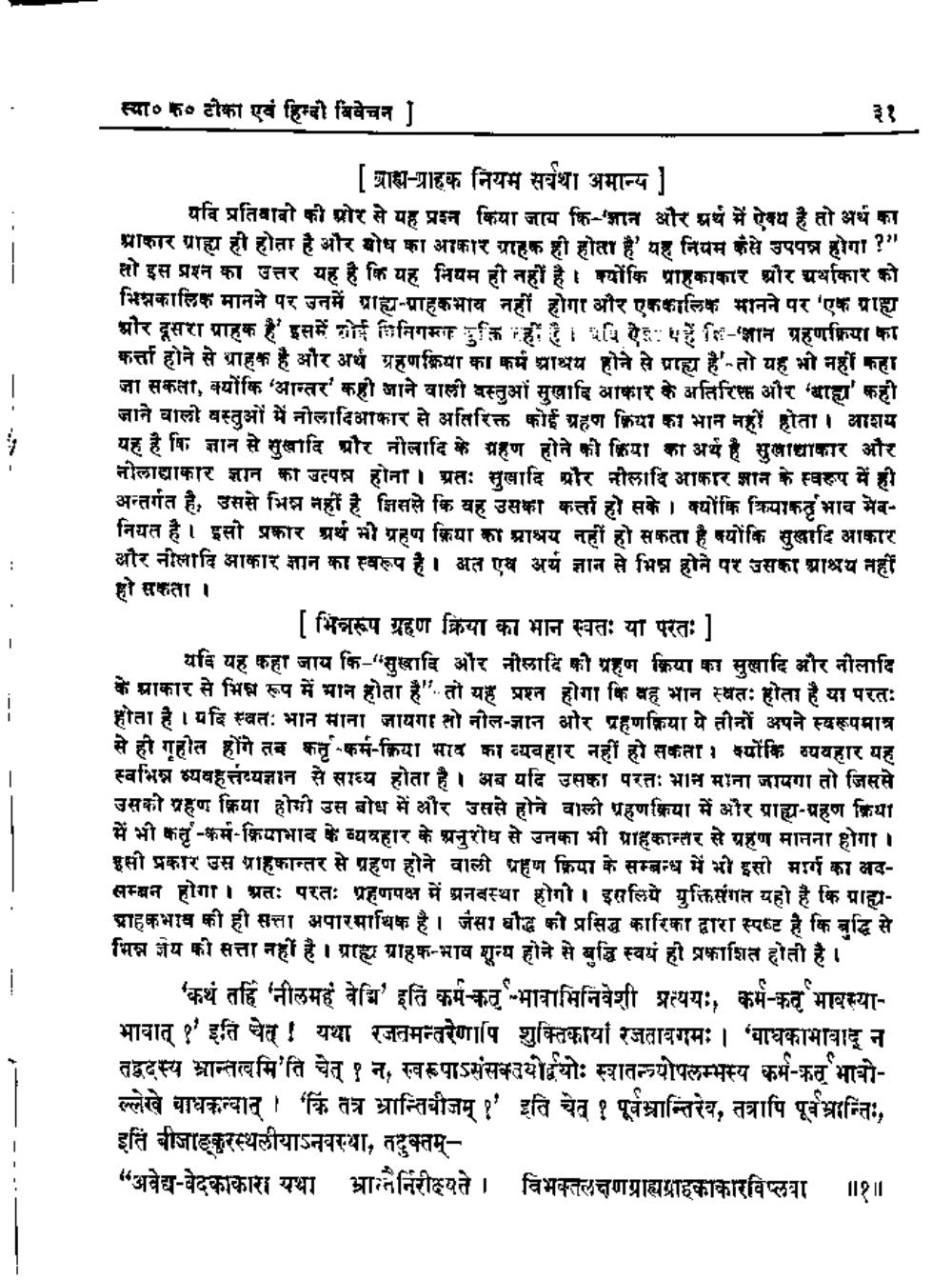________________
स्था.. टोका एवं हिन्दी विवेचन ।
३१
[बाह्य-ग्राहक नियम सर्वथा अमान्य] यदि प्रतिवावो की पोर से यह प्रश्न किया जाय कि-'झान और अर्थ में ऐक्य है तो अर्थ का प्राकार ग्राह्य ही होता है और बोध का आकार ग्राहक ही होता है यह नियम कैसे उपपन्न होगा ?" तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह नियम ही नहीं है। क्योंकि प्राहकाकार और अर्थाकार को भिन्नकालिक मानने पर उनमें ग्राह्य-ग्राहकभाव नहीं होगा और एककालिक मानने पर 'एक ग्राह्य और दूसरा ग्राहक है इसमें कोई मिनिगम्य बुक्ति नहीं है। यदि ऐव: पहें-शान ग्रहणक्रिया का कर्ता होने से ग्राहक है और अर्थ ग्रहण क्रिया का कर्म प्राश्रय होने से प्राह्य है- तो यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 'आन्तर' कही जाने वाली वस्तुओं सुखादि आकार के अतिरिक्त और 'बाहा' कही जाने वाली वस्तुओं में नौलादिआकार से अतिरिक्त कोई ग्रहण क्रिया का भान नहीं होता। आशय यह है कि ज्ञान से सुखादि और नीलादि के ग्रहण होने की क्रिया का अर्थ है सुखाधाकार और नोलाद्याकार ज्ञान का उत्पन्न होना। अतः सुखादि और नीलादि आकार ज्ञान के स्वरूप में ही अन्तर्गत है, उससे भिन्न नहीं है जिससे कि वह उसका कर्ता हो सके। क्योंकि क्रियाकर्तृभाव मेवनियत है। इसी प्रकार अर्थ मी ग्रहण किया का प्राश्रय नहीं हो सकता है क्योंकि सुखादि आकार और नीलादि आकार ज्ञान का स्वरूप है। अत एवं अर्थ ज्ञान से भिन्न होने पर उसका प्राश्रय नहीं हो सकता।
[भिन्नरूप ग्रहण क्रिया का भान स्वतः या परतः ] यदि यह कहा जाय कि-"सुखादि और नीलादि को ग्रहण क्रिया का सुखादि और नीलादि के प्राकार से भिन्न रूप में मान होता है". तो यह प्रश्न होगा कि वह भान स्वतः होता है या परतः होता है । यदि स्वत: भान माना जायगा सो नील-ज्ञान और प्रक्रिया ये तीनों अपने स्वरूपमात्र से ही गृहीत होंगे तर कर्तृ-कर्म-क्रिया माव का व्यवहार नहीं हो सकता। क्योंकि व्यवहार यह स्वभिन्न व्यवहतंव्यज्ञान से साध्य होता है। अब यदि उसका परतः भान माना जायगा तो जिससे उसको ग्रहण क्रिया होगी उस बोध में और उससे होने वाली ग्रहणक्रिया में और ग्राह्य-ग्रहण किया में भी कर्तृ-कर्म-क्रियाभाव के व्यवहार के अनुरोध से उनका भी ग्राहकान्तर से ग्रहण मानना होगा। इसी प्रकार उस ग्राहकान्तर से ग्रहण होने वाली ग्रहण क्रिया के सम्बन्ध में भी इसी मार्ग का अदलम्बन होगा। अतः परतः प्रहणपक्ष में अनवस्था होगी। इसलिये युक्तिसंगत यही है कि ग्रामप्राहकभाष की ही सत्ता अपारमाथिक है। जैसा बौद्ध को प्रसिद्ध कारिका द्वारा स्पष्ट है कि बुद्धि से भिन्न ज्ञेय की सत्ता नहीं है । ग्राह्य ग्राहक-भाव शून्य होने से बुद्धि स्वयं ही प्रकाशित होती है।
_ 'कथं तहि 'नीलमहं वेद्मि' इति कर्मक भावाभिनिवेशी प्रत्ययः, कर्म-कभावस्याभावात् ?' इति चेत् ! यथा रजतमन्तरेणापि शुक्तिकायां रजतावगमः। 'याधकामावाद् न तद्वदस्य भ्रान्तत्वमिति चेत् १ न, स्वरूपाऽसंसक्तयोयोः स्वातन्योपलम्भस्य कर्म-क भावोल्लेख बाधकन्वान् । 'किं तत्र भ्रान्तिबीजम् ?' इति चेत् ? पूर्वभ्रान्तिरेय, तत्रापि पूर्वभ्रान्तिः, इति बीजारस्थलीयाऽनवस्था, तदुक्तम्"अवेद्य-वेदकाकारा यथा भ्रान्तनिरीक्ष्यते । विभक्तलक्षणग्राह्यग्राहकाकारविप्लवा ॥१॥