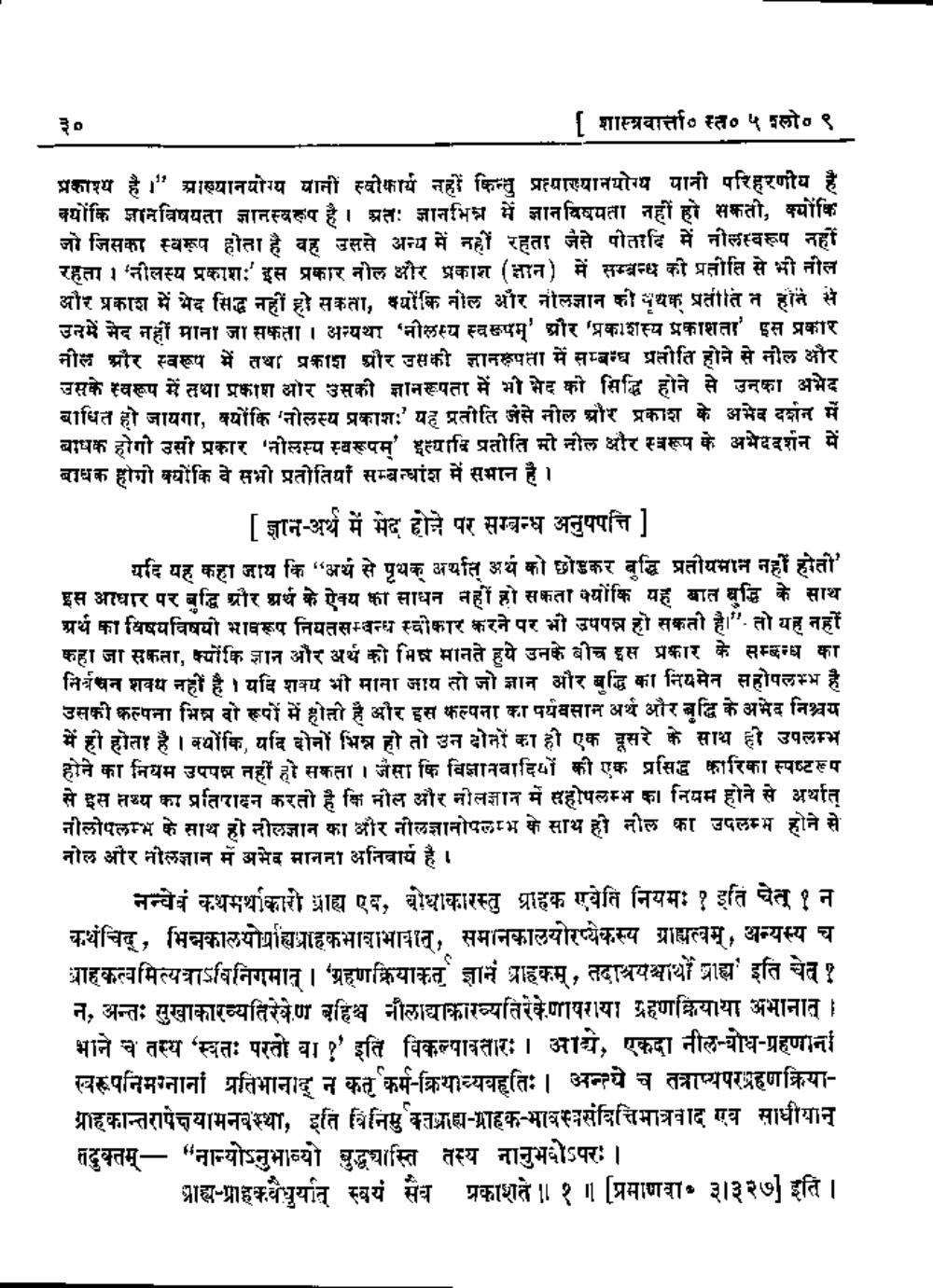________________
३०
[ शास्त्रवार्ता स्त०५ श्लो०९
प्रकाश्य है।" पाख्यानयोग्य यानी स्वीकार्य नहीं किन्तु प्रत्याख्यानयोग्य यानी परिहरणीय है क्योंकि ज्ञान विषयता ज्ञानस्वरूप है। अतः ज्ञानभिन्न में ज्ञान विषयता नहीं हो सकती, क्योंकि जो जिसका स्वरूप होता है वह उससे अन्य में नहीं रहता जैसे पीतादि में नीलस्वरूप नहीं रहता । 'नीलस्य प्रकाशः' इस प्रकार नील और प्रकाश (ज्ञान) में सम्बन्ध की प्रतीति से भी नील और प्रकाश में भेद सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि नील और नौलज्ञान की अथक प्रतीति न होने से उनमें भेद नहीं माना जा सकता । अन्यथा 'नीलस्य स्वरूपम्' और 'प्रकाशस्य प्रकाशता' इस प्रकार नील और स्वरूप में तथा प्रकाश और उसकी ज्ञानरूपत्ता में सम्बन्ध प्रतीति होने से नील और उसके स्वरूप में तथा प्रकाश ओर उसकी ज्ञानरूपता में भी भेद को सिद्धि होने से उनका अभेद बाधित हो जायगा, क्योंकि 'नोलस्य प्रकाशः' यह प्रतीति जैसे नील और प्रकाश के अमेव दर्शन में बाधक होगी उसी प्रकार 'नीलस्य स्वरूपम्' इत्यादि प्रतीति मो नोल और स्वरूप के अभेददर्शन में बाधक होगी क्योंकि वे सभी प्रतीतियाँ सम्बन्धांश में समान है।
[ ज्ञान-अर्थ में भेद होने पर सम्बन्ध अनुपपत्ति ] ___ यदि यह कहा जाय कि "अर्थ से पृथक् अर्थात् अर्थ को छोडकर बुद्धि प्रतीयमान नहीं होती' इस आधार पर बुद्धि और अर्थ के ऐक्य का साधन नहीं हो सकता क्योंकि यह बात धुद्धि के साथ अर्थ का विषयविषयो भावरूप नियतसम्बन्ध स्वीकार करने पर भी उपपन्न हो सकती है।" तो यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज्ञान और अर्थ को मिन्न मानते हुये उनके बीच इस प्रकार के सम्बन्ध का निर्वचन शक्य नहीं है। यदि शक्य भी माना जाय तो जो ज्ञान और बुद्धि का नियमेन सहोपलभ्भ है उसकी कल्पना भिन्न दो रूपों में होती है और इस कल्पना का पर्यवसान अर्थ और बुद्धि के अभेद निश्चय में ही होता है । क्योंकि, यदि दोनों भिन्न हो तो उन दोनों का ही एक दूसरे के साथ ही उपलम्भ होने का नियम उपपन्न नहीं हो सकता। जैसा कि विज्ञानवादियों की एक प्रसिद्ध कारिका स्पष्टरूप से इस तथ्य का प्रतिरादन करती है कि नील और नीलझान में सहोपलम्भ का नियम अर्थात नीलोपलम्भ के साथ होनोलज्ञान का और नीलज्ञानोपलम्भ के साथ ही नील का उपलम्म होने से नोल और नोलज्ञान में अभेव मानना अनिवार्य है।
नन्वेवं कथमाकारी ग्राह्य एव, बोधाकारस्तु प्राहक एवेति नियमः १ इति चेत् १ न कथंचिद् , भिन्नकालयोांववाहकभावाभावान्, समानकालयोरप्येकस्य ग्राह्यत्वम् , अन्यस्य च ग्राहकत्वमित्यत्राविनिगमात् । 'ग्रहणक्रियाकत ज्ञानं प्राहकम् , तदाश्रयश्चाओं ब्राह्म' इति चेत् ? न, अन्तः सुखाकारव्यतिरेवेण बहिश्च नौलाद्याकारण्यतिरेकेणापराया ग्रहणक्रियाया अभानात् । भाने च तस्य 'स्वतः परतो वा ?' इति विकल्पावतारः । आये, एकदा नील-योध-प्रहणानां खरूपनिमग्नानां प्रतिभानाद् न क कर्म-क्रियाव्यवहृतिः। अन्ये च तत्राप्यपरग्रहण क्रियाग्राहकान्तरापेक्षयामनवस्था, इति विनिमुक्तिनाप-ग्राहक-भावस्वसंवित्तिमात्रवाद एव साधीयान तदुक्तम्- "नान्योऽनुभाव्यो बुद्धयास्ति तस्य नानुभवोऽपरः ।
ब्राह्य-प्राहकवैधुर्यात् स्वयं सैव प्रकाशते ॥ १ ॥ [प्रमाणवा• ३।३२७] इति ।