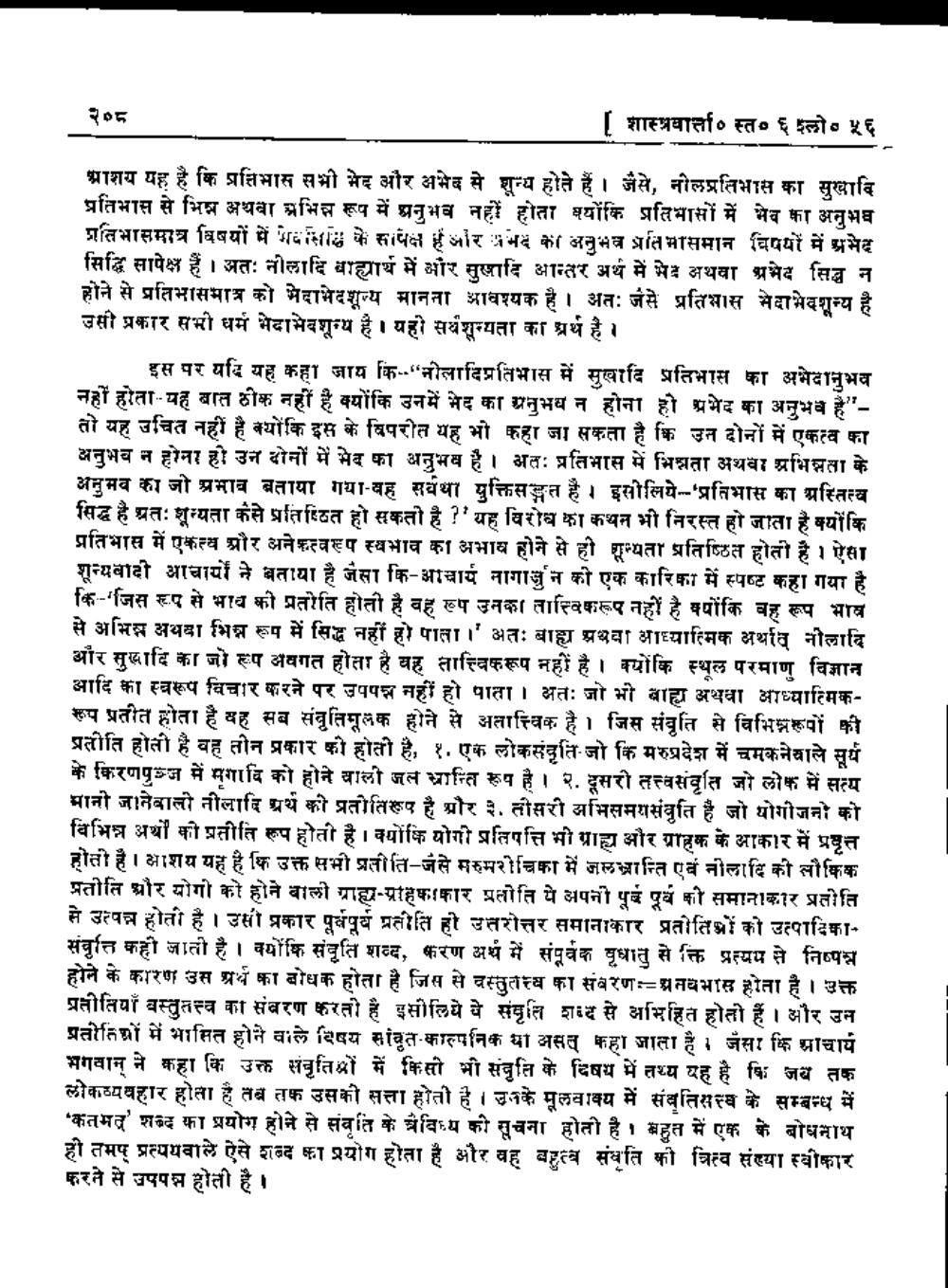________________
[ शास्त्रवार्ता० स्त० ६ श्लो० ५६
श्राशय यह है कि प्रतिभास सभी भेद और अमेव से शुन्य होते हैं । जैसे, नीलप्रतिभास का सुखादि प्रतिभास से भिन्न अथवा अभिन्न रूप में अनुभव नहीं होता श्योंकि प्रतिभासों में भेव का अनुभव प्रतिभासमात्र विषयों में माता के सापेक्ष है और अभद का अनुभव प्रतिमासमान विषयों में अभेद सिद्धि सापेक्ष हैं। अतः नीलादि बाह्यार्थ में और सुखादि आन्तर अर्थ में भेद अथवा अभेद सिद्ध न होने से प्रतिभासमात्र को भेदाभेदशून्य मानना आवश्यक है। अतः जैसे प्रतिभास भेदाभेदशून्य है उसी प्रकार सभी धर्म भेदाभेवशून्य है। यही सर्थशून्यता का अर्थ है।
इस पर यदि यह कहा जाय कि-"नीलादिप्रतिभास में सुखादि प्रतिभास का अभेदानुभव नहीं होता- यह बात ठीक नहीं है क्योंकि उनमें भेद का अनभव न होना ही प्रभेद तो यह उचित नहीं है क्योंकि इस के विपरीत यह भी कहा जा सकता है कि उन दोनों में एकत्व का अनुभव न होना ही उन दोनों में भेद का अनुभव है। अतः प्रतिभास में भिन्नता अथवा अभिन्नता के अनुमव का जो प्रभाव बताया गया-वह सर्वथा युक्तिसङ्गत है। इसीलिये--'प्रतिभास का अस्तित्व सिद्ध है अतः शून्यता कैसे प्रतिष्ठित हो सकती है ? यह विरोध का कथन भी निरस्त हो जाता है क्योंकि प्रतिभास में एकत्व और अनेकत्वरूप स्वभाव का अभाव होने से ही शून्यता प्रतिष्ठित होती है। ऐसा शून्यबादी आचार्यों ने बताया है जैसा कि-आचार्य नागार्जुन को एक कारिका में स्पष्ट कहा गया है कि-जिस रूप से भाव की प्रतीति होती है वह रूप उनका तात्त्विकरूप नहीं है क्योंकि वह रूप भाव से अभिन्न अथवा भिन्न रूप में सिद्ध नहीं हो पाता।' अतः बाह्य अथवा आध्यात्मिक अर्थाव नीलादि और सुखादि का जो रूप अवगत होता है यह तात्त्विकरूप नहीं है। क्योंकि स्थूल परमाणु विज्ञान आदि का स्वरूप विचार करने पर उपपन्न नहीं हो पाता। अतः जो भी बाह्य अथवा आध्यात्मिकरूप प्रतीत होता है यह सब संवृतिमूलक होने से अतात्विक है। जिस संवृति से विभिन्नरूपों की प्रतीति होती है वह तीन प्रकार की होती है, १. एक लोकसंदति-जो कि मरुप्रदेश में चमकने के किरणपुञ्ज में मगादि को होने वाली जल भ्रान्ति रूप है। २. दूसरी तत्त्वसंवृति जो लोक में सत्य मानी जानेवाली नीलादि अर्थ को प्रतीतिरूप है और ३. तीसरी अभिसमयसंवृति है जो योगीजनो को विभिन्न अर्थों को प्रतीति रूप होती है। क्योंकि योगी प्रतिपत्ति भी ग्राह्य और ग्राहक के आकार में प्रवृत्त होती है । आशय यह है कि उक्त सभी प्रतीति-जैसे मरुमरीचिका में जलभ्रान्ति एवं नीलादि की लौकिक प्रतीति और योगी को होने वाली ग्राहा-ग्राहकाकार प्रतोति ये अपनी पूर्व पूर्व को समानाकार प्रतीति से उत्पन्न होती है । उसी प्रकार पूर्वपूर्व प्रतीति हो उत्तरोत्तर समानाकार प्रतोतिनों को उत्पादिका. संवृत्ति कही जाती है। क्योंकि संवृति शब्द, करण अर्थ में संपूर्वक वृधातु से क्ति प्रत्यय से निष्पन्न होने के कारण उस अर्थ का बोधक होता है जिस से वस्तुतत्त्व का संवरण: अनवभास होता है । उक्त प्रतीतियाँ बस्तुतत्त्व का संवरण करती है इसीलिये ये संवृत्ति शब्द से अभिहित होतो हैं । और उन प्रतीतित्रों में भासित होने वाले विषय सांवृत-काल्पनिक या असत् कहा जाता है। जैसा कि प्राचार्य भगवान ने कहा कि उक्त संतिओं में किसी भी संवति के विषय में तथ्य यह है कि जब तक लोकव्यवहार होता है तब तक उसकी सत्ता होती है । उनके मूलवाक्य में संवृतिसत्व के सम्बन्ध में 'कतम' शब्द का प्रयोग होने से संवृति के त्रैविध्य को सूचना होती है। बहुत में एक के बोधनाथ ही तमप् प्रत्ययवाले ऐसे शब्द का प्रयोग होता है और वह बहुत्व संवृति को त्रित्व संख्या स्वीकार करने से उपपन्न होती है।