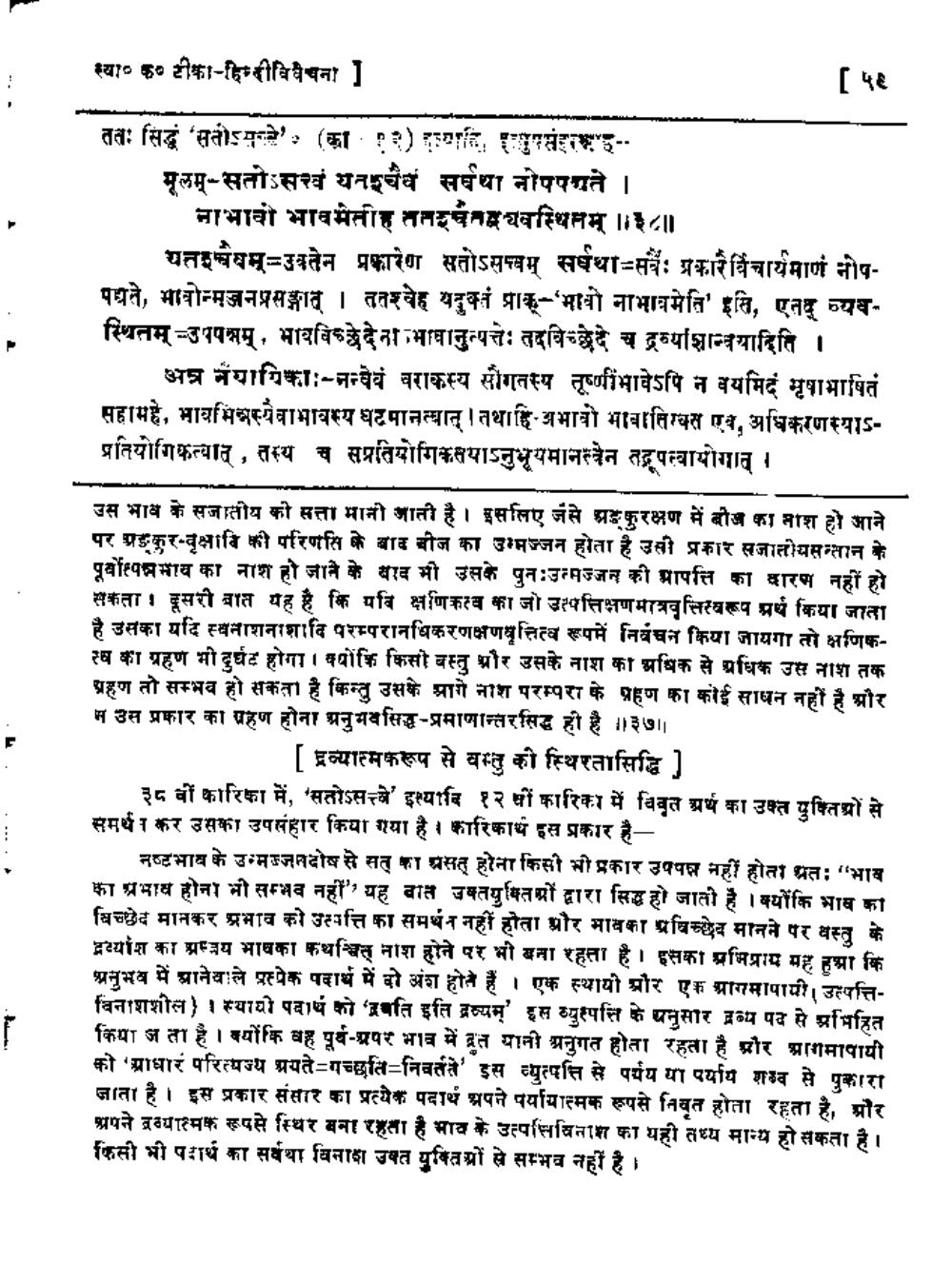________________
स्या का टीका-हिन्दीविधैधना ]
[ ५६
-
-
ततः सिद्धं 'सतोऽसाले (का. ३) जाति पसंहारमा इ..
मूलम्-सतोऽसत्वं यतश्चैवं सर्वथा नोपपद्यते ।
नाभावो भावमेतीह ततश्चतमयवस्थितम् ॥३८॥
यतश्चैषम् उक्तेन प्रकारेण सतोऽसम्यम् सर्षया सर्वैः प्रकारे विचार्यमाणं नोपपनते, मावोन्मजनप्रसङ्गात् । ततश्वेह यदुक्तं प्राक्-'मावो नाभावमेति' इति, एतद् व्यवस्थितम् उपपत्रम् , भारविच्छेदेना भाषानुत्पत्तेः तदविच्छेदे च द्रव्यांशान्वयादिति ।।
___ अत्र नैयायिका:-नन्वेवं वराकस्य सौगतस्य तूष्णीभावेऽपि न वयमिदं मृषाभाषितं सहामहे, भारभिन्नस्यैवाभावस्य घटमानत्वात् । तथाहि अभावो भावातिरक्स एव, अधिकरणस्याप्रतियोगिफत्वात् , तस्य च सप्रतियोगिकसयाऽनुभूयमानत्वेन तद्पन्वायोगात् ।
उस भाव के सजातीय को सत्ता मानी जाती है। इसलिए जैसे अङ्कुरक्षण में बीज का नाश हो आने पर प्रडकुर-वृक्षावि की परिणति के बाद बीज का उम्मजन होता है उसी प्रकार सजातीयसन्तान के पूर्वोत्पन्नमाय का नाश हो जाने के बाद भी उसके पुन:जन्मज्जन की मापत्ति का कारण नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि यदि क्षणिकरव का जो उत्पत्तिक्षणमात्रवृत्तिस्वरूप प्रर्थ किया जाता
यदि स्वनाशनाशादि परम्परानधिकरणक्षणवृत्तित्व रूपमें नियंचन किया जायगा तो क्षणिकस्वका ग्रहण भी दर्घट होगा। क्योंकि किसी वस्तु और उसके नाश का अधिक से अधिक उस शतक ग्रहण तो सम्भव हो सकता है किन्तु उसके आगे नाश परम्परा के प्रहण का कोई साधन नहीं है और म उस प्रकार का ग्रहण होना अनुभवसिद्ध-प्रमाणान्तरसिद्ध ही है ॥३७।।।
[द्रव्यात्मकरूप से वस्तु को स्थिरतासिद्धि ] ३८ वीं कारिका में, 'सतोऽसत्त्वे' इत्यादि १२ वी कारिका में विवृत अर्थ का उक्त युक्तियों से समर्थन कर उसका उपसंहार किया गया है। कारिफार्थ इस प्रकार है
नष्टभाव के उन्मजनदोष से सत् का प्रसत् होना किसी भी प्रकार उपपन्न नहीं होता प्रत: "भाव का प्रभाव होना भी सम्भव नहीं' यह बात उक्तयुक्तियों द्वारा सिद्ध हो जाती है । क्योंकि भाव का विच्छेद मानकर प्रभाव को उत्पत्ति का समर्थन नहीं होता और भावका अविच्छेव मानने पर वस्तु के द्रव्यांश का अस्त्रय भाषका कथञ्चित् नाश होने पर भी बना रहता है। इसका अभिप्राय मह हा कि अनुभव में प्रानेवाले प्रत्येक पदार्थ में वो अंश होते हैं । एक स्थायी और एक पागमापायी। उत्पत्तिविनाशशील)। स्थायी पदार्थ को 'द्रवति इति द्रव्यम्' इस व्युत्पत्ति के अनुसार द्रब्य पद से अभिहित किया जता है । क्योंकि वह पूर्व-प्रपर भाव में द्रुत यानी अनुगत होता रहता है और प्रागमापायी को 'प्राधार परित्यज्य प्रयते-गच्छति निवर्तते' इस व्युत्पत्ति से पर्यय या पर्याय सम्व से पुकारा जाता है। इस प्रकार संसार का प्रत्येक पदार्थ अपने पर्यायात्मक रूपसे निवृत होता रहता है, और अपने द्रव्यात्मक रूपसे स्थिर बना रहता है भाव के उत्पत्तिविनाश का यही तथ्य मान्य हो सकता है। किसी भी पदार्थ का सर्वथा विनाश उक्त युक्तियों से सम्भव नहीं है।